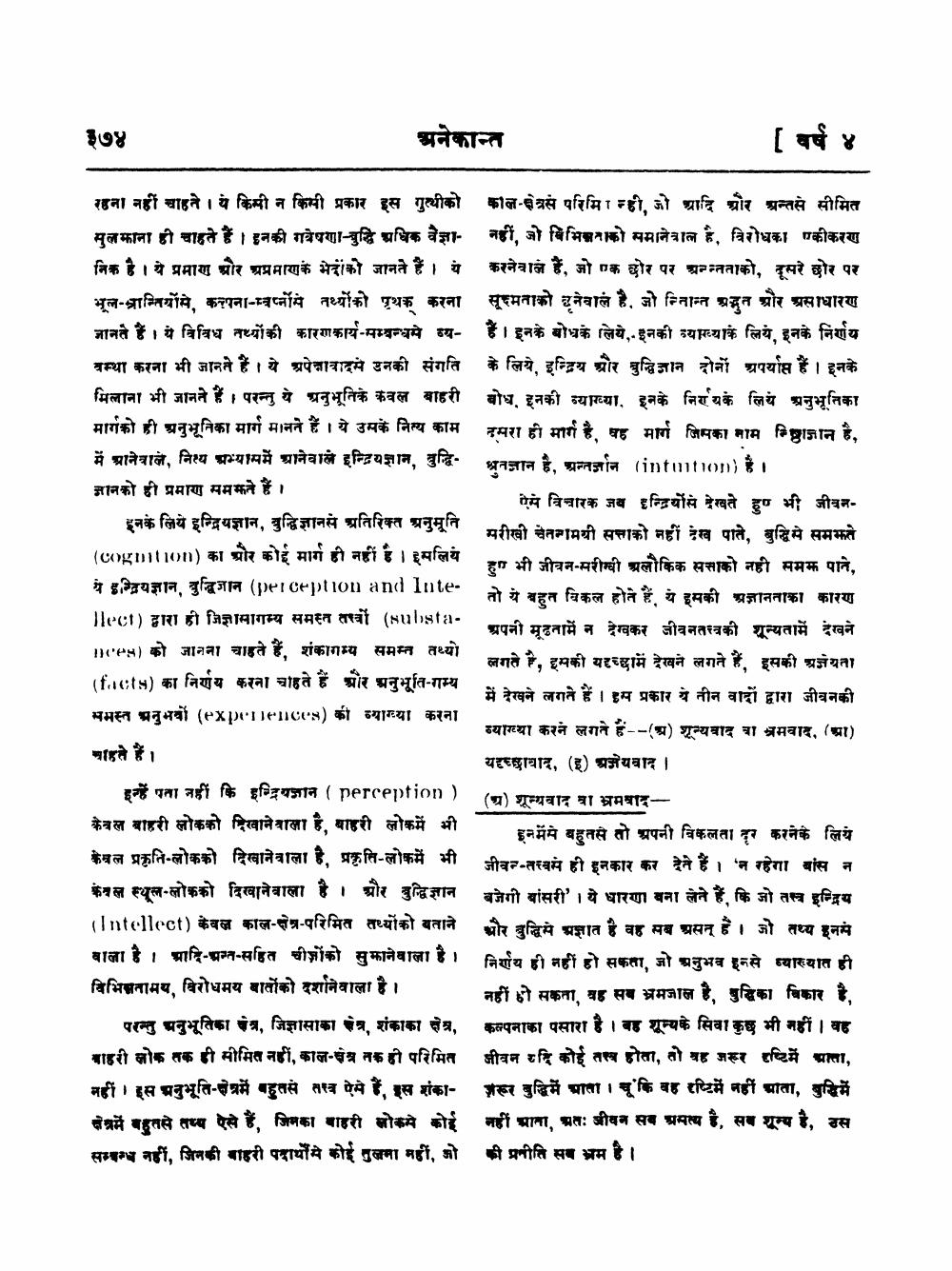________________
३७४
अनेकान्त
।
रहना नहीं चाहते। ये किसी न किसी प्रकार इस गुत्थीको सुलझाना ही चाहते हैं। इनकी बुद्धि अधिक वैज्ञागवेषणा-बुद्धि निक है। ये प्रमाण और अप्रमाणकं भेदोंको जानते हैं। ये भू-प्रान्तियोंमे कल्पना-स्वप्नोंये तथ्योंको पृथक करना जानते हैं। ये विविध तथ्योंकी कारणकार्य सम्बन्धमे व्य वस्था करना भी जानते हैं। ये पेवावाद उनकी संगति मिलाना भी जानते हैं परन्तु ये धनुभूतिके केवल बाहरी मार्गको ही अनुभूतिका मार्ग मानते हैं। ये उसके नित्य काम में आनेवाले, नित्य अभ्यासमें श्रानेवाले इन्द्रियज्ञान, बुद्धिज्ञानको ही प्रमाण समझते हैं।
F
इसके लिये इन्द्रियज्ञान, बुद्धिज्ञान अतिरिक्त अनुभूति (cognition) का और कोई मार्ग ही नहीं है। मि ये इन्द्रियज्ञान, बुद्धिज्ञान ( perception and Inte llect) द्वारा ही जिज्ञासागम्य समस्त तत्वों (substa एल) को जानना चाहते हैं, शंकागम्य समस्त तथ्यो (facts) का निर्णय करना चाहते हैं और अनुभूति-गम्य समस्त अनुभव (experiences) की व्याख्या करना चाहते हैं।
इन्हें पता नहीं कि इन्द्रियज्ञान ( perception ) केवल बाहरी लोकको दिखाने वाला है, बाहरी लोक में भी केवल प्रकृति-लोकको दिखानेवाला है, प्रकृति-लोकमें भी केवल स्थूल लोकको दिखाने वाला है । और बुद्धिज्ञान (Intellect) केवल काल क्षेत्र परिमित तथ्योंको बताने वाला है। आदि-अन-सहित पीशोंको सुकानेवाला है। विभिन्नतामय, विरोधमय बालोंको दर्शानेवाला है।
[ वर्ष ४
काल-क्षेत्र परिमित नही जो यादि और अन्त सीमित नहीं, जो कि माल है. विरोधका एकीकरण समानेवाल करनेवाले हैं, जो एक छोर पर अन्न्नताको, दूसरे छोर पर सूक्ष्मताको छूनेवाल है, जो नितान्त अद्भुत चोर असाधारण हैं। इनके बोधके लिये, इनकी व्याख्याके लिये इनके निय के लिये इन्द्रिय और विज्ञान दोनों अपयश हैं। इनके
,
बोध इनकी व्याख्या
इनके
निर्णय के लिये अनुभूतिका
दूसरा ही मार्ग है, वह
मार्ग जिसका नाम मिष्ठज्ञान है, (intation) है।
परन्तु अनुभूतिका क्षेत्र जिज्ञासाका क्षेत्र शंकाका क्षेत्र, बाहरी लोक तक ही सीमित नहीं, काल-क्षेत्र तक ही परिमित नहीं। इस अनुभूति में बहुत है, इस शंकाक्षेत्र में बहुतसे तथ्य ऐसे हैं, जिनका बाहरी लोकसे कोई सम्बन्ध नहीं, जिनकी बाहरी पदार्थोंमे कोई मुखमा नहीं को
श्रुतज्ञान नजान है
विचारक जब इन्द्रियोंसे देखते हुए भी जीवनमीनाको नहीं देख पाते, बुद्धि सम
हुए
भी जीवन सम्बी अलौकिक ससाको नही समझ पाते, तो ये बहुत विकल होते हैं, ये इसकी अज्ञानताका कारण अपनी नामें न देखकर जीवनतत्वकी शून्यतामें देखने लगते है, इसकी हमें देखने लगते हैं, इसकी अज्ञेयता में देखने लगते हैं। इस प्रकार ये तीन वादों द्वारा जीवनकी व्याख्या करने लगते हैं-- (अ) शून्यवाद वा श्रमवाद, (श्री) छावाद, (इ) अज्ञेयवाद ।
(थ) शून्यवाद वा भ्रमवाद
इनमें बहुतसे तो अपनी विकलता दूर करनेके लिये जीवन-तत्व ही इनकार कर देते हैं। 'न रहेगा बांस न बजेगी बांसरी' | ये धारणा बना लेते हैं, कि जो तस्त्र इन्द्रिय और बुद्धि अज्ञात है वह सब असत् है । जो तथ्य इनमे निर्णय ही नहीं हो सकता, जो अनुभव इनसे व्यवास्थात ही नहीं हो सकता, यह सब भ्रमजाल है, बुद्धिका विकार है, कल्पनाका पसारा है । वह शून्यके सिवा कुछ भी नहीं। वह जीवन यदि कोई तस्त्र होता, तो वह जरूर दृष्टिमें प्राता, जरूर बुद्धिमें आता । चूंकि वह रष्टिमें नहीं आता, बुद्धिमें नहीं आता, अतः जीवन सब असत्य है, सब शून्य है, उस की प्रनीति सब भ्रम है 1