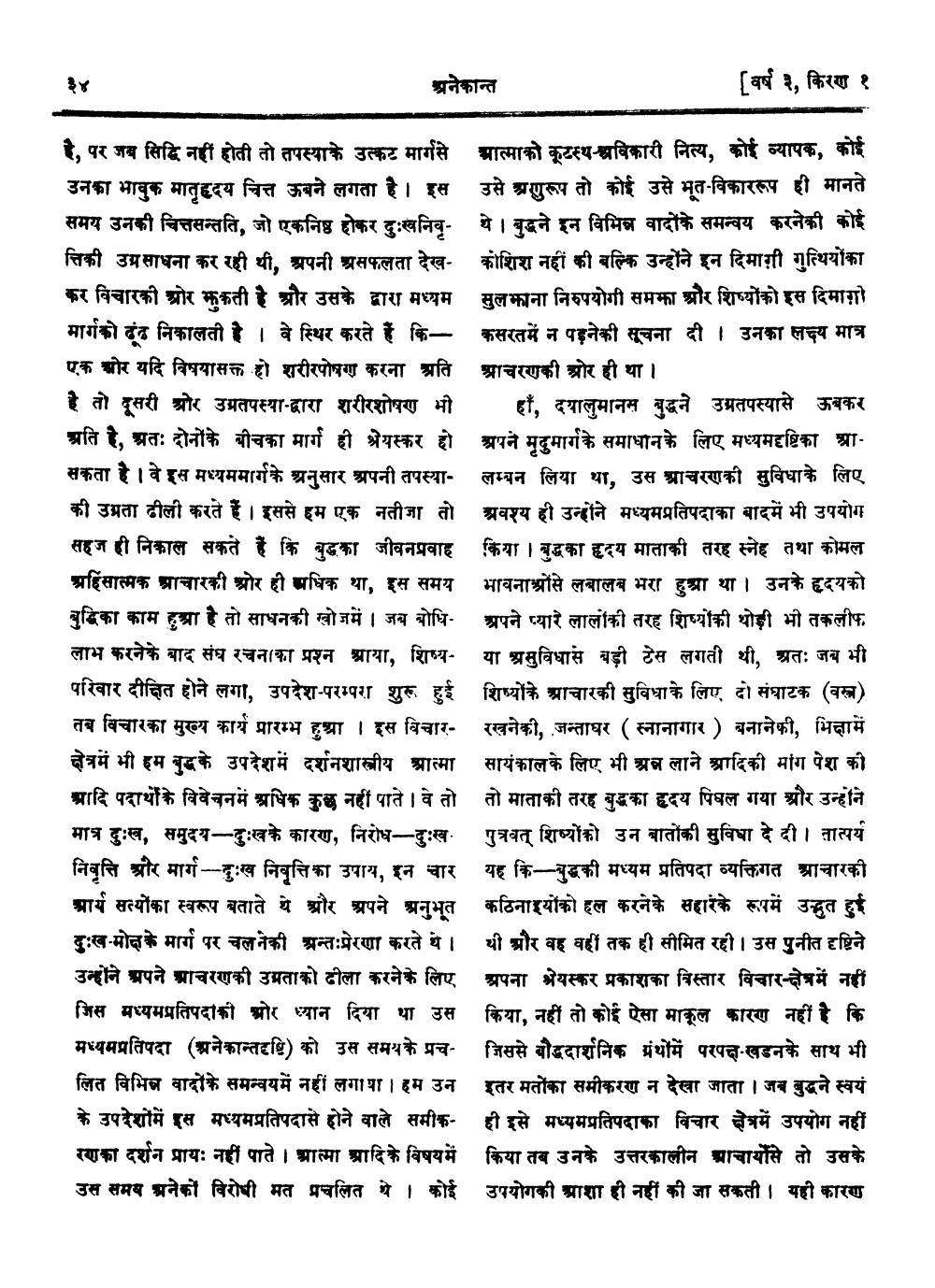________________
अनेकान्त
[वर्ष ३, किरण १
है, पर जब सिद्धि नहीं होती तो तपस्याके उत्कट मार्गसे आत्माको कूटस्थ-अविकारी नित्य, कोई व्यापक, कोई उनका भावुक मातृहृदय चित्त ऊबने लगता है। इस उसे अणुरूप तो कोई उसे भूत-विकाररूप ही मानते समय उनकी चित्तसन्तति, जो एकनिष्ठ होकर दुःखनिवृ- थे। बुद्धने इन विभिन्न वादोंके समन्वय करनेकी कोई त्तिकी उपसाधना कर रही थी, अपनी असफलता देख- कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने इन दिमाग़ी गुत्थियोंका कर विचारकी ओर झुकती है और उसके द्वारा मध्यम सुलझाना निरुपयोगी समझा और शिष्योंको इस दिमागो मार्गको ढूंढ निकालती है। वे स्थिर करते हैं कि- कसरतमें न पड़नेकी सूचना दी । उनका लक्ष्य मात्र एक ओर यदि विषयासक्त हो शरीरपोषण करना अति आचरणकी ओर ही था। है तो दूसरी ओर उग्रतपस्या-द्वारा शरीरशोषण भी हाँ, दयालुमानम बुद्धने उग्रतपस्यासे ऊबकर अति है, अतः दोनोंके बीचका मार्ग ही श्रेयस्कर हो अपने मृदुमार्गके समाधान के लिए मध्यमदृष्टिका श्रासकता है । वे इस मध्यममार्गके अनुसार अपनी तपस्या- लम्बन लिया था, उस आचरणकी सुविधा के लिए की उग्रता ढीली करते हैं । इससे हम एक नतीजा तो अवश्य ही उन्होंने मध्यमप्रतिपदाका बादमें भी उपयोग सहज ही निकाल सकते हैं कि बुद्धका जीवनप्रवाह किया । बुद्धका हृदय माताकी तरह स्नेह तथा कोमल अहिंसात्मक प्राचारकी ओर ही अधिक था, इस समय भावनाओंसे लबालब भरा हुआ था। उनके हृदयको बुद्धिका काम हुआ है तो साधनकी खोजमें । जब बोधि- अपने प्यारे लालौकी तरह शिष्योंकी थोड़ी भी तकलीफ लाभ करनेके बाद संघ रचनाका प्रश्न अाया, शिष्य- या असुविधास बड़ी ठेस लगती थी, अतः जब भी परिवार दीक्षित होने लगा, उपदेश-परम्परा शुरू हुई शिष्यों के प्राचारकी सुविधा के लिए. दो संघाटक (वस्त्र) तब विचारका मुख्य कार्य प्रारम्भ हुश्रा । इस विचार- रखनेकी, जन्ताघर ( स्नानागार ) बनानेकी, भिक्षामें क्षेत्रमें भी हम बुद्ध के उपदेशमें दर्शनशास्त्रीय प्रात्मा सायंकाल के लिए भी अन्न लाने श्रादिकी मांग पेश की
आदि पदार्थोके विवेचनमें अधिक कुछ नहीं पाते । वे तो तो माताकी तरह बुद्धका हृदय पिघल गया और उन्होंने मात्र दुःख, समुदय-दुःखके कारण, निरोध-दुःख- पुत्रवत् शिष्योंको उन बातोंकी सुविधा दे दी। तात्पर्य निवृत्ति और मार्ग-दुःख निवृत्ति का उपाय, इन चार यह कि-बुद्धकी मध्यम प्रतिपदा व्यक्तिगत प्राचारकी
आर्य सत्योंका स्वरूप बताते थे और अपने अनुभूत कठिनाइयोंको हल करनेके सहारके रूपमें उद्भुत हुई दुःख-मोक्ष के मार्ग पर चलनेकी अन्तःप्रेरणा करते थे। थी और वह वहीं तक ही सीमित रही। उस पुनीत दृष्टिने उन्होंने अपने आचरणकी उग्रताको ढीला करने के लिए अपना श्रेयस्कर प्रकाशका विस्तार विचार-क्षेत्र में नहीं जिस मध्यमप्रतिपदाको ओर ध्यान दिया था उस किया, नहीं तो कोई ऐसा माकूल कारण नहीं है कि मध्यमप्रतिपदा (अनेकान्तदृष्टि) को उस समय के प्रच- जिससे बौद्धदार्शनिक ग्रंथोंमें परपक्ष खडनके साथ भी लित विभिन्न वादोंके समन्वयमें नहीं लगाया । हम उन इतर मतोंका समीकरण न देखा जाता । जब बुद्धने स्वयं के उपदेशोंमें इस मध्यमप्रतिपदासे होने वाले समीक- ही इसे मध्यमप्रतिपदाका विचार क्षेत्रमें उपयोग नहीं रणका दर्शन प्रायः नहीं पाते । प्रात्मा श्रादिके विषयमें किया तब उनके उत्तरकालीन प्राचार्योंसे तो उसके उस समय अनेकों विरोधी मत प्रचलित थे । कोई उपयोगकी आशा ही नहीं की जा सकती। यही कारण