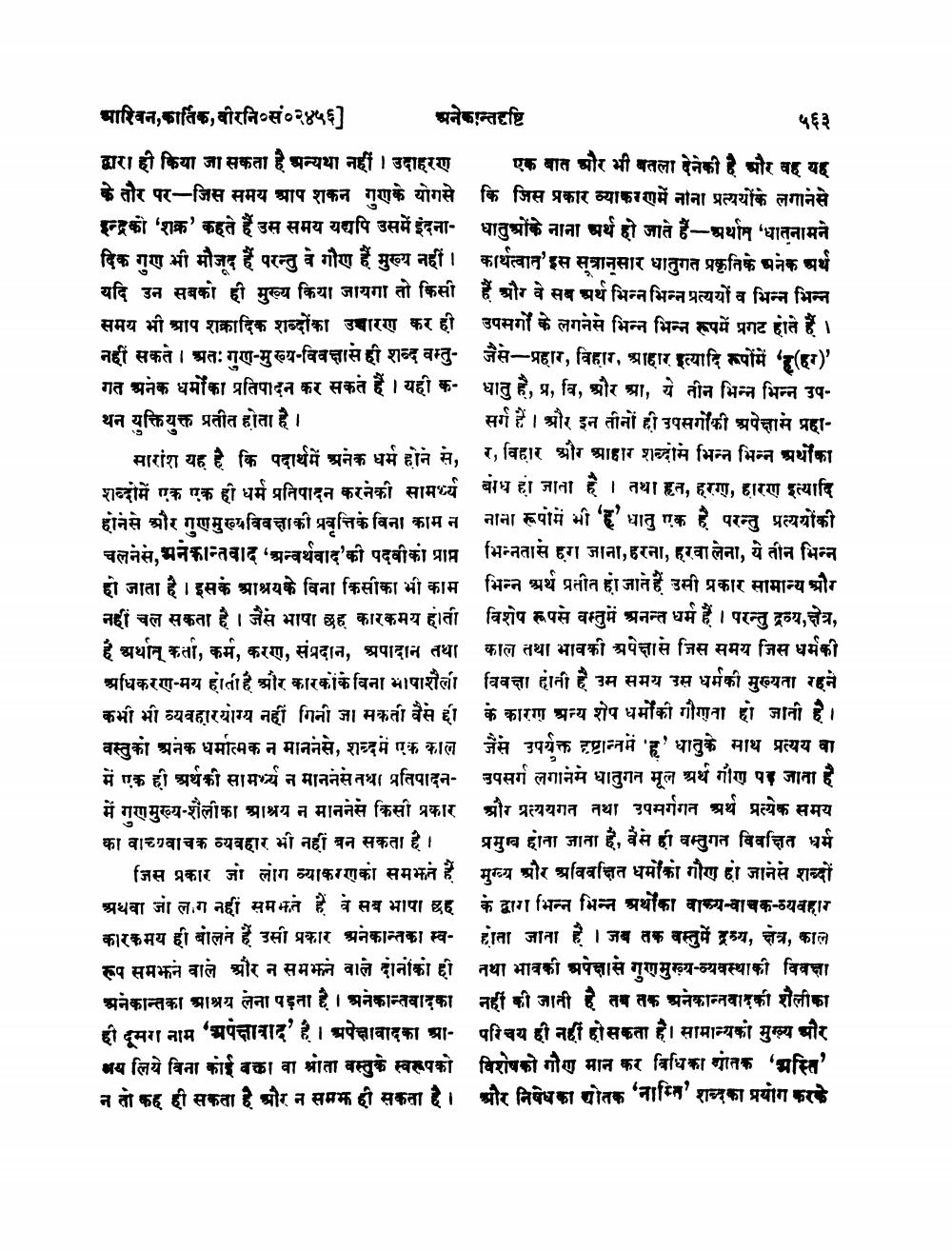________________
माश्विन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६] अनेकान्तदृष्टि
५६३ द्वारा ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं । उदाहरण एक बात और भी बतला देनेकी है और वह यह के तौर पर-जिस समय आप शकन गुणके योगसे कि जिस प्रकार व्याकरणमें नाना प्रत्ययोंके लगानसे इन्द्रको 'शक' कहते हैं उस समय यद्यपि उसमें इंदना- धातुओंके नाना अर्थ हो जाते हैं अर्थात 'धातनामने दिक गण भी मौजूद हैं परन्तु वे गौण हैं मुख्य नहीं। कार्थत्वात' इस सूत्रानुसार धातुगत प्रकृति के अनेक अर्थ यदि उन सबको ही मुख्य किया जायगा तो किसी हैं और वे सब अर्थ भिन्न भिन्न प्रत्ययों व भिन्न भिन्न समय भी आप शकादिक शब्दोंका उच्चारण कर ही उपमों के लगनेसे भिन्न भिन्न रूपमें प्रगट होते हैं । नहीं सकते । अतः गुण-मुख्य-विवक्षास ही शब्द वस्तु- जैसे-प्रहार, विहार, श्राहार इत्यादि रूपोंमें 'ह(हर) गत अनेक धोका प्रतिपादन कर सकते हैं । यही क- धातु है, प्र, वि, और श्रा, ये तीन भिन्न भिन्न उपथन युक्तियुक्त प्रतीत होता है।
सर्ग हैं। और इन तीनों ही उपसर्गोंकी अपेक्षाम प्रहा__ मारांश यह है कि पदार्थमें अनेक धर्म होने से, र, विहार और श्राहार शब्दाम भिन्न भिन्न प्रोंका शब्दोमें एक एक ही धर्म प्रतिपादन करनेकी सामर्थ्य बांध हो जाता है । तथा हत, हरण, हारण इत्यादि होनसे और गुणमुख्यविवक्षाकी प्रवृत्तिकं विना काम न नाना रूपोमें भी 'ह' धातु एक है परन्तु प्रत्ययोंकी चलनेस,भनेकान्तवाद 'अन्वर्थवाद' की पदवीको प्राप्त भिन्नतासं हग जाना, हरना, हरवा लेना, ये तीन भिन्न हो जाता है । इसके आश्रयके विना किसीका भी काम भिन्न अर्थ प्रतीत हो जाते हैं उसी प्रकार सामान्य और नहीं चल सकता है । जैस भाषा छह कारकमय होती विशेष रूपसे वस्तुमें अनन्त धर्म हैं । परन्तु द्रव्य,क्षेत्र, है अर्थात् कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा काल तथा भावकी अपेक्षास जिस समय जिस धर्मकी अधिकरण-मय होती है और कारकोंक विना भाषाशैली विवक्षा होती है उम समय उस धर्मकी मुख्यता रहने कभी भी व्यवहारयोग्य नहीं गिनी जा मकती वैसे ही के कारण अन्य शेप धमों की गौणता हो जानी है। वस्तुको अनेक धर्मात्मक न माननंसे, शब्दमें एक काल जैसे उपयुक्त दृष्टान्नमें 'ह' धातुके माथ प्रत्यय वा में एक ही अर्थकी सामर्थ्य न मानस तथा प्रतिपादन- उपसर्ग लगानम धातुगत मूल अर्थ गौण पर जाना है में गण मुख्य-शैलीका आश्रय न माननेस किसी प्रकार और प्रत्ययगत तथा उपमर्गगन अर्थ प्रत्येक समय का वाचणवाचक व्यवहार भी नहीं बन सकता है। प्रमुम्ब हाना जाता है, वैसे ही वस्तुगत विवक्षित धर्म
जिस प्रकार जो लोग व्याकरणको समझते हैं मुख्य और अविवक्षित धर्मोको गौण हो जानस शब्दों अथवा जो लाग नहीं समझते हैं वे सब भाषा छह के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थोका वाच्य-वाचक-व्यवहार कारकमय ही बालन हैं उसी प्रकार अनकान्तका स्व- होता जाता है । जब तक वस्तुमें द्रव्य, क्षेत्र, काल रूप समझने वाले और न समझने वाले दोनोंको ही नथा भावकी अपेक्षासे गुणमुख्य व्यवस्थाको विवक्षा अनकान्तका आश्रय लेना पड़ता है। अनेकान्तवादका नहीं की जानी है तब तक अनेकान्तवारकी शैलीका ही मग नाम 'अपंक्षावाद' है । अपेक्षावादका आ- परिचय ही नहीं हो सकता है। सामान्यको मुख्य और भय लिये बिना कोई वक्ता वा श्रीता वस्तुके स्वरूपको विशेषको गौण मान कर विधिका गांतक 'मस्ति' न तो कह ही सकता है और न समझ ही सकता है। और निषेधका द्योतक 'नाम्नि शन्नका प्रयोग करके