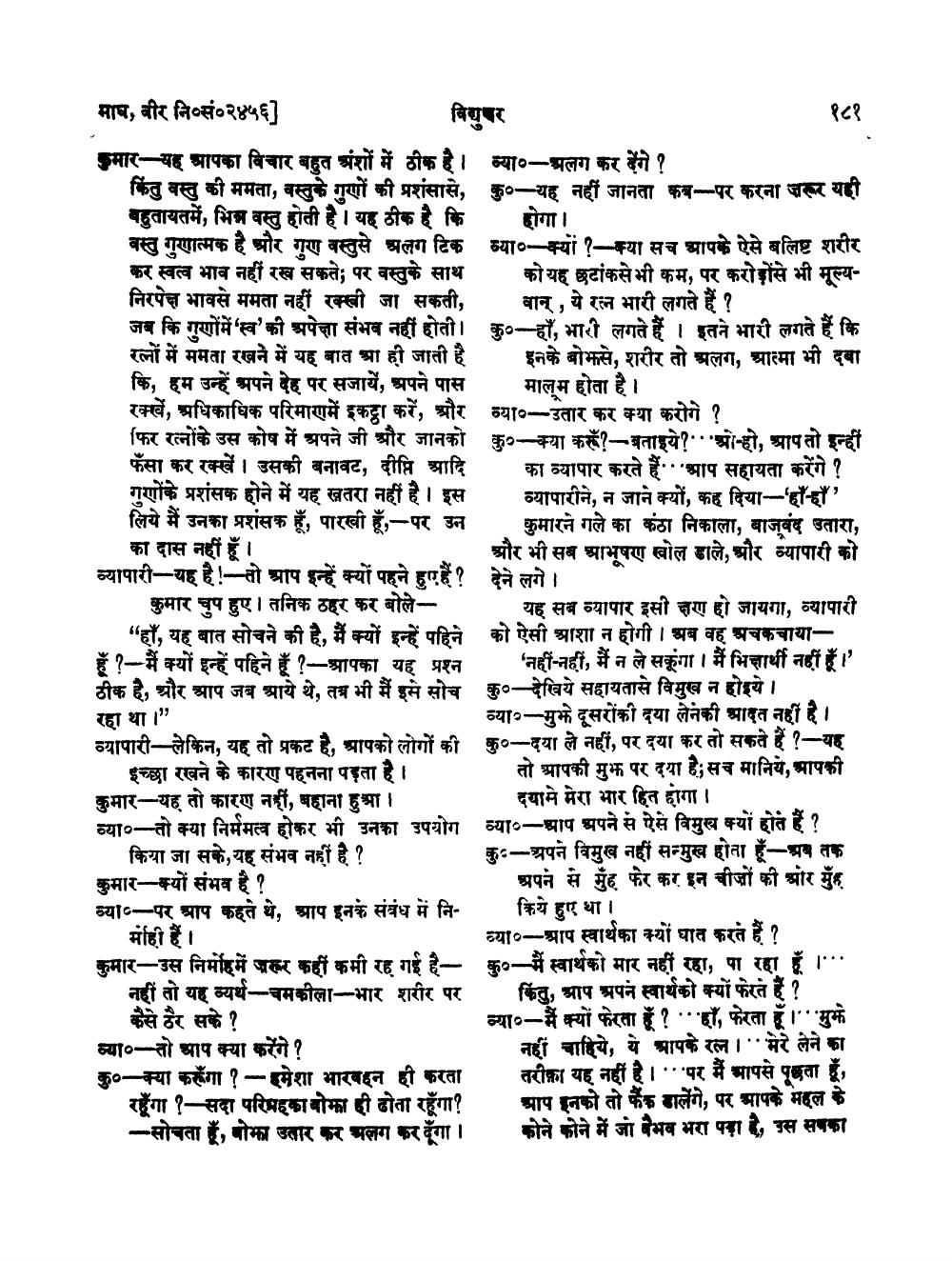________________
विद्युचर
माघ, वीर नि०सं० २४५६ ]
कुमार - यह आपका विचार बहुत अंशों में ठीक है । किंतु वस्तु की ममता, वस्तुके गुणों की प्रशंसासे, बहुतायत में, भिन्न वस्तु होती है। यह ठीक है कि वस्तु गुणात्मक है और गुण वस्तुसे अलग टिक कर स्वत्व भाव नहीं रख सकते; पर वस्तुके साथ निरपेक्ष भावसे ममता नहीं रक्खी जा सकती, जब कि गुणों में 'स्व' की अपेक्षा संभव नहीं होती। रत्नों में ममता रखने में यह बात आ ही जाती है कि, हम उन्हें अपने देह पर सजायें, अपने पास रक्खें, अधिकाधिक परिमाण में इकट्ठा करें, और फिर रत्नोंके उस कोष में अपने जी और जानको फँसा कर रक्खें । उसकी बनावट, दीप्ति आदि गुणोंके प्रशंसक होने में यह खतरा नहीं है । इस लिये मैं उनका प्रशंसक हूँ, पारखी हूँ,का दास नहीं हूँ । व्यापारी - यह है ! तो आप इन्हें क्यों पहने हुए हैं ? कुमार चुप हुए। तनिक ठहर कर बोले"हाँ, यह बात सोचने की है, मैं क्यों इन्हें पहिने हूँ ? - मैं क्यों इन्हें पहिने हूँ ? - आपका यह प्रश्न ठीक है, और आप जब आये थे, तब भी मैं इसे सोच रहा था।"
- पर उन
-
व्यापारी - लेकिन, यह तो प्रकट है, आपको लोगों की
इच्छा रखने के कारण पहनना पड़ता है । कुमार - यह तो कारण नहीं, बहाना हुआ। व्या० - तो क्या निर्ममत्व होकर भी उनका उपयोग किया जा सके, यह संभव नहीं है ? कुमार- क्यों संभव है ?
व्यापर आप कहते थे, आप इनके संबंध में निमही हैं।
कुमार-उस निर्मोह में जरूर कहीं कमी रह गई है— नहीं तो यह व्यर्थ - चमकीला - भार शरीर पर कैसे ठैर सके ?
व्या० तो आप क्या करेंगे ?
कु० - क्या करूँगा ? - हमेशा भारवहन ही करता रहूँगा ? - सदा परिग्रहका बोझा ही ढोता रहूँगा? -सोचता हूँ, बोझा उतार कर अलग कर दूँगा ।
१८१
व्या० - अलग कर देंगे ?
कु० - यह नहीं जानता कब पर करना जरूर यही होगा ।
व्या०—क्यों ? क्या सच आपके ऐसे बलिष्ट शरीर को यह छटांकसे भी कम पर करोड़ोंसे भी मूल्यये रत्न भारी लगते हैं ?
वान्
कु० - हाँ, भारी लगते हैं । इतने भारी लगते हैं कि इनके बोझसे, शरीर तो अलग, आत्मा भी दबा मालूम होता है ।
व्या० - उतार कर क्या करोगे ?
कु० - क्या करूँ ? बताइये? श्रो- हो, श्राप तो इन्हीं का व्यापार करते हैं आप सहायता करेंगे ? व्यापारीने, न जाने क्यों, कह दिया- 'हाँ-हाँ' कुमारने गले का कंठा निकाला, बाजूबंद उतारा, और भी सब आभूषण खोल डाले, और व्यापारी को देने लगे ।
यह सब व्यापार इसी क्षण हो जायगा, व्यापारी को ऐसी आशा न होगी । अब वह अचकचाया
'नहीं-नहीं, मैं न ले सकूंगा । मैं भिक्षार्थी नहीं हूँ ।' कु० – देखिये सहायतासे विमुख न होइये । व्याः- मुझे दूसरोंकी दया लेकी आदत नहीं है। कु० - दया ले नहीं, पर दया कर तो सकते हैं ? - यह
तो आपकी मुझ पर दया है; सच मानिये, आपकी दया मेरा भार हित होगा ।
व्या० - चाप अपने से ऐसे विमुख क्यों होते हैं ? कुः - अपने विमुख नहीं सन्मुख होता हूँ- अब तक अपने से मुँह फेर कर इन चीजों की ओर मुँह किये हुए था।
..
व्या० - आप स्वार्थका क्यों घात करते हैं ? कु० – मैं स्वार्थको मार नहीं रहा, पा रहा हूँ ।" किंतु, आप अपने स्वार्थको क्यों फेरते हैं ? व्या० - मैं क्यों फेरता हूँ ? हाँ, फेरता हूँ। मुझे नहीं चाहिये, ये आपके रत्न । मेरे लेने का तरीका यह नहीं है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप इनको तो फैंक डालेंगे, पर आपके महल के कोने कोने में जो वैभव भरा पड़ा है, उस सबका