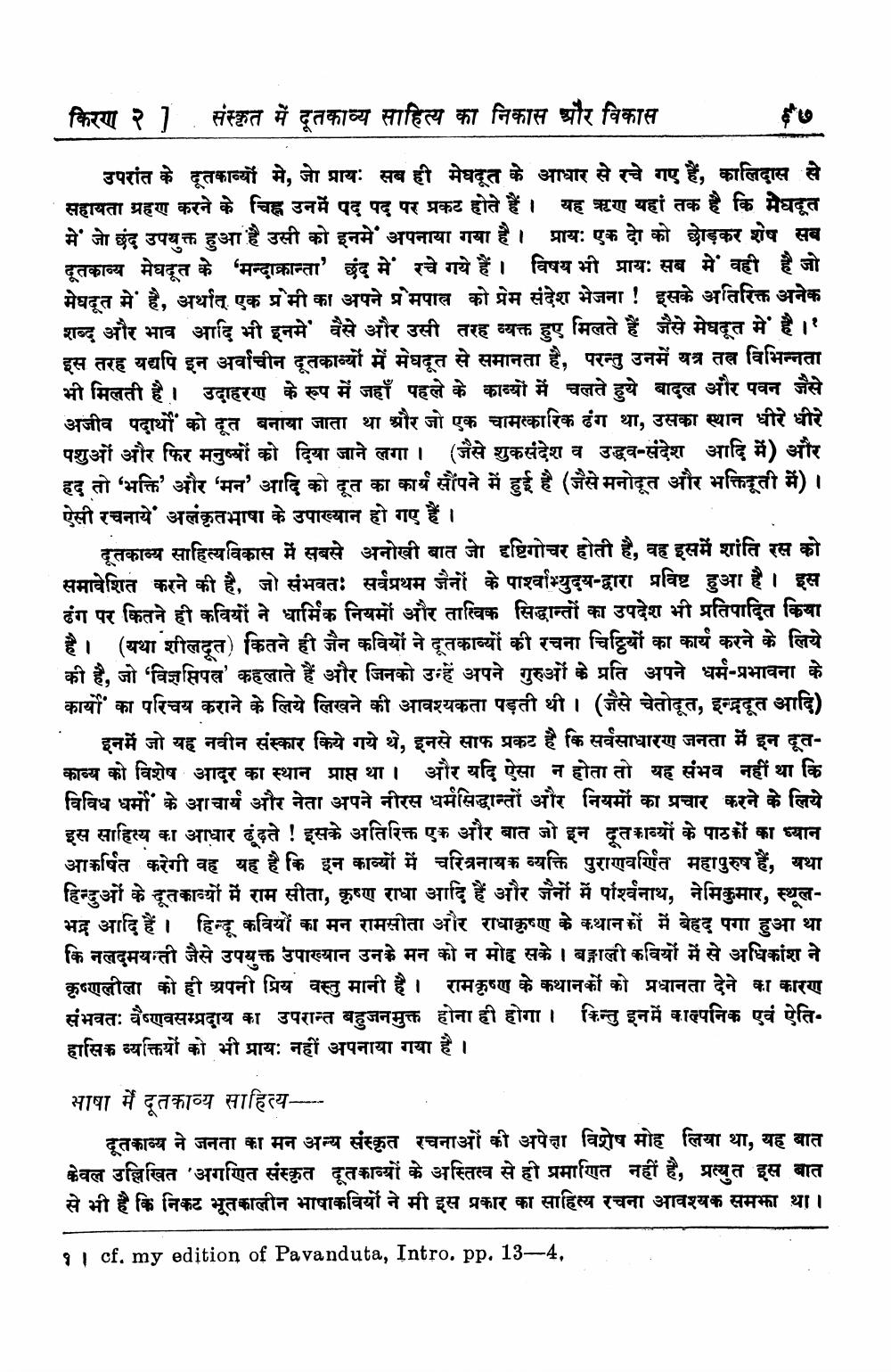________________
किरण २] संस्कृत में दूतकाव्य साहित्य का निकास और विकास
उपरांत के दूतकाव्यों मे, जो प्रायः सब ही मेघदूत के आधार से रचे गए हैं, कालिदास से सहायता ग्रहण करने के चिह्न उनमें पद पद पर प्रकट होते हैं। यह ऋण यहां तक है कि मेघदूत में जो छंद उपयुक्त हुआ है उसी को इनमें अपनाया गया है। प्रायः एक दो को छोड़कर शेष सब दूतकाव्य मेघदूत के 'मन्दाक्रान्ता' छंद में रचे गये हैं। विषय भी प्रायः सब में वही है जो मेघदूत में है, अर्थात् एक प्रेमी का अपने प्रेमपात्र को प्रेम संदेश भेजना ! इसके अतिरिक्त अनेक शब्द और भाव आदि भी इनमें वैसे और उसी तरह व्यक्त हुए मिलते हैं जैसे मेघदूत में है।' इस तरह यद्यपि इन अर्वाचीन दूतकाव्यों में मेघदूत से समानता है, परन्तु उनमें यत्र तत्र विभिन्नता भी मिलती है। उदाहरण के रूप में जहाँ पहले के काव्यों में चलते हुये बादल और पवन जैसे अजीव पदार्थों को दूत बनाया जाता था और जो एक चामत्कारिक ढंग था, उसका स्थान धीरे धीरे पशुओं और फिर मनुष्यों को दिया जाने लगा। (जैसे शुकसंदेश व उद्धव-संदेश आदि में) और हद तो 'भक्ति' और 'मन' आदि को दूत का कार्य सौंपने में हुई है (जैसे मनोदूत और भक्तिदूती में)। ऐसी रचनायें अलंकृतभाषा के उपाख्यान हो गए हैं।
दूतकाव्य साहित्यविकास में सबसे अनोखी बात जो दृष्टिगोचर होती है, वह इसमें शांति रस को समावेशित करने की है, जो संभवतः सर्वप्रथम जैनों के पार्वाभ्युदय-द्वारा प्रविष्ट हुआ है। इस ढंग पर कितने ही कवियों ने धार्मिक नियमों और ताविक सिद्धान्तों का उपदेश भी प्रतिपादित किया है। (यथा शीलदूत) कितने ही जैन कवियों ने दूतकाव्यों की रचना चिट्ठियों का कार्य करने के लिये की है, जो 'विज्ञप्तिपत्र' कहलाते हैं और जिनको उन्हें अपने गुरुओं के प्रति अपने धर्म-प्रभावना के कार्यों का परिचय कराने के लिये लिखने की आवश्यकता पड़ती थी। (जैसे चेतोदूत, इन्द्रदूत आदि) - इनमें जो यह नवीन संस्कार किये गये थे, इनसे साफ प्रकट है कि सर्वसाधारण जनता में इन दूतकाव्य को विशेष आदर का स्थान प्राप्त था। और यदि ऐसा न होता तो यह संभव नहीं था कि विविध धर्मों के आचार्य और नेता अपने नीरस धर्मसिद्धान्तों और नियमों का प्रचार करने के लिये इस साहित्य का आधार ढूंढ़ते ! इसके अतिरिक्त एक और बात जो इन दूतकाव्यों के पाठकों का ध्यान आकर्षित करेगी वह यह है कि इन काव्यों में चरित्रनायक व्यक्ति पुराणवर्णित महापुरुष हैं, यथा हिन्दुओं के दूतकाव्यों में राम सीता, कृष्ण राधा आदि हैं और जैनों में पार्श्वनाथ, नेमिकुमार, स्थूलभद्र आदि हैं। हिन्दू कवियों का मन रामसीता और राधाकृष्ण के कथानकों में बेहद पगा हुआ था कि नलदमयाती जैसे उपयुक्त उपाख्यान उनके मन को न मोह सके । बङ्गाली कवियों में से अधिकांश ने कृष्णलीला को ही अपनी प्रिय वस्तु मानी है। रामकृष्ण के कथानकों को प्रधानता देने का कारण संभवतः वैष्णवसम्प्रदाय का उपरान्त बहुजनमुक्त होना ही होगा। किन्तु इनमें काल्पनिक एवं ऐति. हासिक व्यक्तियों को भी प्रायः नहीं अपनाया गया है ।
भाषा में दूतकाव्य साहित्य---
दूतकाव्य ने जनता का मन अन्य संस्कृत रचनाओं की अपेक्षा विशेष मोह लिया था, यह बात केवल उल्लिखित 'अगणित संस्कृत दूतकाव्यों के अस्तित्व से ही प्रमाणित नहीं है, प्रत्युत इस बात से भी है कि निकट भूतकालीन भाषाकवियों ने मी इस प्रकार का साहित्य रचना आवश्यक समझा था।
१। cf. my edition of Pavanduta, Intro. pp. 13-4,