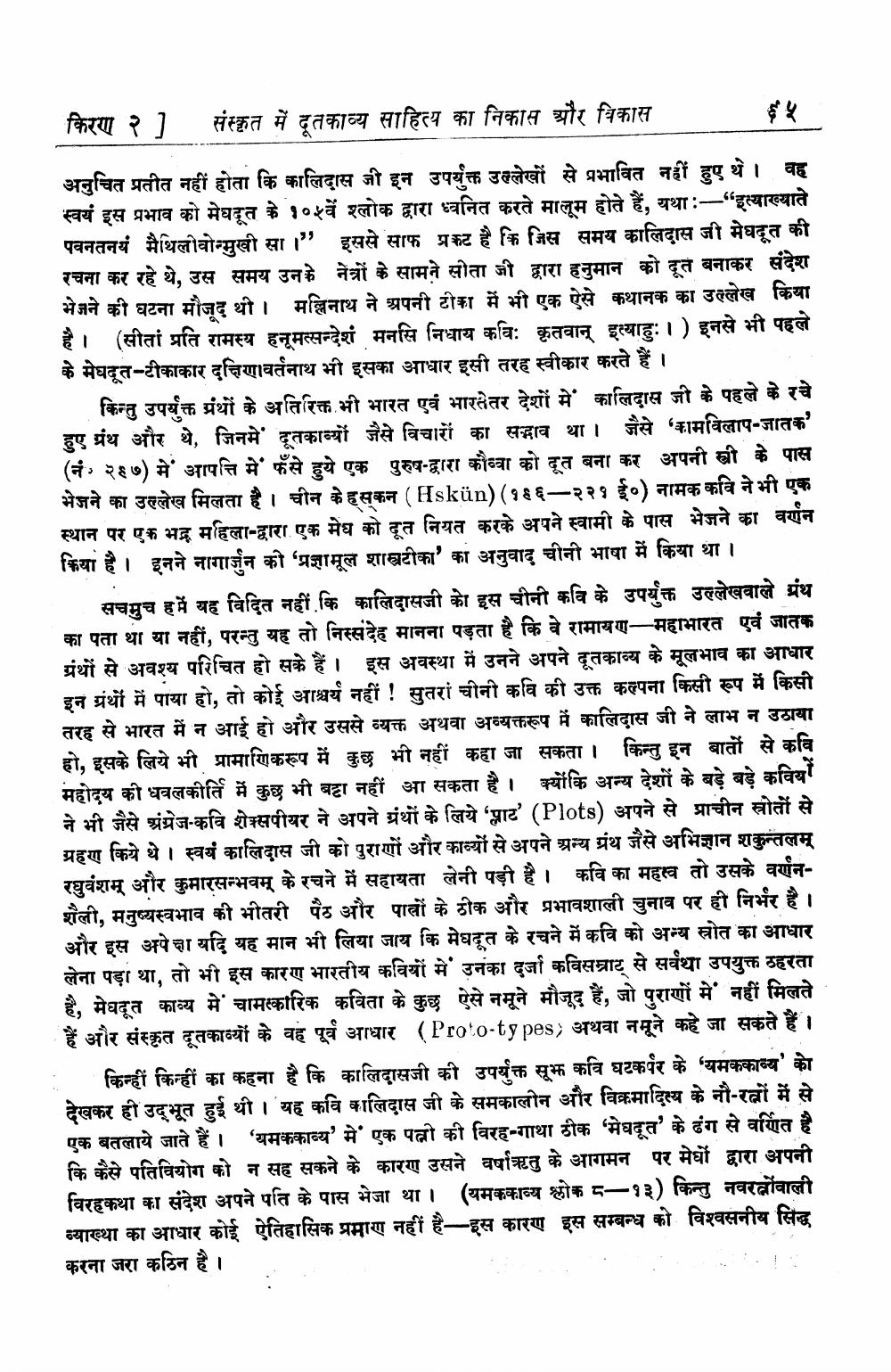________________
किरण २]
संस्कृत में दूतकाव्य साहित्य का निकास और विकास
अनुचित प्रतीत नहीं होता कि कालिदास जी इन उपर्युक्त उल्लेखों से प्रभावित नहीं हुए थे। वह स्वयं इस प्रभाव को मेघदूत के १०वें श्लोक द्वारा ध्वनित करते मालूम होते हैं, यथा:-"इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा।" इससे साफ प्रकट है कि जिस समय कालिदास जी मेघदूत की रचना कर रहे थे, उस समय उनके नेत्रों के सामने सीता जी द्वारा हनुमान को दूत बनाकर संदेश भेजने की घटना मौजूद थी। मल्लिनाथ ने अपनी टीका में भी एक ऐसे कथानक का उल्लेख किया है। (सीतां प्रति रामस्य हनूमत्सन्देशं मनसि निधाय कविः कृतवान् इत्याहुः । ) इनसे भी पहले के मेघदूत-टीकाकार दक्षिणावर्तनाथ भी इसका आधार इसी तरह स्वीकार करते हैं ।।
किन्तु उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त भी भारत एवं भारतेतर देशों में कालिदास जी के पहले के रचे हुए ग्रंथ और थे, जिनमें दूतकाव्यों जैसे विचारों का सद्भाव था। जैसे 'कामविलाप-जातक' (नं. २६७) में आपत्ति में फंसे हुये एक पुरुष-द्वारा कौव्वा को दूत बना कर अपनी स्त्री के पास भेजने का उल्लेख मिलता है। चीन के हस्कन (Hskin) (१९६-२२१ ई०) नामक कवि ने भी एक स्थान पर एक भद्र महिला-द्वारा एक मेघ को दूत नियत करके अपने स्वामी के पास भेजने का वर्णन किया है। इनने नागार्जुन को 'प्रज्ञामूल शास्त्रटीका' का अनुवाद चीनी भाषा में किया था।
सचमुच हमें यह विदित नहीं कि कालिदासजी को इस चीनी कवि के उपर्युक्त उल्लेखवाले ग्रंथ का पता था या नहीं, परन्तु यह तो निस्संदेह मानना पड़ता है कि वे रामायण-महाभारत एवं जातक ग्रंथों से अवश्य परिचित हो सके हैं। इस अवस्था में उनने अपने दूतकाव्य के मूलभाव का आधार इन ग्रंथों में पाया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं ! सुतरां चीनी कवि की उक्त कल्पना किसी रूप में किसी तरह से भारत में न आई हो और उससे व्यक्त अथवा अव्यक्तरूप में कालिदास जी ने लाभ न उठाया हो, इसके लिये भी प्रामाणिकरूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किन्तु इन बातों से कवि महोदय की धवलकीर्ति में कुछ भी बट्टा नहीं आ सकता है। क्योंकि अन्य देशों के बड़े बड़े कवियों ने भी जैसे अंग्रेज-कवि शेक्सपीयर ने अपने ग्रंथों के लिये 'प्लाट' (Plots) अपने से प्राचीन स्रोतों से ग्रहण किये थे। स्वयं कालिदास जी को पुराणों और काव्यों से अपने अन्य ग्रंथ जैसे अभिज्ञान शकुन्तलम् रघुवंशम् और कुमारसम्भवम् के रचने में सहायता लेनी पड़ी है। कवि का महत्व तो उसके वर्णनशैली, मनुष्यस्वभाव की भीतरी पैठ और पात्रों के ठीक और प्रभावशाली चुनाव पर ही निर्भर है।
और इस अपेक्षा यदि यह मान भी लिया जाय कि मेघदूत के रचने में कवि को अन्य स्रोत का आधार लेना पड़ा था, तो भी इस कारण भारतीय कवियों में उनका दर्जा कविसम्राट से सर्वथा उपयुक्त ठहरता है, मेघदूत काव्य में चामत्कारिक कविता के कुछ ऐसे नमूने मौजूद हैं, जो पुराणों में नहीं मिलते हैं और संस्कृत दूतकाव्यों के वह पूर्व आधार (Proto-ty pes) अथवा नमूने कहे जा सकते हैं।
किन्हीं किन्हीं का कहना है कि कालिदासजी की उपर्युक्त सूझ कवि घटकर के 'यमककाव्य' को देखकर ही उद्भूत हुई थी। यह कवि कालिदास जी के समकालीन और विक्रमादित्य के नौ-रत्नों में से एक बतलाये जाते हैं। 'यमककाव्य' में एक पत्नी की विरह-गाथा ठीक 'मेघदूत' के ढंग से वर्णित है कि कैसे पतिवियोग को न सह सकने के कारण उसने वर्षाऋतु के आगमन पर मेघों द्वारा अपनी विरहकथा का संदेश अपने पति के पास भेजा था। (यमककाव्य श्लोक ८-१३) किन्तु नवरत्नोंवाली व्याख्था का आधार कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है-इस कारण इस सम्बन्ध को विश्वसनीय सिद्ध करना जरा कठिन है।