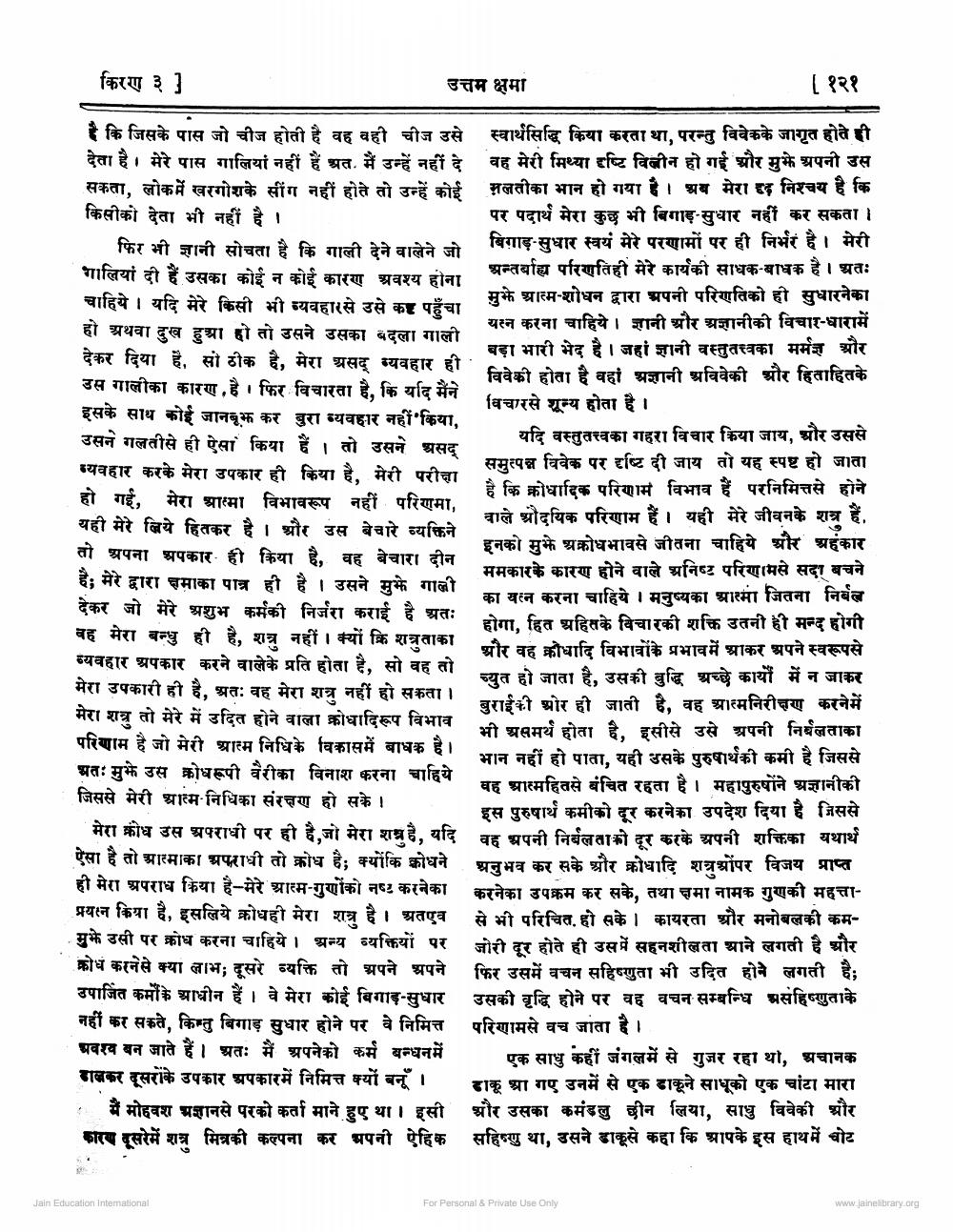________________
किरण ३]
उत्तम क्षमा
[१२१
है कि जिसके पास जो चीज होती है वह वही चीज उसे स्वार्थसिद्धि किया करता था, परन्तु विवेकके जागृत होते ही देता है। मेरे पास गालियां नहीं हैं अत. मैं उन्हें नहीं दे वह मेरी मिथ्या दृष्टि विलीन हो गई और मुझे अपनी उस सकता, लोकमें खरगोशके सींग नहीं होते तो उन्हें कोई ग़लतीका भान हो गया है। अब मेरा द निश्चय है कि किसीको देता भी नहीं है।
पर पदार्थ मेरा कुछ भी बिगाड़-सुधार नहीं कर सकता। फिर भी ज्ञानी सोचता है कि गाली देने वालेने जो
बिगाड़-सुधार स्वयं मेरे परणामों पर ही निर्भर है। मेरी गालियां दी हैं उसका कोई न कोई कारण अवश्य होना
अन्तर्बाह्य परिणतिही मेरे कार्यकी साधक-बाधक है । अतः चाहिये। यदि मेरे किसी भी व्यवहारसे उसे कह पहुँचा
मुझे अात्म-शोधन द्वारा अपनी परिणतिको ही सुधारनेका हो अथवा दुख हुआ हो तो उसने उसका बदला गाली
यत्न करना चाहिये। ज्ञानी और अज्ञानीकी विचार-धारामें देकर दिया है, सो ठीक है, मेरा असद् व्यवहार ही
बड़ा भारी भेद है। जहां ज्ञानी वस्तुतत्वका मर्मज्ञ और
विवेकी होता है वहां अज्ञानी अविवेकी और हिताहितके उस गालीका कारण है। फिर विचारता है, कि यदि मैंने इसके साथ कोई जानबूझ कर बुरा व्यवहार नहीं किया,
विचारसे शून्य होता है। उसने गलतीसे ही ऐसा किया हैं। तो उसने असद्
यदि वस्तुतत्त्वका गहरा विचार किया जाय, और उससे
समुत्पन्न विवेक पर दृष्टि दी जाय तो यह स्पष्ट हो जाता व्यवहार करके मेरा उपकार ही किया है, मेरी परीक्षा
है कि क्रोधादिक परिणाम विभाव हैं परनिमित्तसे होने हो गई, मेरा आस्मा विभावरूप नहीं परिणमा, यही मेरे लिये हितकर है। और उस बेचारे व्यक्तिने
वाले औदयिक परिणाम हैं। यही मेरे जीवनके शत्र हैं, तो अपना अपकार ही किया है, वह बेचारा दीन
इनको मुझे अक्रोधभावसे जीतना चाहिये और अहंकार
ममकारके कारण होने वाले अनिष्ट परिणामसे सदा बचने है; मेरे द्वारा क्षमाका पात्र ही है । उसने मुझे गाली
का यत्न करना चाहिये । मनुष्यका पात्मा जितमा निर्बल देकर जो मेरे अशुभ कर्मकी निर्जरा कराई है अतः
होगा, हित अहितके विचारकी शक्ति उतनी ही मन्द होगी वह मेरा बन्धु ही है, शत्रु नहीं । क्यों कि शत्रुताका
और वह क्रोधादि विभावोंके प्रभाव में आकर अपने स्वरूपसे व्यवहार अपकार करने वालेके प्रति होता है, सो वह तो मेरा उपकारी ही है, अत: वह मेरा शत्रु नहीं हो सकता।
च्युत हो जाता है, उसकी बुद्धि अच्छे कार्यों में न जाकर
बुराईकी ओर ही जाती है, वह अात्मनिरीक्षण करने में मेरा शत्रु तो मेरे में उदित होने वाला क्रोधादिरूप विभाव
भी असमर्थ होता है, इसीसे उसे अपनी निर्बलताका परिणाम है जो मेरी श्रात्म निधिके विकासमें बाधक है।
भान नहीं हो पाता, यही उसके पुरुषार्थकी कमी है जिससे अतः मुझे उस क्रोधरूपी वैरीका विनाश करना चाहिये
वह प्रात्महितसे बंचित रहता है। महापुरुषोंने अज्ञानीकी जिससे मेरी श्रात्म-निधिका संरक्षण हो सके।
इस पुरुषार्थ कमीको दूर करनेका उपदेश दिया है जिससे मेरा क्रोध उस अपराधी पर ही है,जो मेरा शन्न है, यदि वह अपनी निर्बलताको दूर करके अपनी शक्तिका यथार्थ ऐसा है तो आत्माका अपराधी तो क्रोध है; क्योंकि वोधने अनुभव कर सके और क्रोधादि शवोंपर विजय प्राप्त ही मेरा अपराध किया है-मेरे प्रात्म-गुणोंको नष्ट करनेका करनेका उपक्रम कर सके, तथा क्षमा नामक गुणकी महत्ताप्रयत्न किया है, इसलिये क्रोधही मेरा शत्र है। अतएव से भी परिचित.हो सके। कायरता और मनोबलकी कममुझे उसी पर क्रोध करना चाहिये। अन्य व्यक्तियों पर जोरी दूर होते ही उसमें सहनशीलता पाने लगती है और क्रोध करनेसे क्या लाभ; दूसरे व्यक्ति तो अपने अपने फिर उसमें वचन सहिष्णुता भी उदित होने लगती है; उपार्जित कर्मों के आधीन हैं। वे मेरा कोई विगाड़-सुधार उसकी वृद्धि होने पर वह वचन सम्बन्धि असहिष्णुताके नहीं कर सकते, किन्तु बिगाड़ सुधार होने पर वे निमित्त परिणामसे बच जाता है। अवश्य बन जाते हैं। अतः मैं अपनेको कर्म बन्धनमें एक साथ कहीं जंगल में से गुजर रहा था, अचानक बालकर दूसरोंके उपकार अपकारमें निमित्त क्यों बनूं। डाकू पा गए उनमें से एक ढाकूने साधूको एक चांटा मारा - मैं मोहवश अज्ञानसे परको कर्ता माने हुए था। इसी और उसका कमंडलु छीन लिया, साधु विवेकी और कारण दूसरेमें शत्रु मित्रकी कल्पना कर अपनी ऐहिक सहिष्णु था, उसने डाकूसे कहा कि आपके इस हाथमें चोट
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org