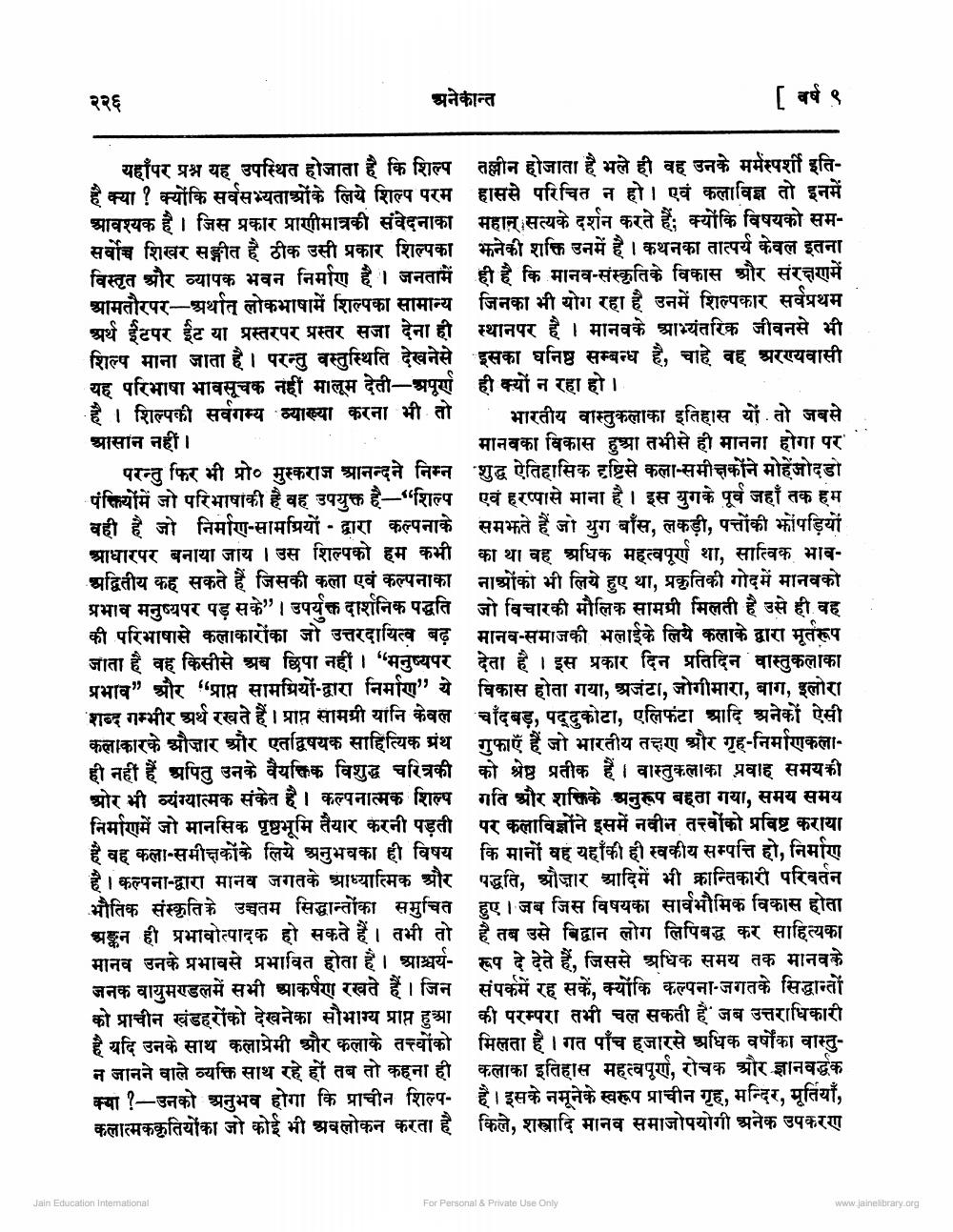________________
२२६
अनेकान्त
[ वर्ष ९
यहाँपर प्रश्न यह उपस्थित होजाता है कि शिल्प तल्लीन होजाता है भले ही वह उनके मर्मस्पर्शी इतिहै क्या ? क्योंकि सर्वसभ्यताओंके लिये शिल्प परम हाससे परिचित न हो। एवं कलाविज्ञ तो इनमें
आवश्यक है। जिस प्रकार प्राणीमात्रकी संवेदनाका महान् सत्यके दर्शन करते हैं; क्योंकि विषयको सर्वोच्च शिखर सङ्गीत है ठीक उसी प्रकार शिल्पका भनेकी शक्ति उनमें है । कथनका तात्पर्य केवल इतना विस्तृत और व्यापक भवन निर्माण है । जनतामें ही है कि मानव-संस्कृतिके विकास और संरक्षणमें आमतौरपर-अर्थात् लोकभाषामें शिल्पका सामान्य जिनका भी योग रहा है उनमें शिल्पकार सर्वप्रथम अर्थ ईटपर ईट या प्रस्तरपर प्रस्तर सजा देना ही स्थानपर है । मानवके आभ्यंतरिक जीवनसे भी शिल्प माना जाता है। परन्तु वस्तुस्थिति देखनेसे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है, चाहे वह अरण्यवासी यह परिभाषा भावसूचक नहीं मालूम देती-अपूर्ण ही क्यों न रहा हो। है। शिल्पकी सर्वगम्य व्याख्या करना भी तो भारतीय वास्तुकलाका इतिहास यों तो जबसे आसान नहीं।
मानवका विकास हुआ तभीसे ही मानना होगा पर' परन्तु फिर भी प्रो० मुस्कराज आनन्दने निम्न शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से कला-समीक्षकोंने मोहेंजोदडो पंक्तियों में जो परिभाषाकी है वह उपयुक्त है-"शिल्प एवं हरप्पासे माना है। इस युगके पूर्व जहाँ तक हम वही है जो निर्माण-सामग्रियों - द्वारा कल्पनाके समझते हैं जो युग बाँस, लकड़ी, पत्तोंकी झोंपड़ियों आधारपर बनाया जाय । उस शिल्पको हम कभी का था वह अधिक महत्वपूर्ण था, सात्विक भावअद्वितीय कह सकते हैं जिसकी कला एवं कल्पनाका नाओंको भी लिये हुए था, प्रकृतिकी गोदमें मानवको प्रभाव मनुष्यपर पड़ सके"। उपर्युक्त दार्शनिक पद्धति जो विचारकी मौलिक सामग्री मिलती है उसे ही वह की परिभाषासे कलाकारोंका जो उत्तरदायित्व बढ़ मानव-समाजकी भलाई के लिये कलाके द्वारा मूर्तरूप जाता है वह किसीसे अब छिपा नहीं। "मनुष्यपर देता है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वास्तुक प्रभाव" और "प्राप्त सामग्रियों-द्वारा निर्माण" ये विकास होता गया, अजंटा, जोगीमारा, बाग, इलोरा शब्द गम्भीर अर्थ रखते हैं। प्राप्त सामग्री यानि केवल चाँदबड़, पदुकोटा, एलिफंटा आदि अनेकों ऐसी कलाकारके औजार और एतद्विषयक साहित्यिक ग्रंथ गुफाएँ हैं जो भारतीय तक्षण और गृह-निर्माणकलाही नहीं हैं अपितु उनके वैयक्तिक विशुद्ध चरित्रकी को श्रेष्ठ प्रतीक हैं। वास्तुकलाका प्रवाह समयकी
ओर भी व्यंग्यात्मक संकेत है। कल्पनात्मक शिल्प गति और शक्तिके अनुरूप बहता गया, समय समय निर्माणमें जो मानसिक पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती पर कलाविज्ञोंने इसमें नवीन तत्त्वोंको प्रविष्ट कराया है वह कला-समीक्षकोंके लिये अनुभवका ही विषय कि मानों वह यहाँकी ही स्वकीय सम्पत्ति हो, निर्माण है। कल्पना-द्वारा मानव जगतके आध्यात्मिक और पद्धति, औजार आदिमें भी क्रान्तिकारी परिवर्तन भौतिक संस्कृति के उच्चतम सिद्धान्तोंका समुचित हुए। जब जिस विषयका सार्वभौमिक विकास होता अङ्कन ही प्रभावोत्पादक हो सकते हैं। तभी तो है तब उसे विद्वान लोग लिपिबद्ध कर साहित्यका मानव उनके प्रभावसे प्रभावित होता है। आश्चर्य- रूप दे देते हैं, जिससे अधिक समय तक मानवके जनक वायुमण्डलमें सभी आकर्षण रखते हैं। जिन संपर्कमें रह सकें, क्योंकि कल्पना-जगतके सिद्धान्तों को प्राचीन खंडहरोंको देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ की परम्परा तभी चल सकती है जब उत्तराधिकारी है यदि उनके साथ कलाप्रेमी और कलाके तत्वोंको मिलता है। गत पाँच हजारसे अधिक वर्षों का वास्तुन जानने वाले व्यक्ति साथ रहे हों तब तो कहना ही कलाका इतिहास महत्वपूर्ण, रोचक और ज्ञानवर्द्धक क्या ?-उनको अनुभव होगा कि प्राचीन शिल्प- है। इसके नमूनेके स्वरूप प्राचीन गृह, मन्दिर, मूर्तियाँ, कलात्मककृतियोंका जो कोई भी अवलोकन करता है किले, शस्त्रादि मानव समाजोपयोगी अनेक उपकरण
Jain Education Interational
For Personal & Private Use Only
www.lainelibrary.org