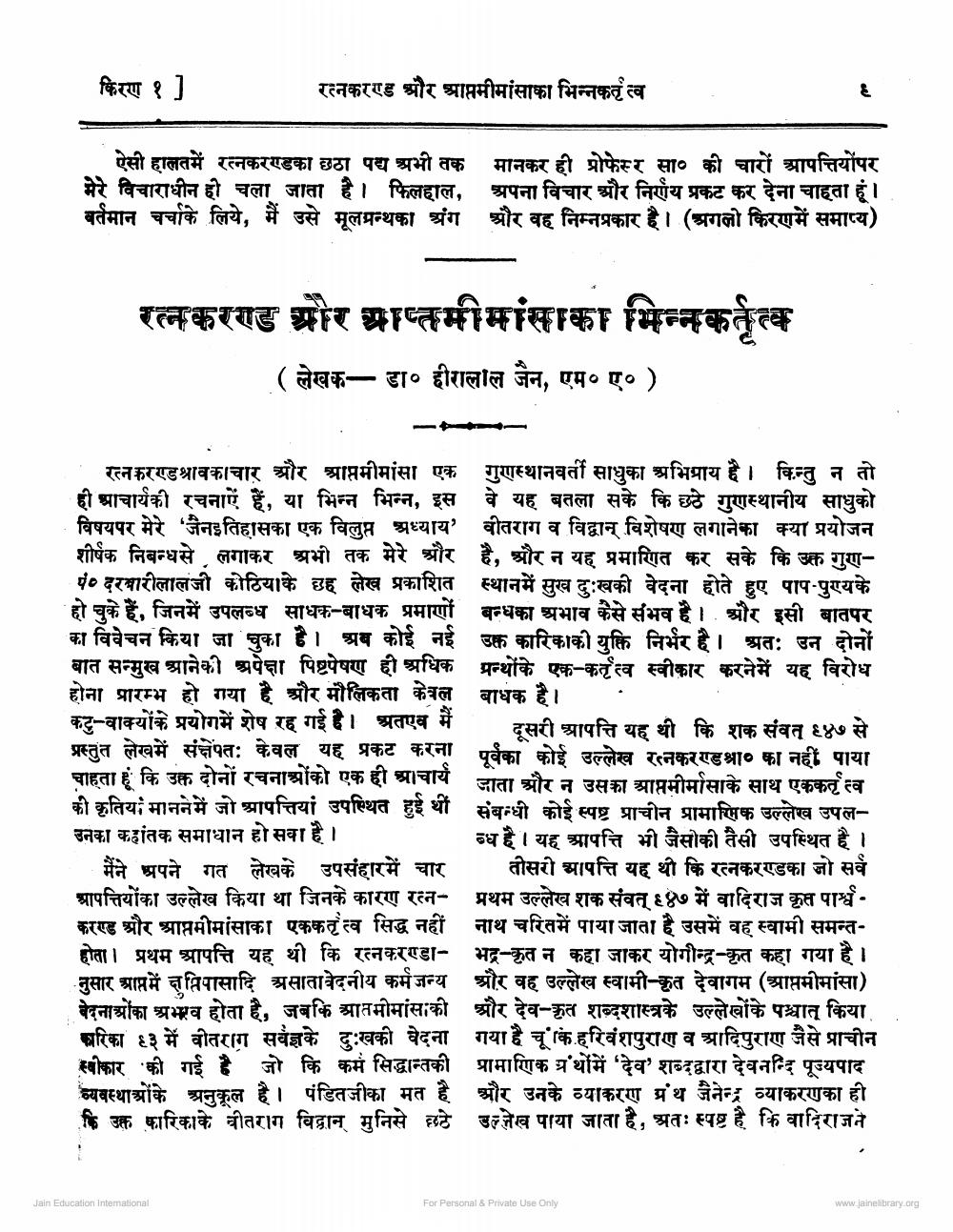________________
किरण १ ]
ऐसी हालत में रत्नकरण्डका छठा पद्य अभी तक मेरे विचाराधीन हो चला जाता है। फिलहाल, वर्तमान चर्चाके लिये, मैं उसे मूलग्रन्थका अंग
रत्नकरण्ड और श्राप्तमीमांसाका भिन्नकर्तृत्व
रत्नकरण्ड और प्राप्तमीमांसाका भिन्नकर्तृत्व
( लेखक - डा० हीरालाल जैन, एम० ए० )
रत्नकरण्ड श्रावकाचार और श्राप्तमीमांसा एक ही श्राचार्यकी रचनाऐं हैं, या भिन्न भिन्न, इस विषयपर मेरे 'जैन इतिहासका एक विलुप्त अध्याय' शीर्षक निबन्धसे लगाकर अभी तक मेरे और पं० दरबारीलालजी कोठिया के छह लेख प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें उपलब्ध साधक-बाधक प्रमाणों का विवेचन किया जा चुका 1 अब कोई नई बात सन्मुख आने की अपेक्षा पिष्टपेषण ही अधिक होना प्रारम्भ हो गया है और मौलिकता केवल कटु-वाक्योंके प्रयोगमें शेष रह गई है । अतएव मैं प्रस्तुत लेख में संक्षेपतः केवल यह प्रकट करना चाहता हूं कि उक्त दोनों रचनाओं को एक ही आचार्य की कृतियां मानने में जो आपत्तियां उपस्थित हुई थीं उनका कहांतक समाधान हो सका है ।
मैंने अपने गत लेखके उपसंहारमें चार आपत्तियों का उल्लेख किया था जिनके कारण रत्नकरण्ड और श्राप्तमीमांसाका एककर्तृत्व सिद्ध नहीं होता । प्रथम आपत्ति यह थी कि रत्नकरण्डानुसार आप्त में क्षुप्तिपासादि असातावेदनीय कर्मजन्य वेदनाओं का अभाव होता है, जबकि आतमीमांसा की कारका १३ में वीतराग सर्वज्ञके दुःखकी वेदना स्वीकार की गई है जो कि कर्म सिद्धान्तकी व्यवस्थाओं के अनुकूल है। पंडितजीका मत है कि उक्त कारिara ataराग विद्वान मुनिसे छठे
Jain Education International
मानकर ही प्रोफेसर सा० की चारों आपत्तियोंपर अपना विचार और निर्णय प्रकट कर देना चाहता हूं । और वह निम्नप्रकार है । (अगली किरणमें समाप्य )
1
गुणस्थानवर्ती साधुका अभिप्राय है । किन्तु न तो वे यह बतला सके कि छठे गुणस्थानीय साधुको वीतराग व विद्वान् विशेषण लगानेका क्या प्रयोजन है, और न यह प्रमाणित कर सके कि उक्त गुणस्थान में सुख दुःखकी वेदना होते हुए पाप-पुण्यके बन्धका अभाव कैसे संभव है । और इसी बातपर उक्त कारिकाकी युक्ति निर्भर है । अतः उन दोनों प्रन्थोंके एक- कर्तृत्व स्वीकार करने में यह विरोध बाधक है ।
दूसरी आपत्ति यह थी कि शक संवत् ६४७ से पूर्वका कोई उल्लेख रत्नकरण्ड श्रा० का नहीं पाया जाता और न उसका आप्तमीर्मासाके साथ एककर्तृत्व संबन्धी कोई स्पष्ट प्राचीन प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध है । यह आपत्ति भी जैसोकी तैसी उपस्थित है ।
तीसरी आपत्ति यह थी कि रत्नकरण्डका जो सर्व प्रथम उल्लेख शक संवत् ६४७ में वादिराज कृत पार्श्व - नाथ चरितमें पाया जाता है उसमें वह स्वामी समन्तभद्र-कृत न कहा जाकर योगीन्द्र - कृत कहा गया है । और वह उल्लेख स्वामी - कृत देवागम (आप्तमीमांसा) और देव कृत शब्दशास्त्र के उल्लेखोंके पश्चात् किया. गया है चूंकि हरिवंशपुराण व आदिपुराण जैसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों में 'देव' शब्दद्वारा देवनन्दि पूज्यपाद और उनके व्याकरण ग्रंथ जैनेन्द्र व्याकरणका ही उल्लेख पाया जाता है, अतः स्पष्ट है कि वादिराजने
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org