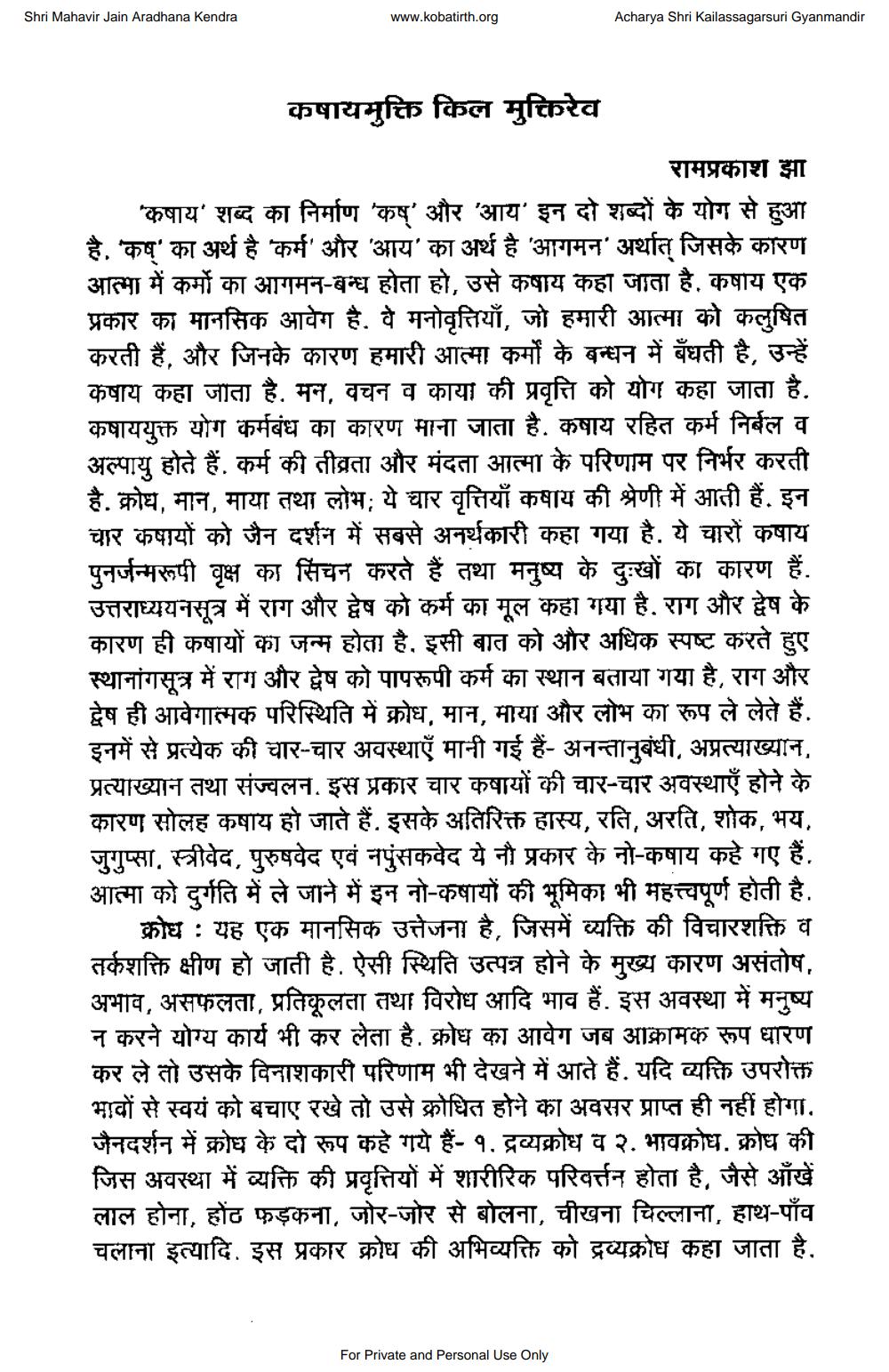________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
कषायमुक्ति किल मुक्तिरेव
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
रामप्रकाश झा
'कषाय' शब्द का निर्माण 'कष्' और 'आय' इन दो शब्दों के योग से हुआ है. 'कष' का अर्थ है 'कर्म' और 'आय' का अर्थ है 'आगमन' अर्थात् जिसके कारण आत्मा में कर्मों का आगमन -बन्ध होता हो, उसे कषाय कहा जाता है. कषाय एक प्रकार का मानसिक आवेग है. वे मनोवृत्तियाँ, जो हमारी आत्मा को कलुषित करती हैं, और जिनके कारण हमारी आत्मा कर्मों के बन्धन में बँधती है, उन्हें कषाय कहा जाता है. मन, वचन व काया की प्रवृत्ति को योग कहा जाता है. कषाययुक्त योग कर्मबंध का कारण माना जाता है. कषाय रहित कर्म निर्बल व अल्पायु होते हैं. कर्म की तीव्रता और मंदता आत्मा के परिणाम पर निर्भर करती है. क्रोध, मान, माया तथा लोभ; ये चार वृत्तियाँ कषाय की श्रेणी में आती हैं. इन चार कषायों को जैन दर्शन में सबसे अनर्थकारी कहा गया है. ये चारों कषाय पुनर्जन्मरूपी वृक्ष का सिंचन करते हैं तथा मनुष्य के दुःखों का कारण हैं. उत्तराध्ययनसूत्र में राग और द्वेष को कर्म का मूल कहा गया है. राग और द्वेष के कारण ही कषायों का जन्म होता है. इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए स्थानांगसूत्र में राग और द्वेष को पापरूपी कर्म का स्थान बताया गया है, राग और द्वेष ही आवेगात्मक परिस्थिति में क्रोध, मान, माया और लोभ का रूप ले लेते हैं. इनमें से प्रत्येक की चार-चार अवस्थाएँ मानी गई हैं- अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा संज्वलन. इस प्रकार चार कषायों की चार-चार अवस्थाएँ होने के कारण सोलह कषाय हो जाते हैं. इसके अतिरिक्त हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद एवं नपुंसकवेद ये नौ प्रकार के नो- कषाय कहे गए हैं. आत्मा को दुर्गति में ले जाने में इन नो-कषायों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है.
क्रोध : यह एक मानसिक उत्तेजना है, जिसमें व्यक्ति की विचारशक्ति व तर्कशक्ति क्षीण हो जाती है. ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के मुख्य कारण असंतोष, अभाव, असफलता, प्रतिकूलता तथा विरोध आदि भाव हैं. इस अवस्था में मनुष्य न करने योग्य कार्य भी कर लेता है. क्रोध का आवेग जब आक्रामक रूप धारण कर ले तो उसके विनाशकारी परिणाम भी देखने में आते हैं. यदि व्यक्ति उपरोक्त भावों से स्वयं को बचाए रखे तो उसे क्रोधित होने का अवसर प्राप्त ही नहीं होगा. जैनदर्शन में क्रोध के दो रूप कहे गये हैं- १. द्रव्यक्रोध व २. भावक्रोध. क्रोध की जिस अवस्था में व्यक्ति की प्रवृत्तियों में शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे आँखें लाल होना, होंठ फड़कना जोर-जोर से बोलना, चीखना चिल्लाना, हाथ-पाँव चलाना इत्यादि. इस प्रकार क्रोध की अभिव्यक्ति को द्रव्यक्रोध कहा जाता है.
For Private and Personal Use Only