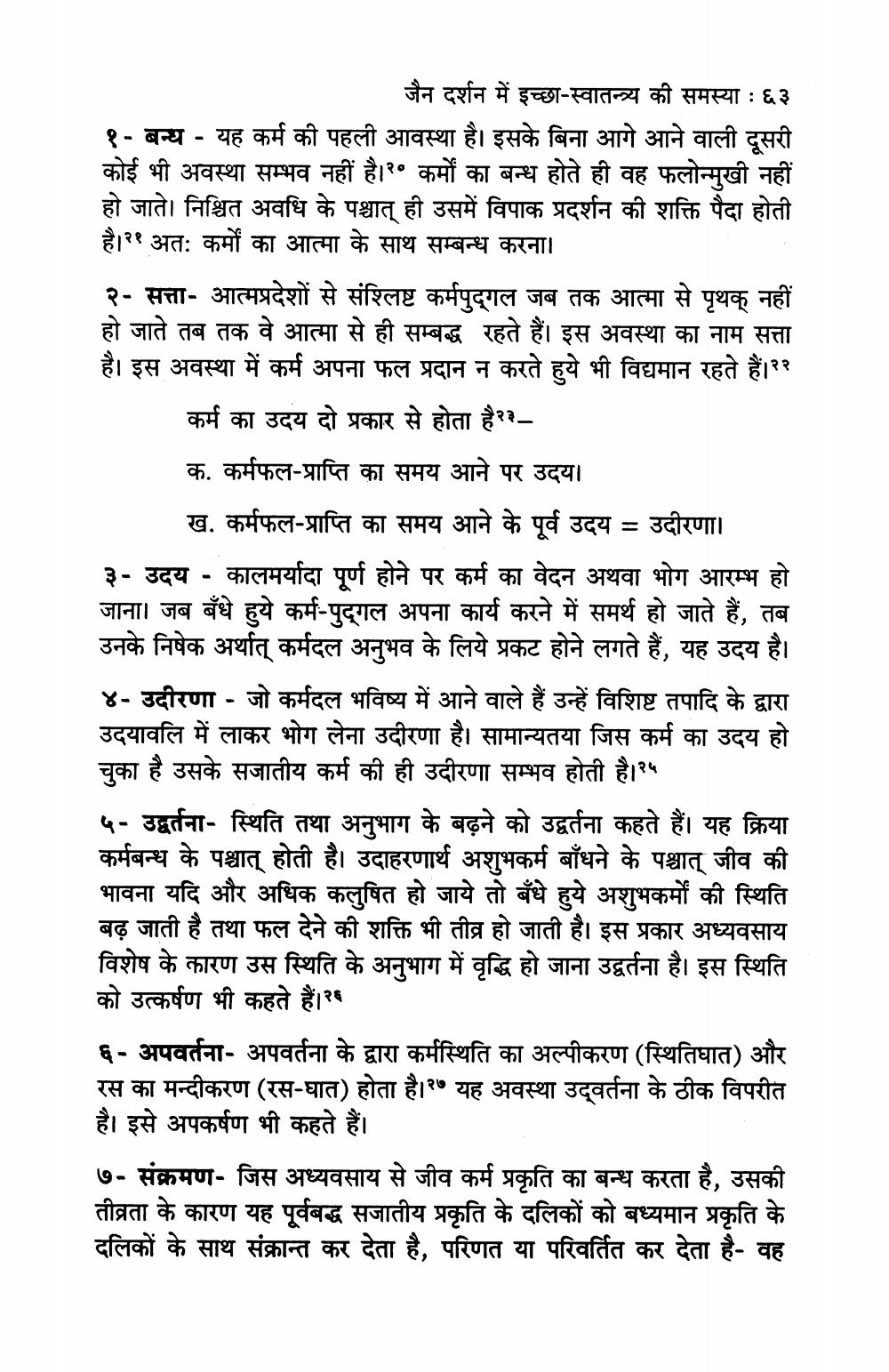________________
जैन दर्शन में इच्छा-स्वातन्त्र्य की समस्या : ६३ १- बन्य - यह कर्म की पहली आवस्था है। इसके बिना आगे आने वाली दूसरी कोई भी अवस्था सम्भव नहीं है।२० कर्मों का बन्ध होते ही वह फलोन्मुखी नहीं हो जाते। निश्चित अवधि के पश्चात् ही उसमें विपाक प्रदर्शन की शक्ति पैदा होती है।२१ अत: कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध करना। २- सत्ता- आत्मप्रदेशों से संश्लिष्ट कर्मपुद्गल जब तक आत्मा से पृथक् नहीं हो जाते तब तक वे आत्मा से ही सम्बद्ध रहते हैं। इस अवस्था का नाम सत्ता है। इस अवस्था में कर्म अपना फल प्रदान न करते हुये भी विद्यमान रहते हैं।२२
कर्म का उदय दो प्रकार से होता हैक. कर्मफल-प्राप्ति का समय आने पर उदय।
ख. कर्मफल-प्राप्ति का समय आने के पूर्व उदय = उदीरणा। ३- उदय - कालमर्यादा पूर्ण होने पर कर्म का वेदन अथवा भोग आरम्भ हो जाना। जब बँधे हुये कर्म-पुद्गल अपना कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं, तब उनके निषेक अर्थात् कर्मदल अनुभव के लिये प्रकट होने लगते हैं, यह उदय है। ४- उदीरणा - जो कर्मदल भविष्य में आने वाले हैं उन्हें विशिष्ट तपादि के द्वारा उदयावलि में लाकर भोग लेना उदीरणा है। सामान्यतया जिस कर्म का उदय हो चुका है उसके सजातीय कर्म की ही उदीरणा सम्भव होती है।२५ ।। ५- उद्वर्तना- स्थिति तथा अनुभाग के बढ़ने को उद्वर्तना कहते हैं। यह क्रिया कर्मबन्ध के पश्चात् होती है। उदाहरणार्थ अशुभकर्म बाँधने के पश्चात् जीव की भावना यदि और अधिक कलुषित हो जाये तो बँधे हुये अशुभकर्मों की स्थिति बढ़ जाती है तथा फल देने की शक्ति भी तीव्र हो जाती है। इस प्रकार अध्यवसाय विशेष के कारण उस स्थिति के अनुभाग में वृद्धि हो जाना उद्वर्तना है। इस स्थिति को उत्कर्षण भी कहते हैं।२६ ६- अपवर्तना- अपवर्तना के द्वारा कर्मस्थिति का अल्पीकरण (स्थितिघात) और रस का मन्दीकरण (रस-घात) होता है।२७ यह अवस्था उद्वर्तना के ठीक विपरीत है। इसे अपकर्षण भी कहते हैं। ७- संक्रमण- जिस अध्यवसाय से जीव कर्म प्रकृति का बन्ध करता है, उसकी तीव्रता के कारण यह पूर्वबद्ध सजातीय प्रकृति के दलिकों को बध्यमान प्रकृति के दलिकों के साथ संक्रान्त कर देता है, परिणत या परिवर्तित कर देता है- वह