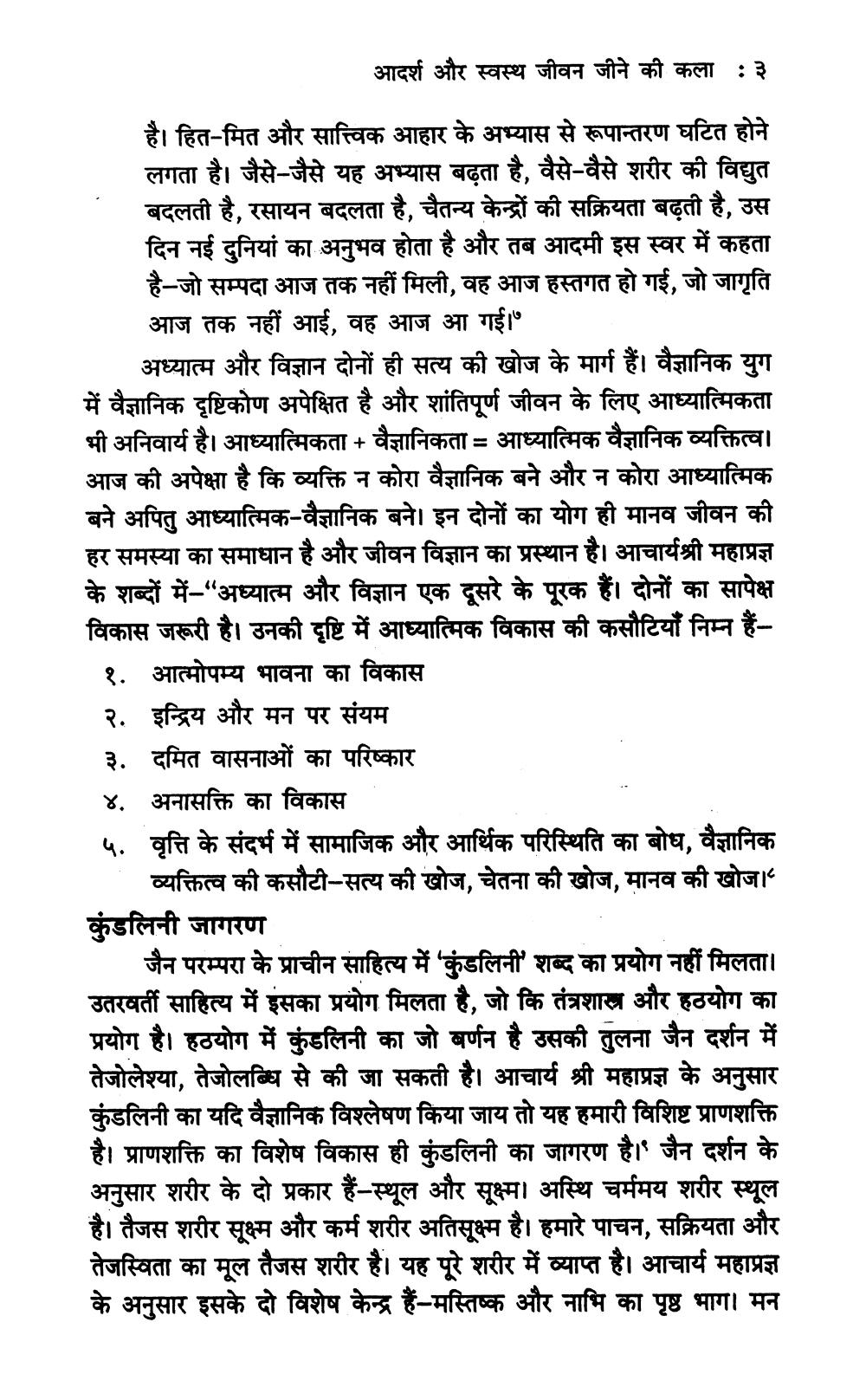________________
आदर्श और स्वस्थ जीवन जीने की कला : ३
है। हित-मित और सात्त्विक आहार के अभ्यास से रूपान्तरण घटित होने लगता है। जैसे-जैसे यह अभ्यास बढ़ता है, वैसे-वैसे शरीर की विद्युत बदलती है, रसायन बदलता है, चैतन्य केन्द्रों की सक्रियता बढ़ती है, उस दिन नई दुनियां का अनुभव होता है और तब आदमी इस स्वर में कहता है-जो सम्पदा आज तक नहीं मिली, वह आज हस्तगत हो गई, जो जागृति आज तक नहीं आई, वह आज आ गई।
अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही सत्य की खोज के मार्ग हैं। वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपेक्षित है और शांतिपूर्ण जीवन के लिए आध्यात्मिकता भी अनिवार्य है। आध्यात्मिकता + वैज्ञानिकता = आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व। आज की अपेक्षा है कि व्यक्ति न कोरा वैज्ञानिक बने और न कोरा आध्यात्मिक बने अपितु आध्यात्मिक-वैज्ञानिक बने। इन दोनों का योग ही मानव जीवन की हर समस्या का समाधान है और जीवन विज्ञान का प्रस्थान है। आचार्यश्री महाप्रज्ञ के शब्दों में-"अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का सापेक्ष विकास जरूरी है। उनकी दृष्टि में आध्यात्मिक विकास की कसौटियाँ निम्न हैं
१. आत्मोपम्य भावना का विकास २. इन्द्रिय और मन पर संयम ३. दमित वासनाओं का परिष्कार ४. अनासक्ति का विकास ५. वृत्ति के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति का बोध, वैज्ञानिक
व्यक्तित्व की कसौटी-सत्य की खोज, चेतना की खोज, मानव की खोजा' कुंडलिनी जागरण
जैन परम्परा के प्राचीन साहित्य में 'कुंडलिनी' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। उतरवर्ती साहित्य में इसका प्रयोग मिलता है, जो कि तंत्रशास्त्र और हठयोग का प्रयोग है। हठयोग में कुंडलिनी का जो वर्णन है उसकी तुलना जैन दर्शन में तेजोलेश्या, तेजोलब्धि से की जा सकती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के अनुसार कुंडलिनी का यदि वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाय तो यह हमारी विशिष्ट प्राणशक्ति है। प्राणशक्ति का विशेष विकास ही कुंडलिनी का जागरण है। जैन दर्शन के अनुसार शरीर के दो प्रकार हैं-स्थूल और सूक्ष्म। अस्थि चर्ममय शरीर स्थूल है। तैजस शरीर सूक्ष्म और कर्म शरीर अतिसूक्ष्म है। हमारे पाचन, सक्रियता और तेजस्विता का मूल तैजस शरीर है। यह पूरे शरीर में व्याप्त है। आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार इसके दो विशेष केन्द्र हैं-मस्तिष्क और नाभि का पृष्ठ भाग। मन