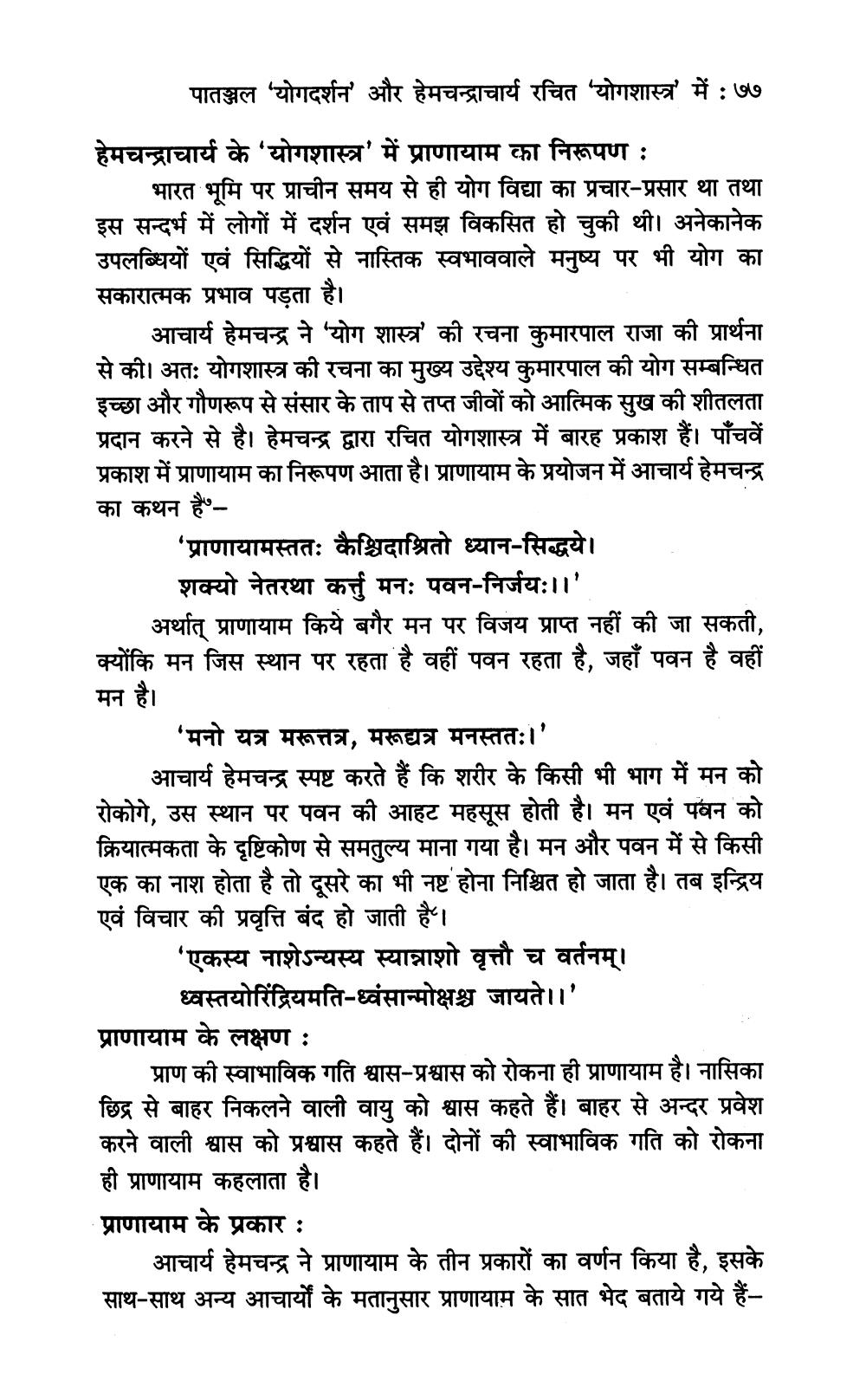________________
पातञ्जल 'योगदर्शन' और हेमचन्द्राचार्य रचित 'योगशास्त्र' में : ७७ हेमचन्द्राचार्य के 'योगशास्त्र' में प्राणायाम का निरूपण :
भारत भूमि पर प्राचीन समय से ही योग विद्या का प्रचार-प्रसार था तथा इस सन्दर्भ में लोगों में दर्शन एवं समझ विकसित हो चुकी थी। अनेकानेक उपलब्धियों एवं सिद्धियों से नास्तिक स्वभाववाले मनुष्य पर भी योग का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ____ आचार्य हेमचन्द्र ने 'योग शास्त्र' की रचना कुमारपाल राजा की प्रार्थना से की। अतः योगशास्त्र की रचना का मुख्य उद्देश्य कुमारपाल की योग सम्बन्धित इच्छा और गौणरूप से संसार के ताप से तप्त जीवों को आत्मिक सुख की शीतलता प्रदान करने से है। हेमचन्द्र द्वारा रचित योगशास्त्र में बारह प्रकाश हैं। पाँचवें प्रकाश में प्राणायाम का निरूपण आता है। प्राणायाम के प्रयोजन में आचार्य हेमचन्द्र का कथन है
'प्राणायामस्ततः कैश्चिदाश्रितो ध्यान-सिद्धये।
शक्यो नेतरथा कर्तुं मनः पवन-निर्जयः।।' अर्थात् प्राणायाम किये बगैर मन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि मन जिस स्थान पर रहता है वहीं पवन रहता है, जहाँ पवन है वहीं मन है।
'मनो यत्र मरूत्तत्र, मरूद्यत्र मनस्ततः।'
आचार्य हेमचन्द्र स्पष्ट करते हैं कि शरीर के किसी भी भाग में मन को रोकोगे, उस स्थान पर पवन की आहट महसूस होती है। मन एवं पवन को क्रियात्मकता के दृष्टिकोण से समतुल्य माना गया है। मन और पवन में से किसी एक का नाश होता है तो दूसरे का भी नष्ट होना निश्चित हो जाता है। तब इन्द्रिय एवं विचार की प्रवृत्ति बंद हो जाती है।
'एकस्य नाशेऽन्यस्य स्यान्नाशो वृत्तौ च वर्तनम्।
ध्वस्तयोरिंद्रियमति-ध्वंसान्मोक्षश्च जायते।।' प्राणायाम के लक्षण :
प्राण की स्वाभाविक गति श्वास-प्रश्वास को रोकना ही प्राणायाम है। नासिका छिद्र से बाहर निकलने वाली वायु को श्वास कहते हैं। बाहर से अन्दर प्रवेश करने वाली श्वास को प्रश्वास कहते हैं। दोनों की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के प्रकार :
आचार्य हेमचन्द्र ने प्राणायाम के तीन प्रकारों का वर्णन किया है, इसके साथ-साथ अन्य आचार्यों के मतानुसार प्राणायाम के सात भेद बताये गये हैं