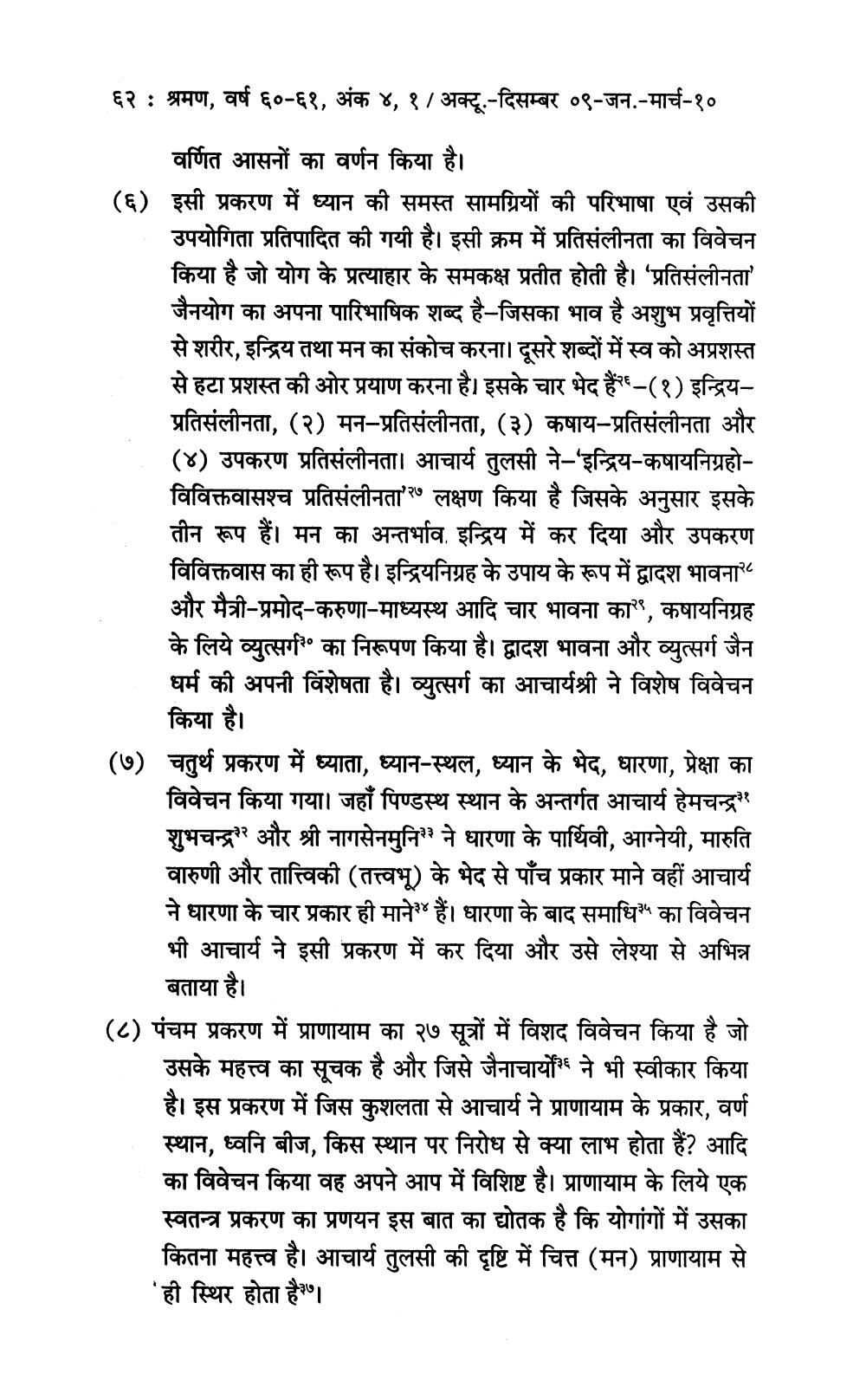________________
६२ : श्रमण, वर्ष ६०-६१, अंक ४, १ / अक्टू.-दिसम्बर ०९-जन.-मार्च-१०
वर्णित आसनों का वर्णन किया है। (६) इसी प्रकरण में ध्यान की समस्त सामग्रियों की परिभाषा एवं उसकी
उपयोगिता प्रतिपादित की गयी है। इसी क्रम में प्रतिसंलीनता का विवेचन किया है जो योग के प्रत्याहार के समकक्ष प्रतीत होती है। 'प्रतिसंलीनता' जैनयोग का अपना पारिभाषिक शब्द है-जिसका भाव है अशुभ प्रवृत्तियों से शरीर, इन्द्रिय तथा मन का संकोच करना। दूसरे शब्दों में स्व को अप्रशस्त से हटा प्रशस्त की ओर प्रयाण करना है। इसके चार भेद हैं२६-(१) इन्द्रियप्रतिसंलीनता, (२) मन-प्रतिसंलीनता, (३) कषाय-प्रतिसंलीनता और (४) उपकरण प्रतिसंलीनता। आचार्य तुलसी ने-'इन्द्रिय-कषायनिग्रहोविविक्तवासश्च प्रतिसंलीनता'२७ लक्षण किया है जिसके अनुसार इसके तीन रूप हैं। मन का अन्तर्भाव. इन्द्रिय में कर दिया और उपकरण विविक्तवास का ही रूप है। इन्द्रियनिग्रह के उपाय के रूप में द्वादश भावना२८
और मैत्री-प्रमोद-करुणा-माध्यस्थ आदि चार भावना का२९, कषायनिग्रह के लिये व्युत्सर्गर का निरूपण किया है। द्वादश भावना और व्युत्सर्ग जैन धर्म की अपनी विशेषता है। व्युत्सर्ग का आचार्यश्री ने विशेष विवेचन किया है। चतुर्थ प्रकरण में ध्याता, ध्यान-स्थल, ध्यान के भेद, धारणा, प्रेक्षा का विवेचन किया गया। जहाँ पिण्डस्थ स्थान के अन्तर्गत आचार्य हेमचन्द्र शुभचन्द्र और श्री नागसेनमुनि ने धारणा के पार्थिवी, आग्नेयी, मारुति वारुणी और तात्त्विकी (तत्त्वभू) के भेद से पाँच प्रकार माने वहीं आचार्य ने धारणा के चार प्रकार ही माने हैं। धारणा के बाद समाधि का विवेचन भी आचार्य ने इसी प्रकरण में कर दिया और उसे लेश्या से अभिन्न
बताया है। (८) पंचम प्रकरण में प्राणायाम का २७ सूत्रों में विशद विवेचन किया है जो
उसके महत्त्व का सूचक है और जिसे जैनाचार्यों ने भी स्वीकार किया है। इस प्रकरण में जिस कुशलता से आचार्य ने प्राणायाम के प्रकार, वर्ण स्थान, ध्वनि बीज, किस स्थान पर निरोध से क्या लाभ होता हैं? आदि का विवेचन किया वह अपने आप में विशिष्ट है। प्राणायाम के लिये एक स्वतन्त्र प्रकरण का प्रणयन इस बात का द्योतक है कि योगांगों में उसका कितना महत्त्व है। आचार्य तुलसी की दृष्टि में चित्त (मन) प्राणायाम से 'ही स्थिर होता है।