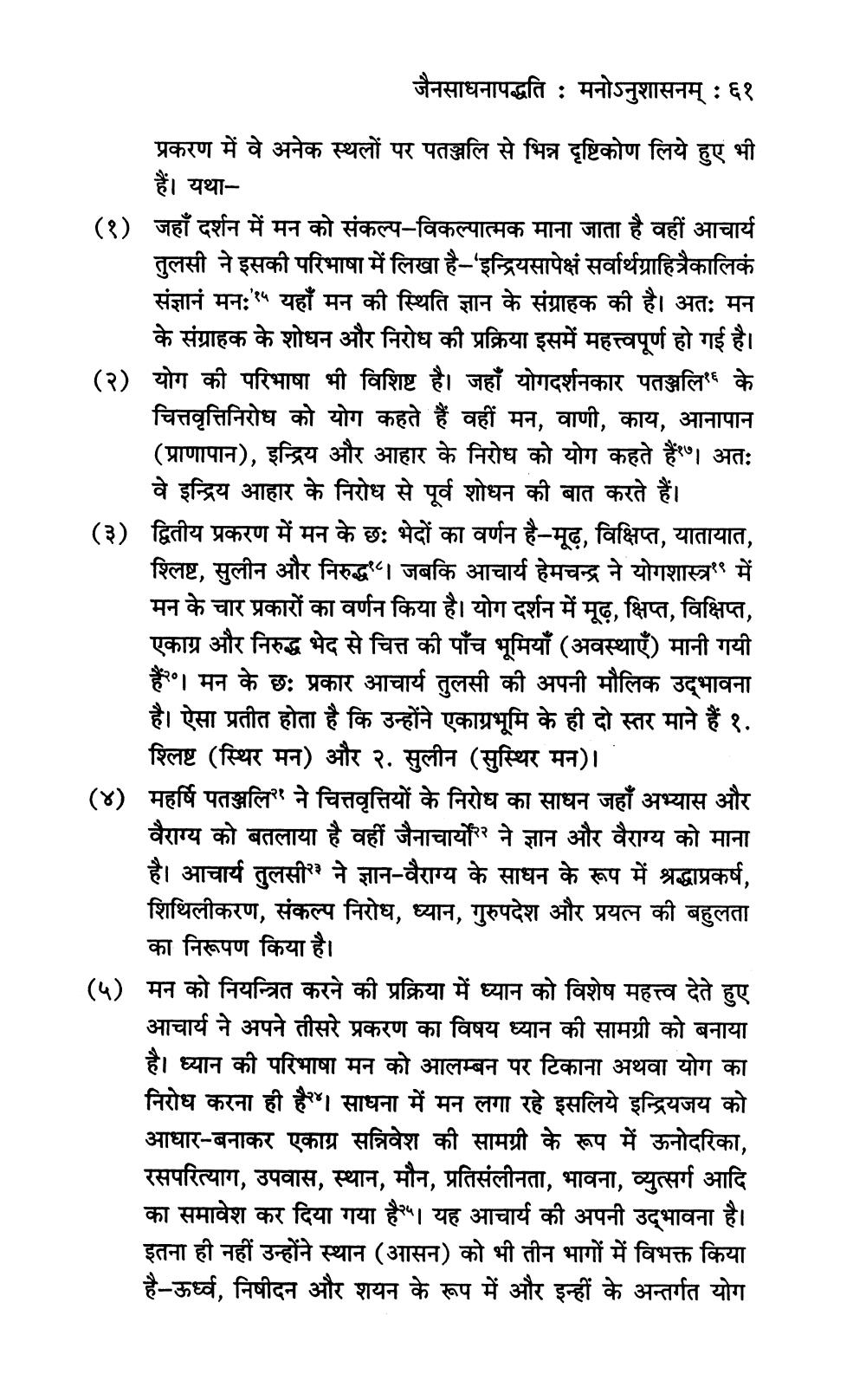________________
जैनसाधनापद्धति : मनोऽनुशासनम् : ६१
(२)
प्रकरण में वे अनेक स्थलों पर पतञ्जलि से भिन्न दृष्टिकोण लिये हुए भी
हैं। यथा(१) जहाँ दर्शन में मन को संकल्प-विकल्पात्मक माना जाता है वहीं आचार्य
तुलसी ने इसकी परिभाषा में लिखा है-'इन्द्रियसापेक्षं सर्वार्थग्राहित्रैकालिकं संज्ञानं मनः५ यहाँ मन की स्थिति ज्ञान के संग्राहक की है। अतः मन के संग्राहक के शोधन और निरोध की प्रक्रिया इसमें महत्त्वपूर्ण हो गई है। योग की परिभाषा भी विशिष्ट है। जहाँ योगदर्शनकार पतञ्जलि'६ के चित्तवृत्तिनिरोध को योग कहते हैं वहीं मन, वाणी, काय, आनापान (प्राणापान), इन्द्रिय और आहार के निरोध को योग कहते हैं। अतः
वे इन्द्रिय आहार के निरोध से पूर्व शोधन की बात करते हैं। (३) द्वितीय प्रकरण में मन के छः भेदों का वर्णन है-मूढ, विक्षिप्त, यातायात,
श्लिष्ट, सुलीन और निरुद्ध। जबकि आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में मन के चार प्रकारों का वर्णन किया है। योग दर्शन में मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध भेद से चित्त की पाँच भूमियाँ (अवस्थाएँ) मानी गयी हैं। मन के छः प्रकार आचार्य तुलसी की अपनी मौलिक उद्भावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एकाग्रभूमि के ही दो स्तर माने हैं १.
श्लिष्ट (स्थिर मन) और २. सुलीन (सुस्थिर मन)। (४) महर्षि पतञ्जलि ने चित्तवृत्तियों के निरोध का साधन जहाँ अभ्यास और
वैराग्य को बतलाया है वहीं जैनाचार्यों ने ज्ञान और वैराग्य को माना है। आचार्य तुलसी ने ज्ञान-वैराग्य के साधन के रूप में श्रद्धाप्रकर्ष, शिथिलीकरण, संकल्प निरोध, ध्यान, गुरुपदेश और प्रयत्न की बहुलता
का निरूपण किया है। (५) मन को नियन्त्रित करने की प्रक्रिया में ध्यान को विशेष महत्त्व देते हुए
आचार्य ने अपने तीसरे प्रकरण का विषय ध्यान की सामग्री को बनाया है। ध्यान की परिभाषा मन को आलम्बन पर टिकाना अथवा योग का निरोध करना ही है। साधना में मन लगा रहे इसलिये इन्द्रियजय को
आधार-बनाकर एकाग्र सन्निवेश की सामग्री के रूप में ऊनोदरिका, रसपरित्याग, उपवास, स्थान, मौन, प्रतिसंलीनता, भावना, व्युत्सर्ग आदि
का समावेश कर दिया गया है। यह आचार्य की अपनी उद्भावना है। इतना ही नहीं उन्होंने स्थान (आसन) को भी तीन भागों में विभक्त किया है-ऊर्ध्व, निषीदन और शयन के रूप में और इन्हीं के अन्तर्गत योग