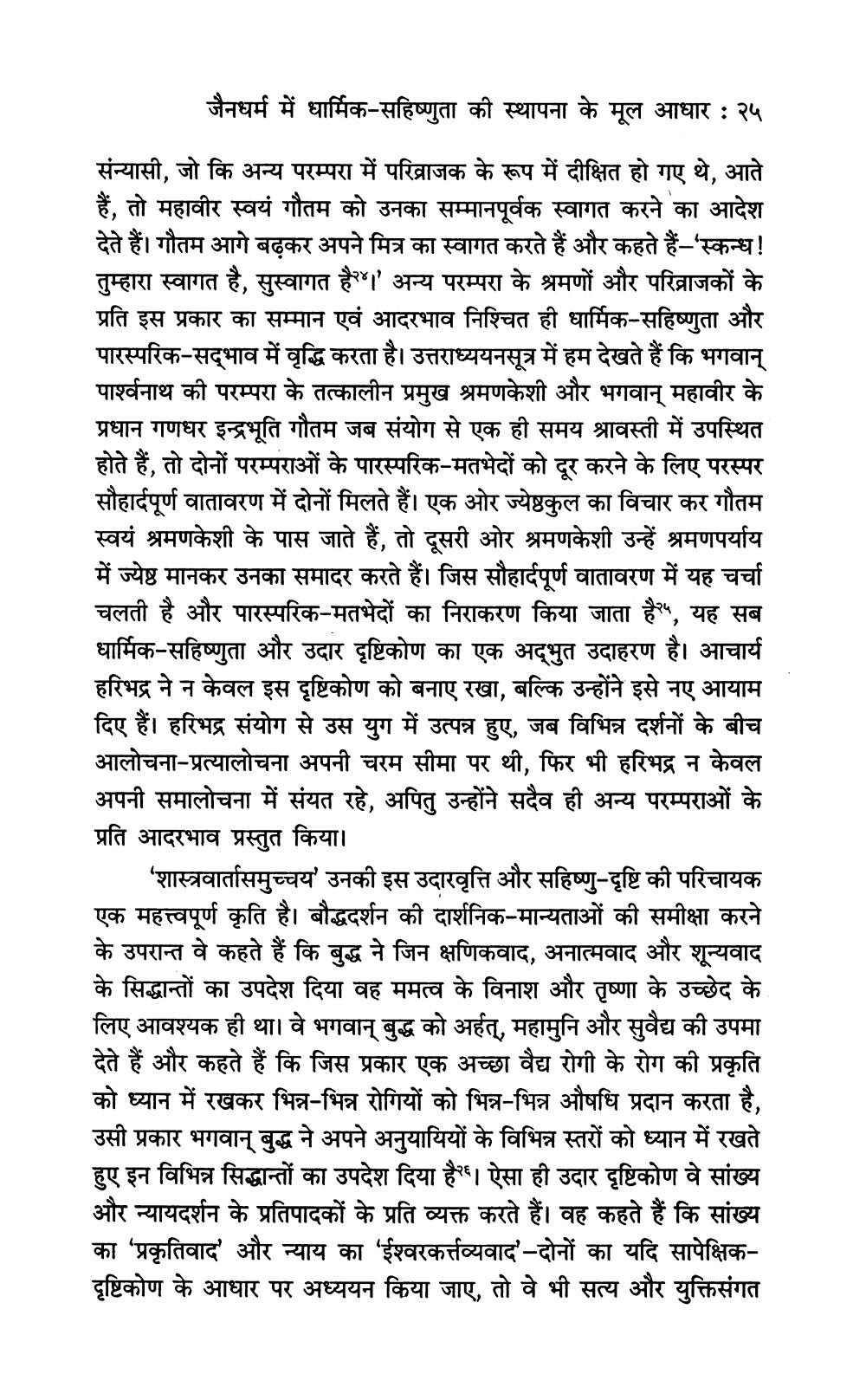________________
जैनधर्म में धार्मिक-सहिष्णुता की स्थापना के मूल आधार : २५
संन्यासी, जो कि अन्य परम्परा में परिव्राजक के रूप में दीक्षित हो गए थे, आते हैं, तो महावीर स्वयं गौतम को उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करने का आदेश देते हैं। गौतम आगे बढ़कर अपने मित्र का स्वागत करते हैं और कहते हैं-'स्कन्ध! तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागत है।' अन्य परम्परा के श्रमणों और परिव्राजकों के प्रति इस प्रकार का सम्मान एवं आदरभाव निश्चित ही धार्मिक-सहिष्णुता और पारस्परिक-सद्भाव में वृद्धि करता है। उत्तराध्ययनसूत्र में हम देखते हैं कि भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के तत्कालीन प्रमुख श्रमणकेशी और भगवान् महावीर के प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतम जब संयोग से एक ही समय श्रावस्ती में उपस्थित होते हैं, तो दोनों परम्पराओं के पारस्परिक-मतभेदों को दूर करने के लिए परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों मिलते हैं। एक ओर ज्येष्ठकुल का विचार कर गौतम स्वयं श्रमणकेशी के पास जाते हैं, तो दूसरी ओर श्रमणकेशी उन्हें श्रमणपर्याय में ज्येष्ठ मानकर उनका समादर करते हैं। जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह चर्चा चलती है और पारस्परिक-मतभेदों का निराकरण किया जाता है, यह सब धार्मिक-सहिष्णुता और उदार दृष्टिकोण का एक अद्भुत उदाहरण है। आचार्य हरिभद्र ने न केवल इस दृष्टिकोण को बनाए रखा, बल्कि उन्होंने इसे नए आयाम दिए हैं। हरिभद्र संयोग से उस युग में उत्पन्न हुए, जब विभिन्न दर्शनों के बीच आलोचना-प्रत्यालोचना अपनी चरम सीमा पर थी, फिर भी हरिभद्र न केवल अपनी समालोचना में संयत रहे, अपितु उन्होंने सदैव ही अन्य परम्पराओं के प्रति आदरभाव प्रस्तुत किया। ___ 'शास्त्रवार्तासमुच्चय' उनकी इस उदारवृत्ति और सहिष्णु-दृष्टि की परिचायक एक महत्त्वपूर्ण कृति है। बौद्धदर्शन की दार्शनिक-मान्यताओं की समीक्षा करने के उपरान्त वे कहते हैं कि बुद्ध ने जिन क्षणिकवाद, अनात्मवाद और शून्यवाद के सिद्धान्तों का उपदेश दिया वह ममत्व के विनाश और तृष्णा के उच्छेद के लिए आवश्यक ही था। वे भगवान बुद्ध को अर्हत्, महामुनि और सुवैद्य की उपमा देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार एक अच्छा वैद्य रोगी के रोग की प्रकृति को ध्यान में रखकर भिन्न-भिन्न रोगियों को भिन्न-भिन्न औषधि प्रदान करता है, उसी प्रकार भगवान् बुद्ध ने अपने अनुयायियों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए इन विभिन्न सिद्धान्तों का उपदेश दिया है। ऐसा ही उदार दृष्टिकोण वे सांख्य
और न्यायदर्शन के प्रतिपादकों के प्रति व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि सांख्य का 'प्रकृतिवाद' और न्याय का 'ईश्वरकर्त्तव्यवाद'-दोनों का यदि सापेक्षिकदृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया जाए, तो वे भी सत्य और युक्तिसंगत