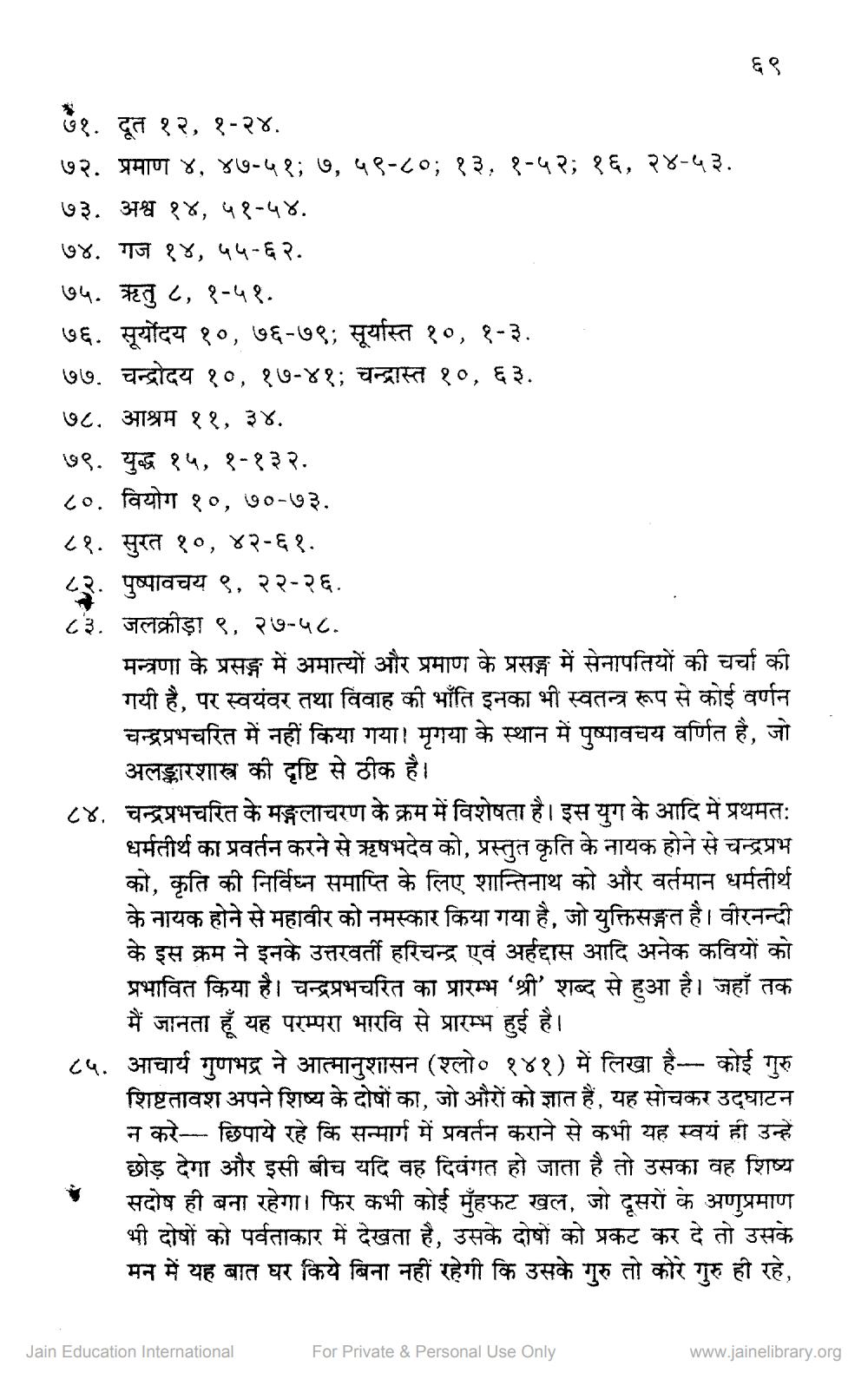________________
६९
७१. दूत १२, १-२४. ७२. प्रमाण ४, ४७-५१; ७, ५९-८०; १३. १-५२; १६, २४-५३. ७३. अश्व १४, ५१-५४. ७४. गज १४, ५५-६२. ७५. ऋतु ८, १-५१. ७६. सूर्योदय १०, ७६-७९; सूर्यास्त १०, १-३. ७७. चन्द्रोदय १०, १७-४१; चन्द्रास्त १०, ६३. ७८. आश्रम ११, ३४. ७९. युद्ध १५, १-१३२. ८०. वियोग १०, ७०-७३. ८१. सुरत १०, ४२-६१. ८२. पुष्पावचय ९, २२-२६. ८३. जलक्रीड़ा ९, २७-५८.
मन्त्रणा के प्रसङ्ग में अमात्यों और प्रमाण के प्रसङ्ग में सेनापतियों की चर्चा की गयी है, पर स्वयंवर तथा विवाह की भाँति इनका भी स्वतन्त्र रूप से कोई वर्णन चन्द्रप्रभचरित में नहीं किया गया। मृगया के स्थान में पुष्पावचय वर्णित है, जो अलङ्कारशास्त्र की दृष्टि से ठीक है। चन्द्रप्रभचरित के मङ्गलाचरण के क्रम में विशेषता है। इस युग के आदि में प्रथमत: धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करने से ऋषभदेव को, प्रस्तुत कृति के नायक होने से चन्द्रप्रभ को, कृति की निर्विघ्न समाप्ति के लिए शान्तिनाथ को और वर्तमान धर्मतीर्थ के नायक होने से महावीर को नमस्कार किया गया है, जो युक्तिसङ्गत है। वीरनन्दी के इस क्रम ने इनके उत्तरवर्ती हरिचन्द्र एवं अर्हद्दास आदि अनेक कवियों को प्रभावित किया है। चन्द्रप्रभचरित का प्रारम्भ 'श्री' शब्द से हुआ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ यह परम्परा भारवि से प्रारम्भ हुई है। आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन (श्लो० १४१) में लिखा है--- कोई गुरु शिष्टतावश अपने शिष्य के दोषों का, जो औरों को ज्ञात हैं, यह सोचकर उद्घाटन न करे-- छिपाये रहे कि सन्मार्ग में प्रवर्तन कराने से कभी यह स्वयं ही उन्हें छोड़ देगा और इसी बीच यदि वह दिवंगत हो जाता है तो उसका वह शिष्य सदोष ही बना रहेगा। फिर कभी कोई मुँहफट खल, जो दूसरों के अणुप्रमाण भी दोषों को पर्वताकार में देखता है, उसके दोषों को प्रकट कर दे तो उसके मन में यह बात घर किये बिना नहीं रहेगी कि उसके गुरु तो कोरे गुरु ही रहे,
८४.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org