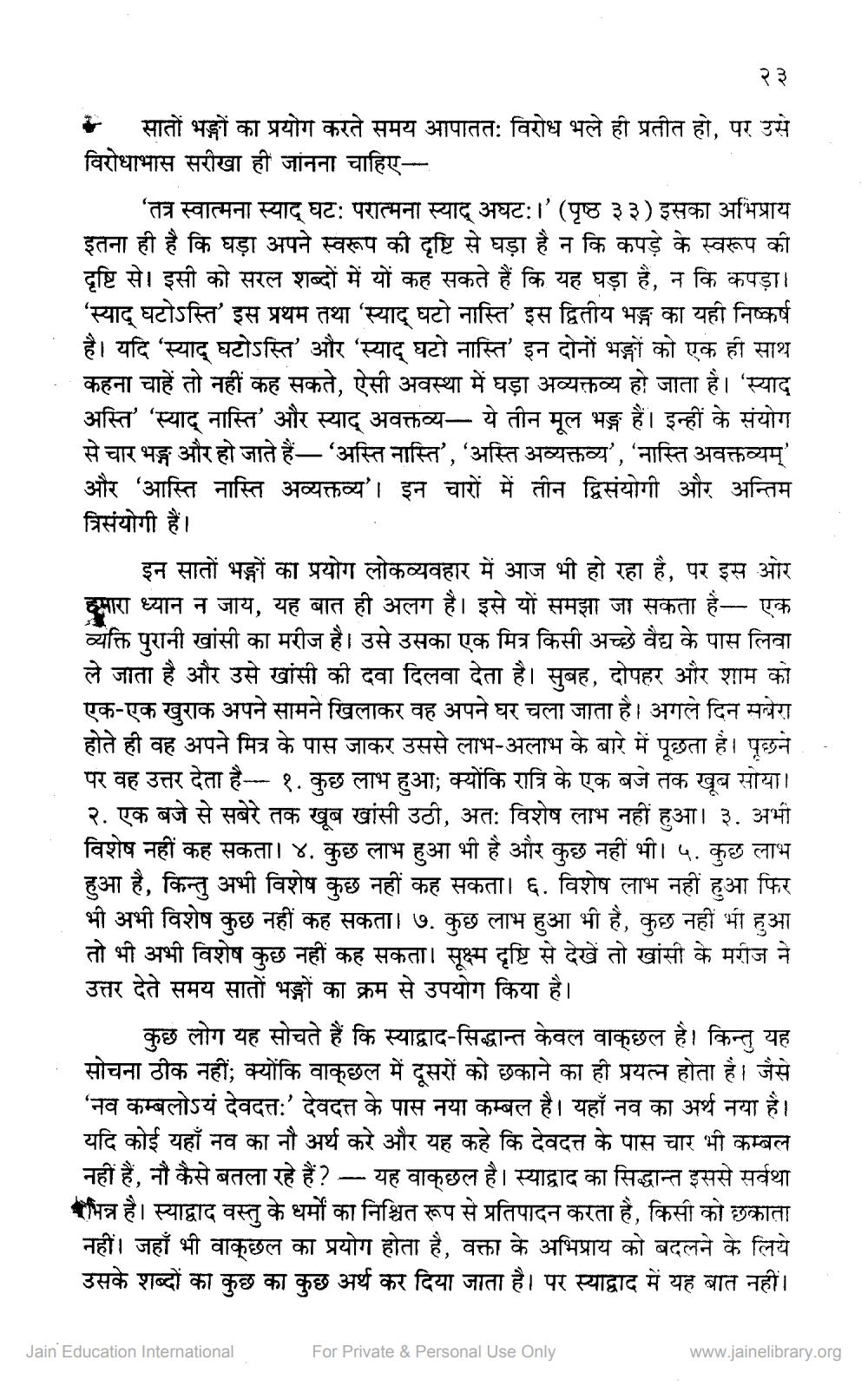________________
* सातों भङ्गों का प्रयोग करते समय आपाततः विरोध भले ही प्रतीत हो, पर उसे विरोधाभास सरीखा ही जानना चाहिए
___ 'तत्र स्वात्मना स्याद् घट: परात्मना स्याद् अघटः।' (पृष्ठ ३३) इसका अभिप्राय इतना ही है कि घड़ा अपने स्वरूप की दृष्टि से घड़ा है न कि कपड़े के स्वरूप की दृष्टि से। इसी को सरल शब्दों में यों कह सकते हैं कि यह घड़ा है, न कि कपड़ा। 'स्याद् घटोऽस्ति' इस प्रथम तथा 'स्याद् घटो नास्ति' इस द्वितीय भङ्ग का यही निष्कर्ष है। यदि 'स्याद् घटोऽस्ति' और 'स्याद् घटो नास्ति' इन दोनों भङ्गों को एक ही साथ कहना चाहें तो नहीं कह सकते, ऐसी अवस्था में घड़ा अव्यक्तव्य हो जाता है। 'स्याद अस्ति' 'स्याद् नास्ति' और स्याद् अवक्तव्य- ये तीन मूल भङ्ग हैं। इन्हीं के संयोग से चार भङ्ग और हो जाते हैं- 'अस्ति नास्ति', 'अस्ति अव्यक्तव्य', 'नास्ति अवक्तव्यम्'
और 'आस्ति नास्ति अव्यक्तव्य'। इन चारों में तीन द्विसंयोगी और अन्तिम त्रिसंयोगी हैं।
इन सातों भङ्गों का प्रयोग लोकव्यवहार में आज भी हो रहा है, पर इस ओर हमारा ध्यान न जाय, यह बात ही अलग है। इसे यों समझा जा सकता है- एक व्यक्ति पुरानी खांसी का मरीज है। उसे उसका एक मित्र किसी अच्छे वैद्य के पास लिवा ले जाता है और उसे खांसी की दवा दिलवा देता है। सुबह, दोपहर और शाम को एक-एक खुराक अपने सामने खिलाकर वह अपने घर चला जाता है। अगले दिन सबेरा होते ही वह अपने मित्र के पास जाकर उससे लाभ-अलाभ के बारे में पूछता है। पूछने पर वह उत्तर देता है--- १. कुछ लाभ हुआ; क्योंकि रात्रि के एक बजे तक खूब सोया। २. एक बजे से सबेरे तक खूब खांसी उठी, अत: विशेष लाभ नहीं हुआ। ३. अभी विशेष नहीं कह सकता। ४. कुछ लाभ हुआ भी है और कुछ नहीं भी। ५. कुछ लाभ हुआ है, किन्तु अभी विशेष कुछ नहीं कह सकता। ६. विशेष लाभ नहीं हुआ फिर भी अभी विशेष कुछ नहीं कह सकता। ७. कुछ लाभ हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ तो भी अभी विशेष कुछ नहीं कह सकता। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो खांसी के मरीज ने उत्तर देते समय सातो भङ्गो का क्रम से उपयोग किया है।
कुछ लोग यह सोचते हैं कि स्याद्वाद-सिद्धान्त केवल वाक्छल है। किन्तु यह सोचना ठीक नहीं; क्योंकि वाक्छल में दूसरों को छकाने का ही प्रयत्न होता है। जैसे 'नव कम्बलोऽयं देवदत्त:' देवदत्त के पास नया कम्बल है। यहाँ नव का अर्थ नया है। यदि कोई यहाँ नव का नौ अर्थ करे और यह कहे कि देवदत्त के पास चार भी कम्बल नहीं हैं, नौ कैसे बतला रहे हैं? --- यह वाक्छल है। स्याद्वाद का सिद्धान्त इससे सर्वथा भिन्न है। स्याद्वाद वस्तु के धर्मों का निश्चित रूप से प्रतिपादन करता है, किसी को छकाता नहीं। जहाँ भी वाक्छल का प्रयोग होता है, वक्ता के अभिप्राय को बदलने के लिये उसके शब्दों का कुछ का कुछ अर्थ कर दिया जाता है। पर स्याद्वाद में यह बात नहीं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org