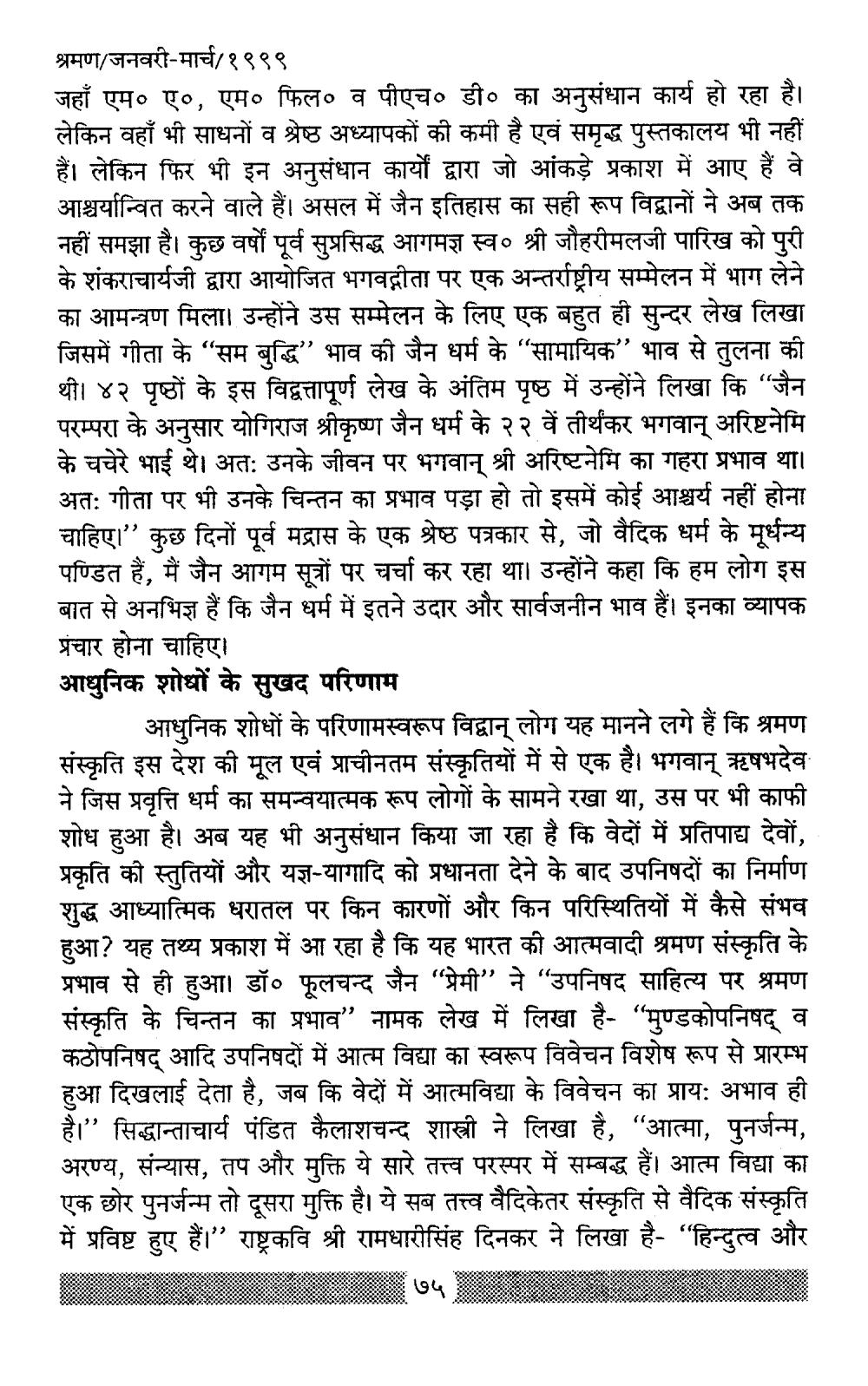________________
श्रमण/जनवरी-मार्च/१९९९ जहाँ एम० ए०, एम० फिल० व पीएच० डी० का अनुसंधान कार्य हो रहा है। लेकिन वहाँ भी साधनों व श्रेष्ठ अध्यापकों की कमी है एवं समृद्ध पुस्तकालय भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी इन अनुसंधान कार्यों द्वारा जो आंकड़े प्रकाश में आए हैं वे आश्चर्यान्वित करने वाले हैं। असल में जैन इतिहास का सही रूप विद्वानों ने अब तक नहीं समझा है। कुछ वर्षों पूर्व सुप्रसिद्ध आगमज्ञ स्व० श्री जौहरीमलजी पारिख को पुरी के शंकराचार्यजी द्वारा आयोजित भगवद्गीता पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का आमन्त्रण मिला। उन्होंने उस सम्मेलन के लिए एक बहुत ही सुन्दर लेख लिखा जिसमें गीता के “सम बुद्धि" भाव की जैन धर्म के “सामायिक" भाव से तुलना की थी। ४२ पृष्ठों के इस विद्वत्तापूर्ण लेख के अंतिम पृष्ठ में उन्होंने लिखा कि “जैन परम्परा के अनुसार योगिराज श्रीकृष्ण जैन धर्म के २२ वें तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि के चचेरे भाई थे। अत: उनके जीवन पर भगवान् श्री अरिष्टनेमि का गहरा प्रभाव था। अत: गीता पर भी उनके चिन्तन का प्रभाव पड़ा हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।" कुछ दिनों पूर्व मद्रास के एक श्रेष्ठ पत्रकार से, जो वैदिक धर्म के मूर्धन्य पण्डित हैं, मैं जैन आगम सूत्रों पर चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जैन धर्म में इतने उदार और सार्वजनीन भाव हैं। इनका व्यापक प्रचार होना चाहिए। आधुनिक शोधों के सुखद परिणाम
आधुनिक शोधों के परिणामस्वरूप विद्वान् लोग यह मानने लगे हैं कि श्रमण संस्कृति इस देश की मूल एवं प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भगवान् ऋषभदेव ने जिस प्रवृत्ति धर्म का समन्वयात्मक रूप लोगों के सामने रखा था, उस पर भी काफी शोध हुआ है। अब यह भी अनुसंधान किया जा रहा है कि वेदों में प्रतिपाद्य देवों, प्रकृति की स्तुतियों और यज्ञ-यागादि को प्रधानता देने के बाद उपनिषदों का निर्माण शुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर किन कारणों और किन परिस्थितियों में कैसे संभव हुआ? यह तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि यह भारत की आत्मवादी श्रमण संस्कृति के प्रभाव से ही हआ। डॉ० फूलचन्द जैन "प्रेमी" ने “उपनिषद साहित्य पर श्रमण संस्कृति के चिन्तन का प्रभाव" नामक लेख में लिखा है- “मुण्डकोपनिषद् व कठोपनिषद् आदि उपनिषदों में आत्म विद्या का स्वरूप विवेचन विशेष रूप से प्रारम्भ हुआ दिखलाई देता है, जब कि वेदों में आत्मविद्या के विवेचन का प्राय: अभाव ही है।" सिद्धान्ताचार्य पंडित कैलाशचन्द शास्त्री ने लिखा है, "आत्मा, पुनर्जन्म, अरण्य, संन्यास, तप और मुक्ति ये सारे तत्त्व परस्पर में सम्बद्ध हैं। आत्म विद्या का एक छोर पुनर्जन्म तो दूसरा मुक्ति है। ये सब तत्त्व वैदिकेतर संस्कृति से वैदिक संस्कृति में प्रविष्ट हुए हैं।" राष्ट्रकवि श्री रामधारीसिंह दिनकर ने लिखा है- “हिन्दुत्व और