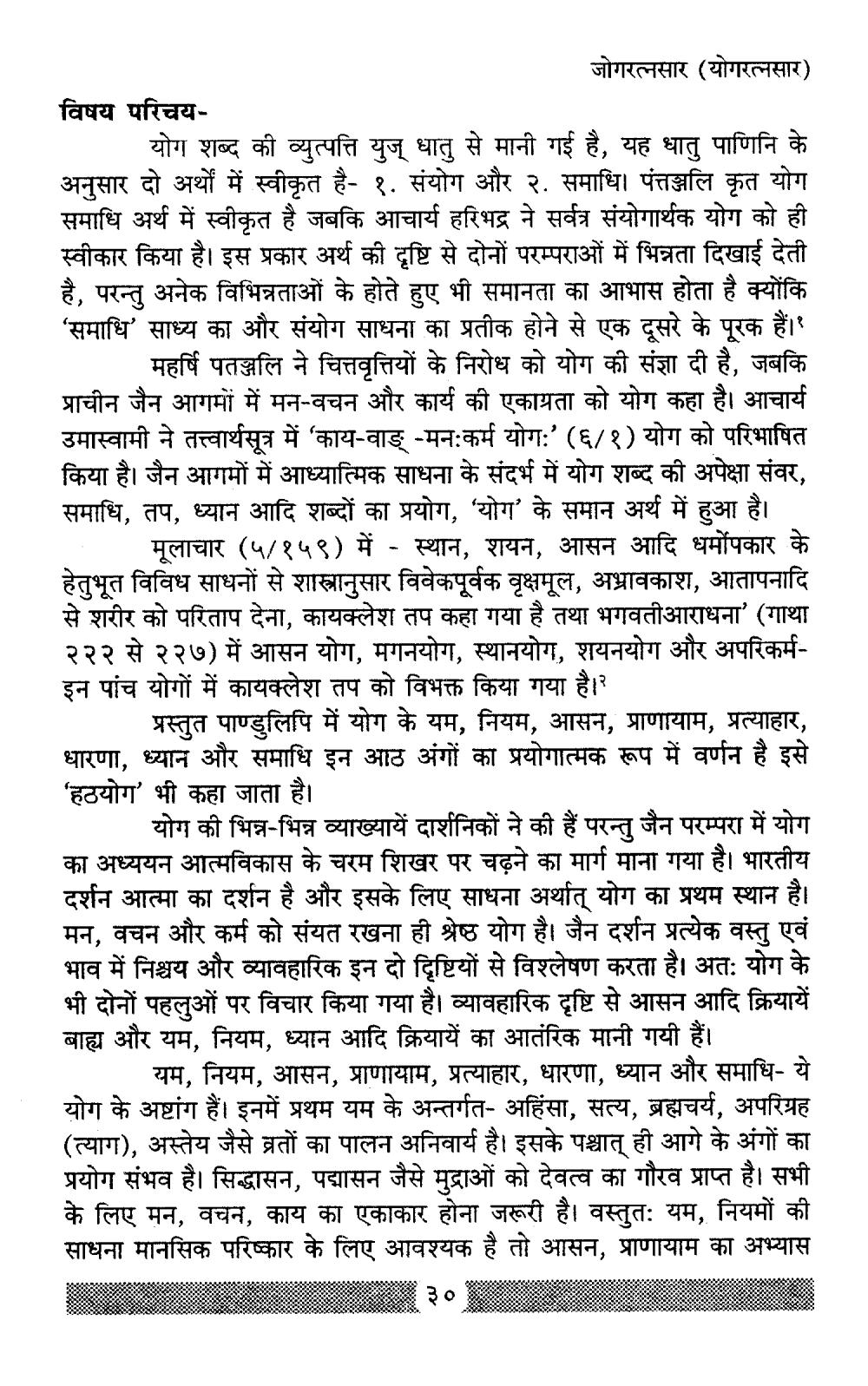________________
जोगरत्नसार (योगरत्नसार) विषय परिचय
योग शब्द की व्युत्पत्ति युज् धातु से मानी गई है, यह धातु पाणिनि के अनुसार दो अर्थों में स्वीकृत है- १. संयोग और २. समाधि। पंतञ्जलि कृत योग समाधि अर्थ में स्वीकृत है जबकि आचार्य हरिभद्र ने सर्वत्र संयोगार्थक योग को ही स्वीकार किया है। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से दोनों परम्पराओं में भिन्नता दिखाई देती है, परन्तु अनेक विभिन्नताओं के होते हुए भी समानता का आभास होता है क्योंकि 'समाधि' साध्य का और संयोग साधना का प्रतीक होने से एक दूसरे के पूरक हैं।'
महर्षि पतञ्जलि ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग की संज्ञा दी है, जबकि प्राचीन जैन आगमों में मन-वचन और कार्य की एकाग्रता को योग कहा है। आचार्य उमास्वामी ने तत्त्वार्थसूत्र में 'काय-वाङ् -मन:कर्म योगः' (६/१) योग को परिभाषित किया है। जैन आगमों में आध्यात्मिक साधना के संदर्भ में योग शब्द की अपेक्षा संवर, समाधि, तप, ध्यान आदि शब्दों का प्रयोग, 'योग' के समान अर्थ में हआ है।
मूलाचार (५/१५९) में - स्थान, शयन, आसन आदि धर्मोपकार के हेतुभूत विविध साधनों से शास्त्रानुसार विवेकपूर्वक वृक्षमूल, अभ्रावकाश, आतापनादि से शरीर को परिताप देना, कायक्लेश तप कहा गया है तथा भगवतीआराधना' (गाथा २२२ से २२७) में आसन योग, मगनयोग, स्थानयोग, शयनयोग और अपरिकर्मइन पांच योगों में कायक्लेश तप को विभक्त किया गया है।
प्रस्तुत पाण्डुलिपि में योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन आठ अंगों का प्रयोगात्मक रूप में वर्णन है इसे 'हठयोग' भी कहा जाता है।
योग की भिन्न-भिन्न व्याख्यायें दार्शनिकों ने की हैं परन्तु जैन परम्परा में योग का अध्ययन आत्मविकास के चरम शिखर पर चढ़ने का मार्ग माना गया है। भारतीय दर्शन आत्मा का दर्शन है और इसके लिए साधना अर्थात् योग का प्रथम स्थान है। मन, वचन और कर्म को संयत रखना ही श्रेष्ठ योग है। जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु एवं भाव में निश्चय और व्यावहारिक इन दो दृिष्टियों से विश्लेषण करता है। अत: योग के भी दोनों पहलुओं पर विचार किया गया है। व्यावहारिक दृष्टि से आसन आदि क्रियायें बाह्य और यम, नियम, ध्यान आदि क्रियायें का आतंरिक मानी गयी हैं।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि- ये योग के अष्टांग हैं। इनमें प्रथम यम के अन्तर्गत- अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह (त्याग), अस्तेय जैसे व्रतों का पालन अनिवार्य है। इसके पश्चात् ही आगे के अंगों का प्रयोग संभव है। सिद्धासन, पद्मासन जैसे मुद्राओं को देवत्व का गौरव प्राप्त है। सभी के लिए मन, वचन, काय का एकाकार होना जरूरी है। वस्तुत: यम, नियमों की साधना मानसिक परिष्कार के लिए आवश्यक है तो आसन, प्राणायाम का अभ्यास