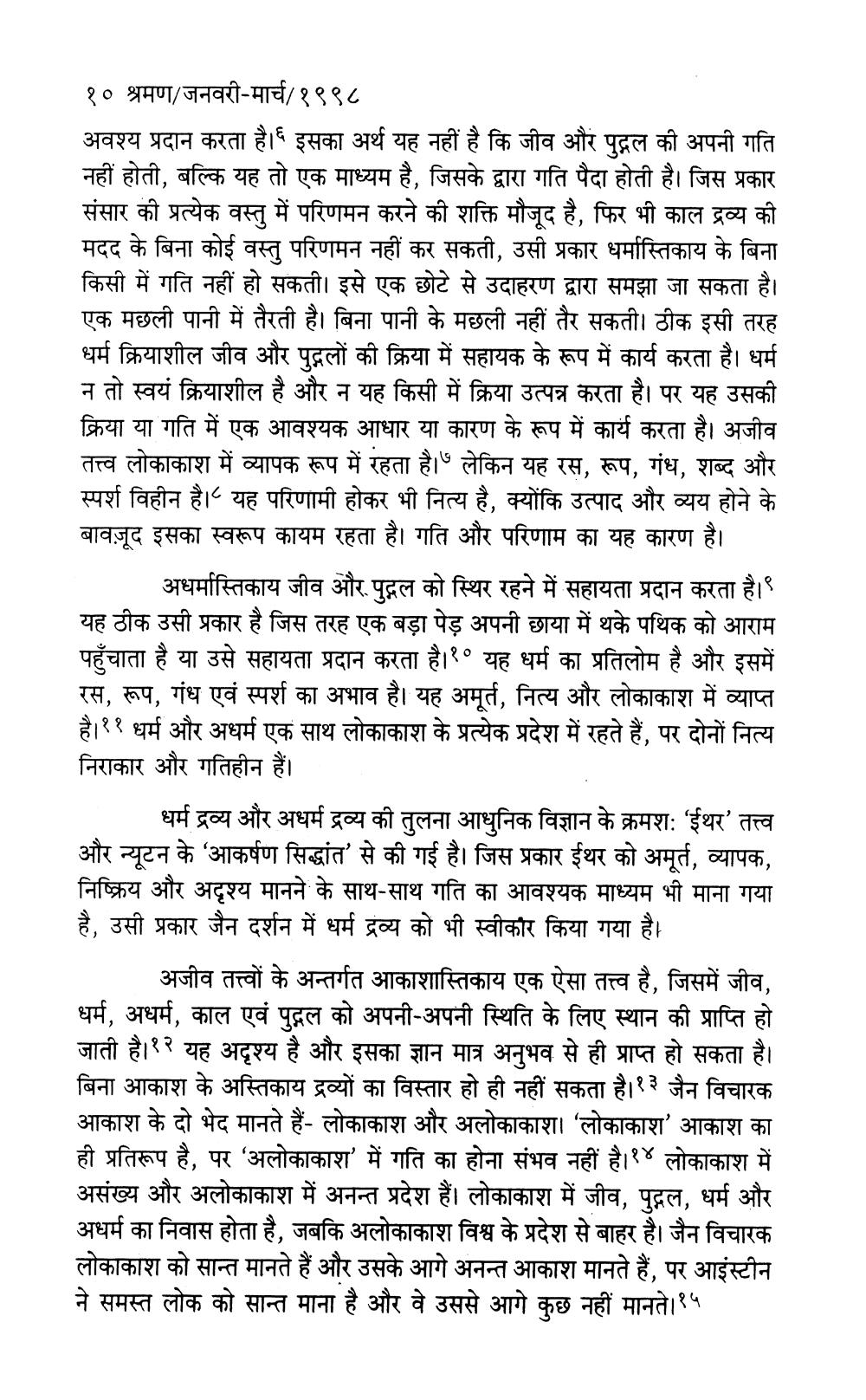________________
१० श्रमण/जनवरी-मार्च/१९९८ अवश्य प्रदान करता है।६ इसका अर्थ यह नहीं है कि जीव और पद्गल की अपनी गति नहीं होती, बल्कि यह तो एक माध्यम है, जिसके द्वारा गति पैदा होती है। जिस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु में परिणमन करने की शक्ति मौजूद है, फिर भी काल द्रव्य की मदद के बिना कोई वस्तु परिणमन नहीं कर सकती, उसी प्रकार धर्मास्तिकाय के बिना किसी में गति नहीं हो सकती। इसे एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। एक मछली पानी में तैरती है। बिना पानी के मछली नहीं तैर सकती। ठीक इसी तरह धर्म क्रियाशील जीव और पुद्गलों की क्रिया में सहायक के रूप में कार्य करता है। धर्म न तो स्वयं क्रियाशील है और न यह किसी में क्रिया उत्पन्न करता है। पर यह उसकी क्रिया या गति में एक आवश्यक आधार या कारण के रूप में कार्य करता है। अजीव तत्त्व लोकाकाश में व्यापक रूप में रहता है। लेकिन यह रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श विहीन है। यह परिणामी होकर भी नित्य है, क्योंकि उत्पाद और व्यय होने के बावजूद इसका स्वरूप कायम रहता है। गति और परिणाम का यह कारण है।
__ अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में सहायता प्रदान करता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस तरह एक बड़ा पेड़ अपनी छाया में थके पथिक को आराम पहुँचाता है या उसे सहायता प्रदान करता है।१° यह धर्म का प्रतिलोम है और इसमें रस, रूप, गंध एवं स्पर्श का अभाव है। यह अमूर्त, नित्य और लोकाकाश में व्याप्त है।११ धर्म और अधर्म एक साथ लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में रहते हैं, पर दोनों नित्य निराकार और गतिहीन हैं।
धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की तुलना आधुनिक विज्ञान के क्रमश: 'ईथर' तत्त्व और न्यूटन के 'आकर्षण सिद्धांत' से की गई है। जिस प्रकार ईथर को अमूर्त, व्यापक, निष्क्रिय और अदृश्य मानने के साथ-साथ गति का आवश्यक माध्यम भी माना गया है, उसी प्रकार जैन दर्शन में धर्म द्रव्य को भी स्वीकार किया गया है।
अजीव तत्त्वों के अन्तर्गत आकाशास्तिकाय एक ऐसा तत्त्व है, जिसमें जीव, धर्म, अधर्म, काल एवं पद्गल को अपनी-अपनी स्थिति के लिए स्थान की प्राप्ति हो जाती है।१२ यह अदृश्य है और इसका ज्ञान मात्र अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है। बिना आकाश के अस्तिकाय द्रव्यों का विस्तार हो ही नहीं सकता है। १३ जैन विचारक आकाश के दो भेद मानते हैं- लोकाकाश और अलोकाकाश। 'लोकाकाश' आकाश का ही प्रतिरूप है, पर 'अलोकाकाश' में गति का होना संभव नहीं है।१४ लोकाकाश में असंख्य और अलोकाकाश में अनन्त प्रदेश हैं। लोकाकाश में जीव, पद्गल, धर्म और अधर्म का निवास होता है, जबकि अलोकाकाश विश्व के प्रदेश से बाहर है। जैन विचारक लोकाकाश को सान्त मानते हैं और उसके आगे अनन्त आकाश मानते हैं, पर आइंस्टीन ने समस्त लोक को सान्त माना है और वे उससे आगे कुछ नहीं मानते।१५