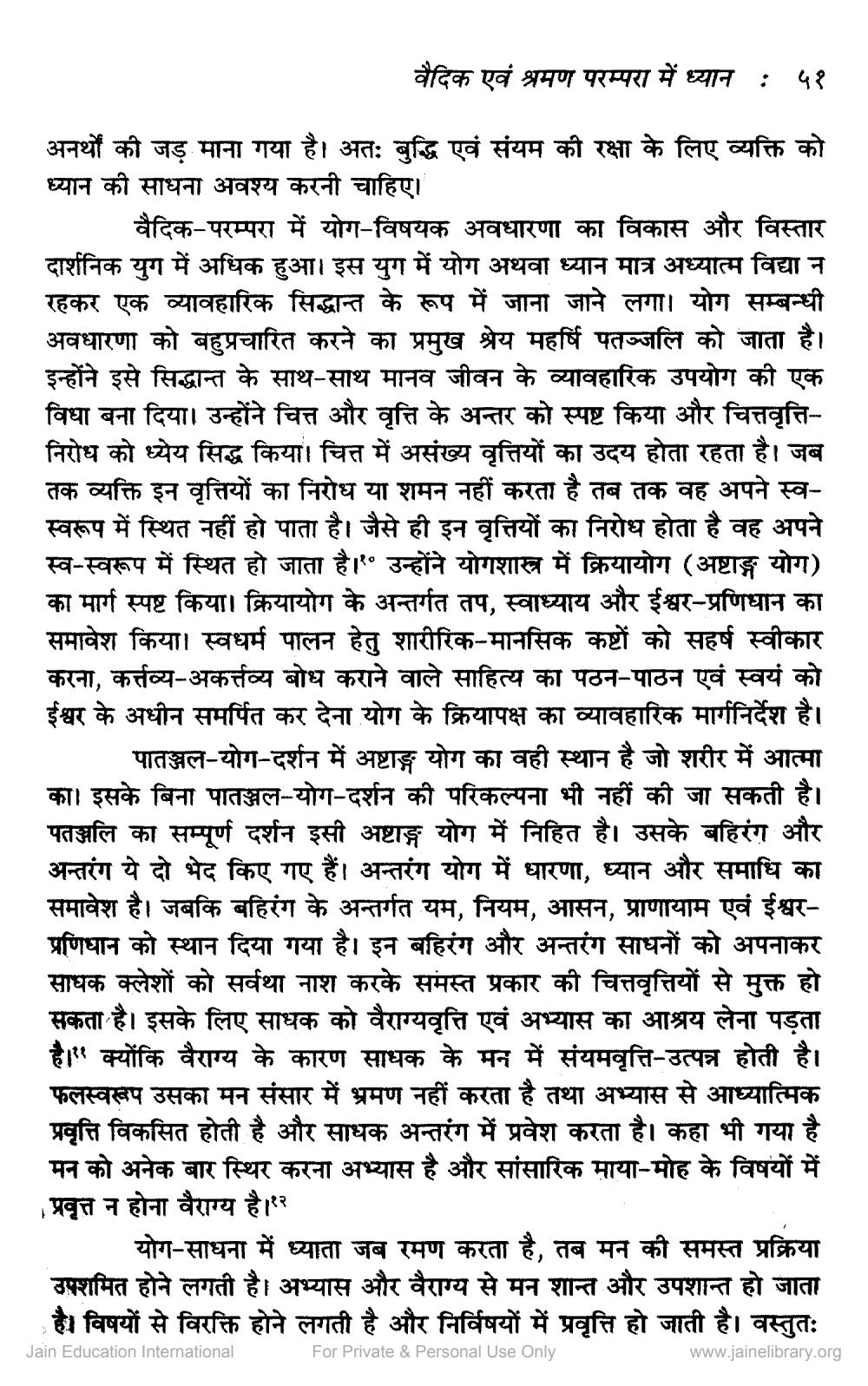________________
वैदिक एवं श्रमण परम्परा में ध्यान : ५१
अनर्थों की जड़ माना गया है। अतः बुद्धि एवं संयम की रक्षा के लिए व्यक्ति को ध्यान की साधना अवश्य करनी चाहिए।
वैदिक-परम्परा में योग-विषयक अवधारणा का विकास और विस्तार दार्शनिक युग में अधिक हुआ। इस युग में योग अथवा ध्यान मात्र अध्यात्म विद्या न रहकर एक व्यावहारिक सिद्धान्त के रूप में जाना जाने लगा। योग सम्बन्धी अवधारणा को बहुप्रचारित करने का प्रमुख श्रेय महर्षि पतञ्जलि को जाता है। इन्होंने इसे सिद्धान्त के साथ-साथ मानव जीवन के व्यावहारिक उपयोग की एक विधा बना दिया। उन्होंने चित्त और वृत्ति के अन्तर को स्पष्ट किया और चित्तवृत्तिनिरोध को ध्येय सिद्ध किया। चित्त में असंख्य वृत्तियों का उदय होता रहता है। जब तक व्यक्ति इन वृत्तियों का निरोध या शमन नहीं करता है तब तक वह अपने स्वस्वरूप में स्थित नहीं हो पाता है। जैसे ही इन वृत्तियों का निरोध होता है वह अपने स्व-स्वरूप में स्थित हो जाता है। उन्होंने योगशास्त्र में क्रियायोग (अष्टाङ्ग योग) का मार्ग स्पष्ट किया। क्रियायोग के अन्तर्गत तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान का समावेश किया। स्वधर्म पालन हेतु शारीरिक-मानसिक कष्टों को सहर्ष स्वीकार करना, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य बोध कराने वाले साहित्य का पठन-पाठन एवं स्वयं को ईश्वर के अधीन समर्पित कर देना योग के क्रियापक्ष का व्यावहारिक मार्गनिर्देश है।
पातञ्जल-योग-दर्शन में अष्टाङ्ग योग का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का। इसके बिना पातञ्जल-योग-दर्शन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। पतञ्जलि का सम्पूर्ण दर्शन इसी अष्टाङ्ग योग में निहित है। उसके बहिरंग और अन्तरंग ये दो भेद किए गए हैं। अन्तरंग योग में धारणा, ध्यान और समाधि का समावेश है। जबकि बहिरंग के अन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं ईश्वरप्रणिधान को स्थान दिया गया है। इन बहिरंग और अन्तरंग साधनों को अपनाकर साधक क्लेशों को सर्वथा नाश करके समस्त प्रकार की चित्तवृत्तियों से मुक्त हो सकता है। इसके लिए साधक को वैराग्यवृत्ति एवं अभ्यास का आश्रय लेना पड़ता है। क्योंकि वैराग्य के कारण साधक के मन में संयमवृत्ति-उत्पन्न होती है। फलस्वस्थप उसका मन संसार में भ्रमण नहीं करता है तथा अभ्यास से आध्यात्मिक प्रवृत्ति विकसित होती है और साधक अन्तरंग में प्रवेश करता है। कहा भी गया है मन को अनेक बार स्थिर करना अभ्यास है और सांसारिक माया-मोह के विषयों में प्रवृत्त न होना वैराग्य है।
योग-साधना में ध्याता जब रमण करता है, तब मन की समस्त प्रक्रिया उपशमित होने लगती है। अभ्यास और वैराग्य से मन शान्त और उपशान्त हो जाता
है। विषयों से विरक्ति होने लगती है और निर्विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। वस्तुतः Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org