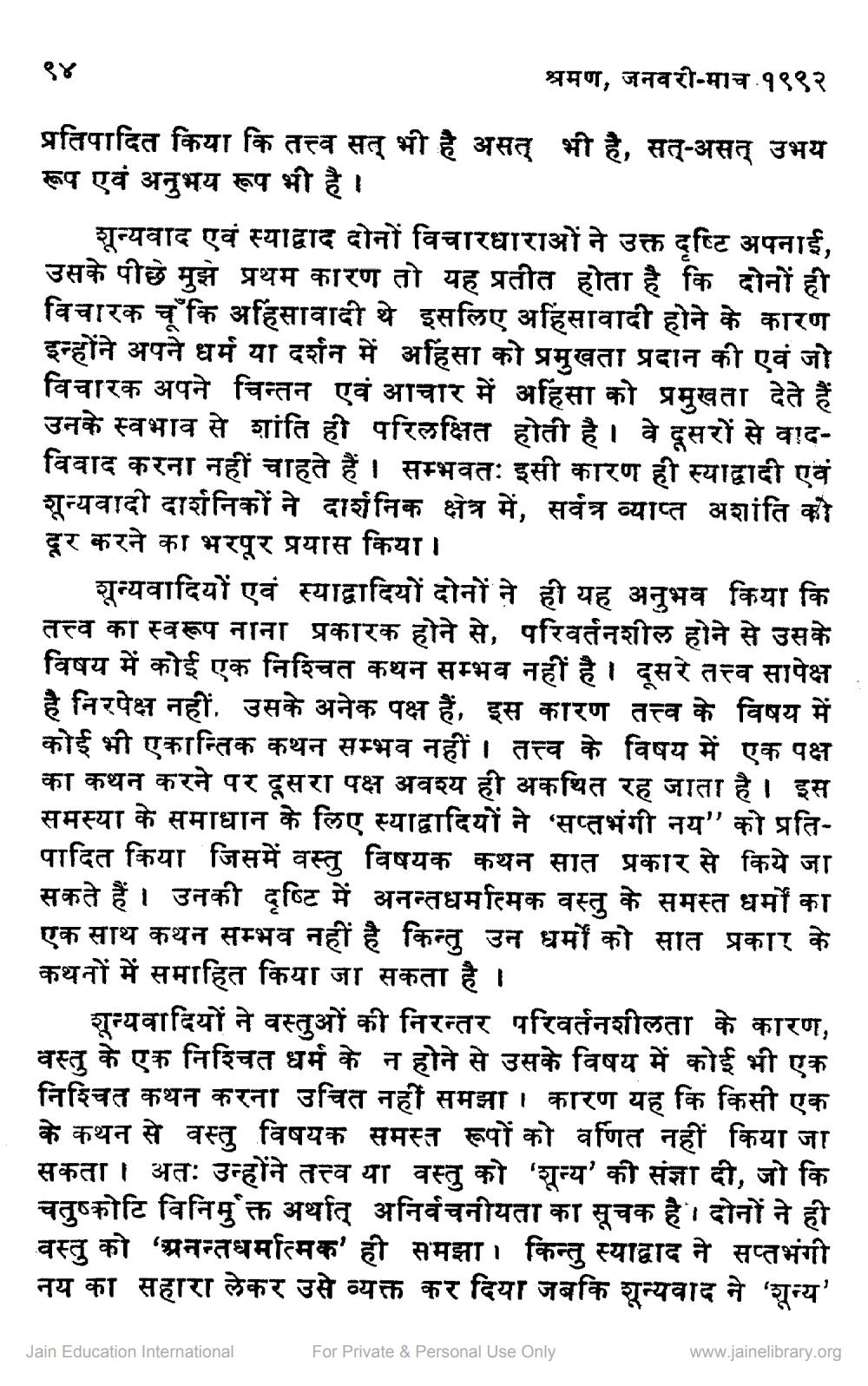________________
श्रमण, जनवरी-मार्च १९९२
प्रतिपादित किया कि तत्त्व सत् भी है असत् भी है, सत्-असत् उभय रूप एवं अनुभय रूप भी है ।
९४
शून्यवाद एवं स्याद्वाद दोनों विचारधाराओं ने उक्त दृष्टि अपनाई, उसके पीछे मुझे प्रथम कारण तो यह प्रतीत होता है कि दोनों ही विचारक चूँकि अहिंसावादी थे इसलिए अहिंसावादी होने के कारण इन्होंने अपने धर्म या दर्शन में अहिंसा को प्रमुखता प्रदान की एवं जो विचारक अपने चिन्तन एवं आचार में अहिंसा को प्रमुखता देते हैं उनके स्वभाव से शांति ही परिलक्षित होती है । वे दूसरों से वादविवाद करना नहीं चाहते हैं । सम्भवतः इसी कारण ही स्याद्वादी एवं शून्यवादी दार्शनिकों ने दार्शनिक क्षेत्र में, सर्वत्र व्याप्त अशांति को दूर करने का भरपूर प्रयास किया ।
शून्यवादियों एवं स्याद्वादियों दोनों ने ही यह अनुभव किया कि तत्त्व का स्वरूप नाना प्रकारक होने से, परिवर्तनशील होने से उसके विषय में कोई एक निश्चित कथन सम्भव नहीं है । दूसरे तत्त्व सापेक्ष है निरपेक्ष नहीं, उसके अनेक पक्ष हैं, इस कारण तत्त्व के विषय में कोई भी एकान्तिक कथन सम्भव नहीं । तत्त्व के विषय में एक पक्ष का कथन करने पर दूसरा पक्ष अवश्य ही अकथित रह जाता है । इस समस्या के समाधान के लिए स्याद्वादियों ने 'सप्तभंगी नय" को प्रतिपादित किया जिसमें वस्तु विषयक कथन सात प्रकार से किये जा सकते हैं । उनकी दृष्टि में अनन्तधर्मात्मक वस्तु के समस्त धर्मों का एक साथ कथन सम्भव नहीं है किन्तु उन धर्मों को सात प्रकार के कथनों में समाहित किया जा सकता है |
शून्यवादियों ने वस्तुओं की निरन्तर परिवर्तनशीलता के कारण, वस्तु के एक निश्चित धर्म के न होने से उसके विषय में कोई भी एक निश्चित कथन करना उचित नहीं समझा। कारण यह कि किसी एक के कथन से वस्तु विषयक समस्त रूपों को वर्णित नहीं किया जा सकता । अतः उन्होंने तत्त्व या वस्तु को 'शून्य' की संज्ञा दी, जो कि चतुष्कोटि विनिर्मुक्त अर्थात् अनिर्वचनीयता का सूचक है। दोनों ने ही वस्तु को 'अनन्तधर्मात्मक' ही समझा । किन्तु स्याद्वाद ने सप्तभंगी नय का सहारा लेकर उसे व्यक्त कर दिया जबकि शून्यवाद ने 'शून्य'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org