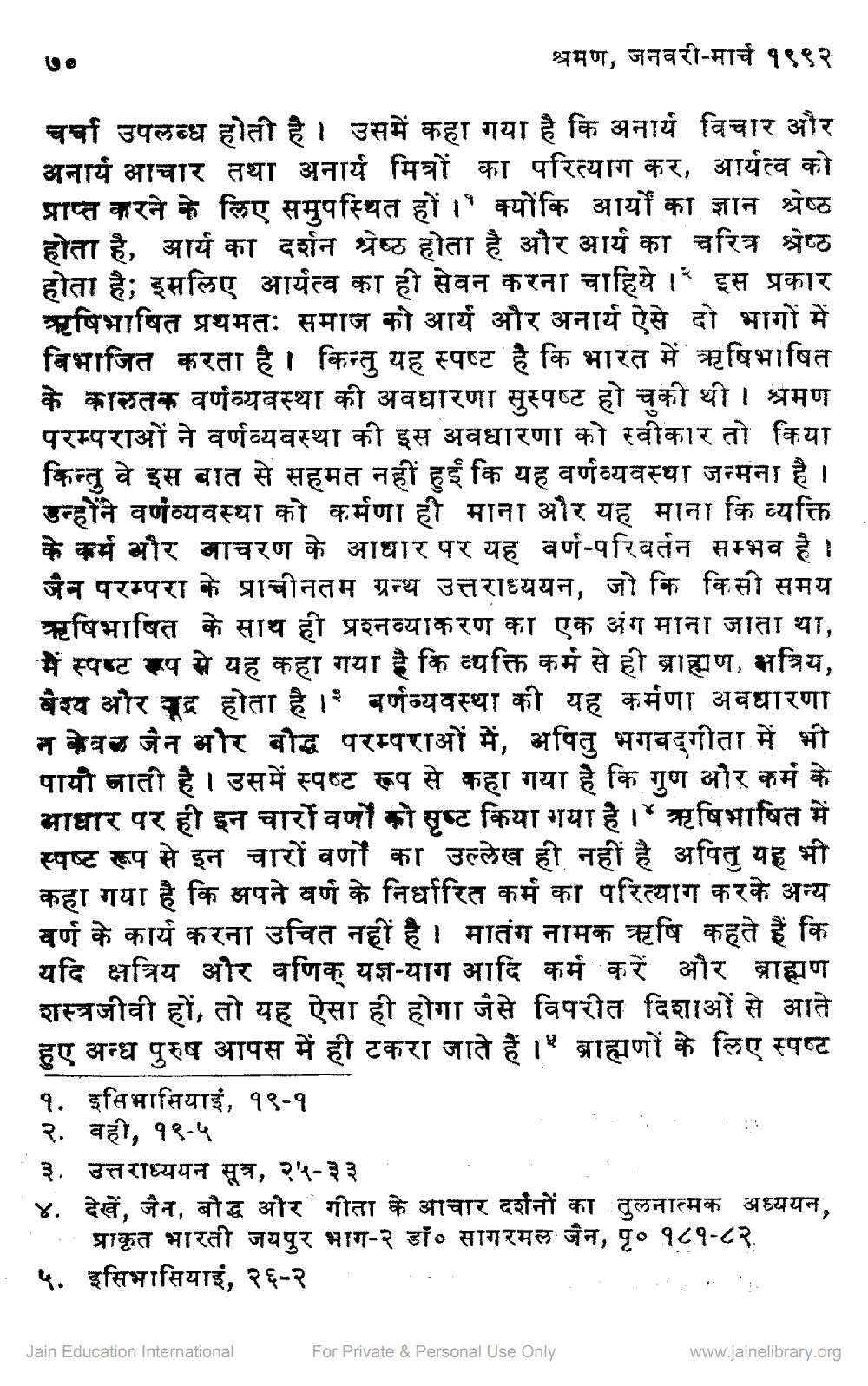________________
श्रमण, जनवरी-मार्च १९९२
चर्चा उपलब्ध होती है। उसमें कहा गया है कि अनार्य विचार और अनार्य आचार तथा अनार्य मित्रों का परित्याग कर, आर्यत्व को प्राप्त करने के लिए समुपस्थित हों।' क्योंकि आर्यों का ज्ञान श्रेष्ठ होता है, आर्य का दर्शन श्रेष्ठ होता है और आर्य का चरित्र श्रेष्ठ होता है; इसलिए आर्यत्व का ही सेवन करना चाहिये । इस प्रकार ऋषिभाषित प्रथमतः समाज को आर्य और अनार्य ऐसे दो भागों में विभाजित करता है। किन्तु यह स्पष्ट है कि भारत में ऋषिभाषित के कालतक वर्णव्यवस्था की अवधारणा सुस्पष्ट हो चकी थी। श्रमण परम्पराओं ने वर्णव्यवस्था की इस अवधारणा को स्वीकार तो किया किन्तु वे इस बात से सहमत नहीं हुई कि यह वर्णव्यवस्था जन्मना है । उन्होंने वर्णव्यवस्था को कर्मणा ही माना और यह माना कि व्यक्ति के कर्म और आचरण के आधार पर यह वर्ण-परिवर्तन सम्भव है । जैन परम्परा के प्राचीनतम ग्रन्थ उत्तराध्ययन, जो कि किसी समय ऋषिभाषित के साथ ही प्रश्नव्याकरण का एक अंग माना जाता था, में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि व्यक्ति कर्म से ही ब्राह्मण, भत्रिय, बैश्य और उद्र होता है । ३ बर्णव्यवस्था की यह कर्मणा अवधारणा न केवल जैन और बौद्ध परम्पराओं में, अपितु भगवद्गीता में भी पायी जाती है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुण और कर्म के माधार पर ही इन चारों वर्गों को सृष्ट किया गया है। ऋषिभाषित में स्पष्ट रूप से इन चारों वर्गों का उल्लेख ही नहीं है अपितु यह भी कहा गया है कि अपने वर्ण के निर्धारित कर्म का परित्याग करके अन्य वर्ण के कार्य करना उचित नहीं है। मातंग नामक ऋषि कहते हैं कि यदि क्षत्रिय और वणिक् यज्ञ-याग आदि कर्म करें और ब्राह्मण शस्त्रजीवी हों, तो यह ऐसा ही होगा जैसे विपरीत दिशाओं से आते हुए अन्ध पुरुष आपस में ही टकरा जाते हैं । ब्राह्मणों के लिए स्पष्ट १. इसिभासियाई, १९-१ २. वही, १९-५ ३. उत्तराध्ययन सूत्र, २५-३३ ४. देखें, जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन, . प्राकृत भारती जयपुर भाग-२ डॉ० सागरमल जैन, पृ० १८१-८२. ५. इसिभासियाई, २६-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org