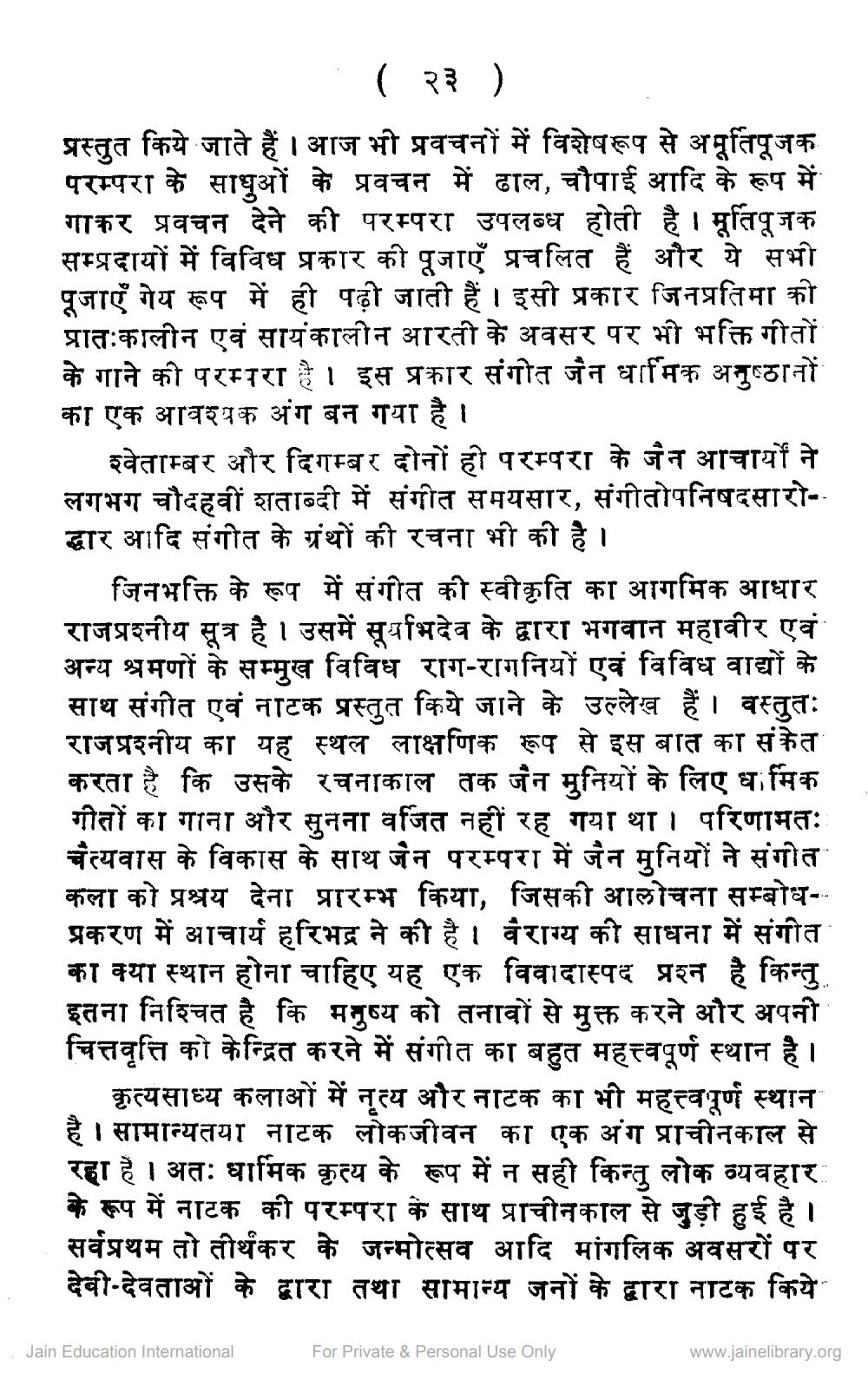________________
( २३ ) प्रस्तुत किये जाते हैं । आज भी प्रवचनों में विशेषरूप से अमूर्तिपूजक परम्परा के साधुओं के प्रवचन में ढाल, चौपाई आदि के रूप में गाकर प्रवचन देने की परम्परा उपलब्ध होती है । मूर्तिपूजक सम्प्रदायों में विविध प्रकार की पूजाएँ प्रचलित हैं और ये सभी पूजाएँ गेय रूप में ही पढ़ी जाती हैं। इसी प्रकार जिनप्रतिमा की प्रातःकालीन एवं सायंकालीन आरती के अवसर पर भी भक्ति गीतों के गाने की परम्परा है। इस प्रकार संगीत जैन धार्मिक अनुष्ठानों का एक आवश्यक अंग बन गया है ।
श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्परा के जैन आचार्यों ने लगभग चौदहवीं शताब्दी में संगीत समयसार, संगीतोपनिषदसारोद्धार आदि संगीत के ग्रंथों की रचना भी की है।
जिनभक्ति के रूप में संगीत की स्वीकृति का आगमिक आधार राजप्रश्नीय सूत्र है । उसमें सूर्याभदेव के द्वारा भगवान महावीर एवं अन्य श्रमणों के सम्मुख विविध राग-रागनियों एवं विविध वाद्यों के साथ संगीत एवं नाटक प्रस्तुत किये जाने के उल्लेख हैं। वस्तुतः राजप्रश्नीय का यह स्थल लाक्षणिक रूप से इस बात का संकेत करता है कि उसके रचनाकाल तक जैन मुनियों के लिए धार्मिक गीतों का गाना और सुनना वजित नहीं रह गया था। परिणामतः चैत्यवास के विकास के साथ जैन परम्परा में जैन मुनियों ने संगीत कला को प्रश्रय देना प्रारम्भ किया, जिसकी आलोचना सम्बोध-.. प्रकरण में आचार्य हरिभद्र ने की है। वैराग्य की साधना में संगीत का क्या स्थान होना चाहिए यह एक विवादास्पद प्रश्न है किन्तु इतना निश्चित है कि मनुष्य को तनावों से मुक्त करने और अपनी चित्तवृत्ति को केन्द्रित करने में संगीत का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है।
कृत्यसाध्य कलाओं में नृत्य और नाटक का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । सामान्यतया नाटक लोकजीवन का एक अंग प्राचीनकाल से रहा है । अतः धार्मिक कृत्य के रूप में न सही किन्तु लोक व्यवहार के रूप में नाटक की परम्परा के साथ प्राचीनकाल से जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम तो तीर्थंकर के जन्मोत्सव आदि मांगलिक अवसरों पर देवी-देवताओं के द्वारा तथा सामान्य जनों के द्वारा नाटक किये
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org