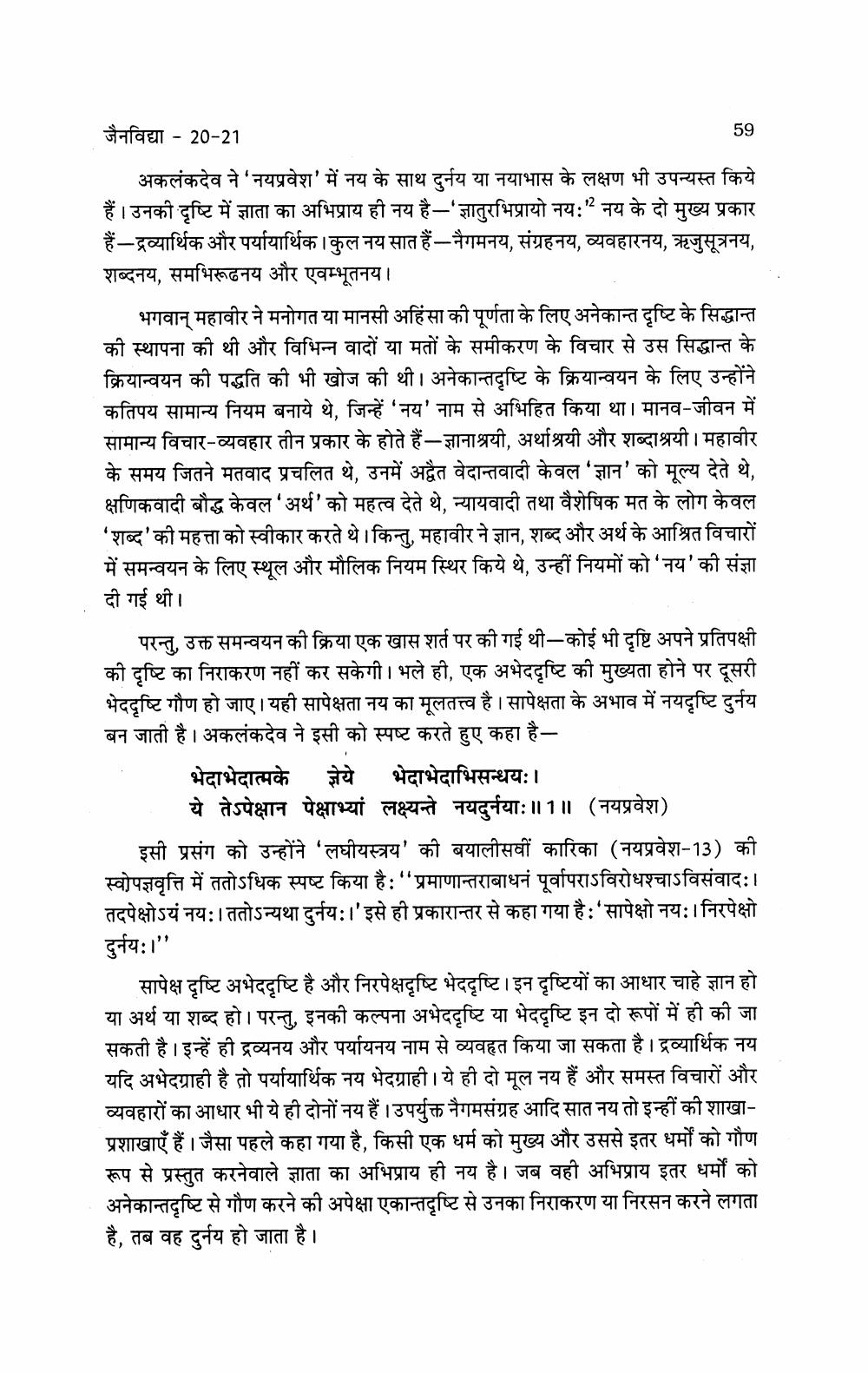________________
जैनविद्या - 20-21
59 अकलंकदेव ने 'नयप्रवेश' में नय के साथ दुर्नय या नयाभास के लक्षण भी उपन्यस्त किये हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञाता का अभिप्राय ही नय है-'ज्ञातुरभिप्रायो नयः” नय के दो मुख्य प्रकार हैं-द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ।कुल नय सात हैं-नैगमनय, संग्रहनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय, शब्दनय, समभिरूढनय और एवम्भूतनय। __ भगवान् महावीर ने मनोगत या मानसी अहिंसा की पूर्णता के लिए अनेकान्त दृष्टि के सिद्धान्त की स्थापना की थी और विभिन्न वादों या मतों के समीकरण के विचार से उस सिद्धान्त के क्रियान्वयन की पद्धति की भी खोज की थी। अनेकान्तदृष्टि के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने कतिपय सामान्य नियम बनाये थे, जिन्हें 'नय' नाम से अभिहित किया था। मानव-जीवन में सामान्य विचार-व्यवहार तीन प्रकार के होते हैं-ज्ञानाश्रयी, अर्थाश्रयी और शब्दाश्रयी। महावीर के समय जितने मतवाद प्रचलित थे, उनमें अद्वैत वेदान्तवादी केवल 'ज्ञान' को मूल्य देते थे, क्षणिकवादी बौद्ध केवल 'अर्थ' को महत्व देते थे, न्यायवादी तथा वैशेषिक मत के लोग केवल 'शब्द' की महत्ता को स्वीकार करते थे। किन्तु, महावीर ने ज्ञान, शब्द और अर्थ के आश्रित विचारों में समन्वयन के लिए स्थूल और मौलिक नियम स्थिर किये थे, उन्हीं नियमों को 'नय' की संज्ञा दी गई थी।
परन्तु, उक्त समन्वयन की क्रिया एक खास शर्त पर की गई थी-कोई भी दृष्टि अपने प्रतिपक्षी की दृष्टि का निराकरण नहीं कर सकेगी। भले ही, एक अभेददृष्टि की मुख्यता होने पर दूसरी भेददृष्टि गौण हो जाए। यही सापेक्षता नय का मूलतत्त्व है । सापेक्षता के अभाव में नयदृष्टि दुर्नय बन जाती है। अकलंकदेव ने इसी को स्पष्ट करते हुए कहा है
भेदाभेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदाभिसन्धयः।
ये तेऽपेक्षान पेक्षाभ्यां लक्ष्यन्ते नयदुर्नयाः॥1॥ (नयप्रवेश) इसी प्रसंग को उन्होंने 'लघीयस्त्रय' की बयालीसवीं कारिका (नयप्रवेश-13) की स्वोपज्ञवृत्ति में ततोऽधिक स्पष्ट किया है: "प्रमाणान्तराबाधनं पूर्वापराऽविरोधश्चाऽविसंवादः। तदपेक्षोऽयं नयः। ततोऽन्यथा दुर्नयः।' इसे ही प्रकारान्तर से कहा गया है : 'सापेक्षो नयः। निरपेक्षो दुर्नयः।"
सापेक्ष दृष्टि अभेददृष्टि है और निरपेक्षदृष्टि भेददृष्टि । इन दृष्टियों का आधार चाहे ज्ञान हो या अर्थ या शब्द हो। परन्तु, इनकी कल्पना अभेददृष्टि या भेददृष्टि इन दो रूपों में ही की जा सकती है। इन्हें ही द्रव्यनय और पर्यायनय नाम से व्यवहत किया जा सकता है। द्रव्यार्थिक नय यदि अभेदग्राही है तो पर्यायार्थिक नय भेदग्राही। ये ही दो मूल नय हैं और समस्त विचारों और व्यवहारों का आधार भी ये ही दोनों नय हैं । उपर्युक्त नैगमसंग्रह आदि सात नय तो इन्हीं की शाखाप्रशाखाएँ हैं । जैसा पहले कहा गया है, किसी एक धर्म को मुख्य और उससे इतर धर्मों को गौण रूप से प्रस्तुत करनेवाले ज्ञाता का अभिप्राय ही नय है। जब वही अभिप्राय इतर धर्मों को अनेकान्तदृष्टि से गौण करने की अपेक्षा एकान्तदृष्टि से उनका निराकरण या निरसन करने लगता है, तब वह दुर्नय हो जाता है।