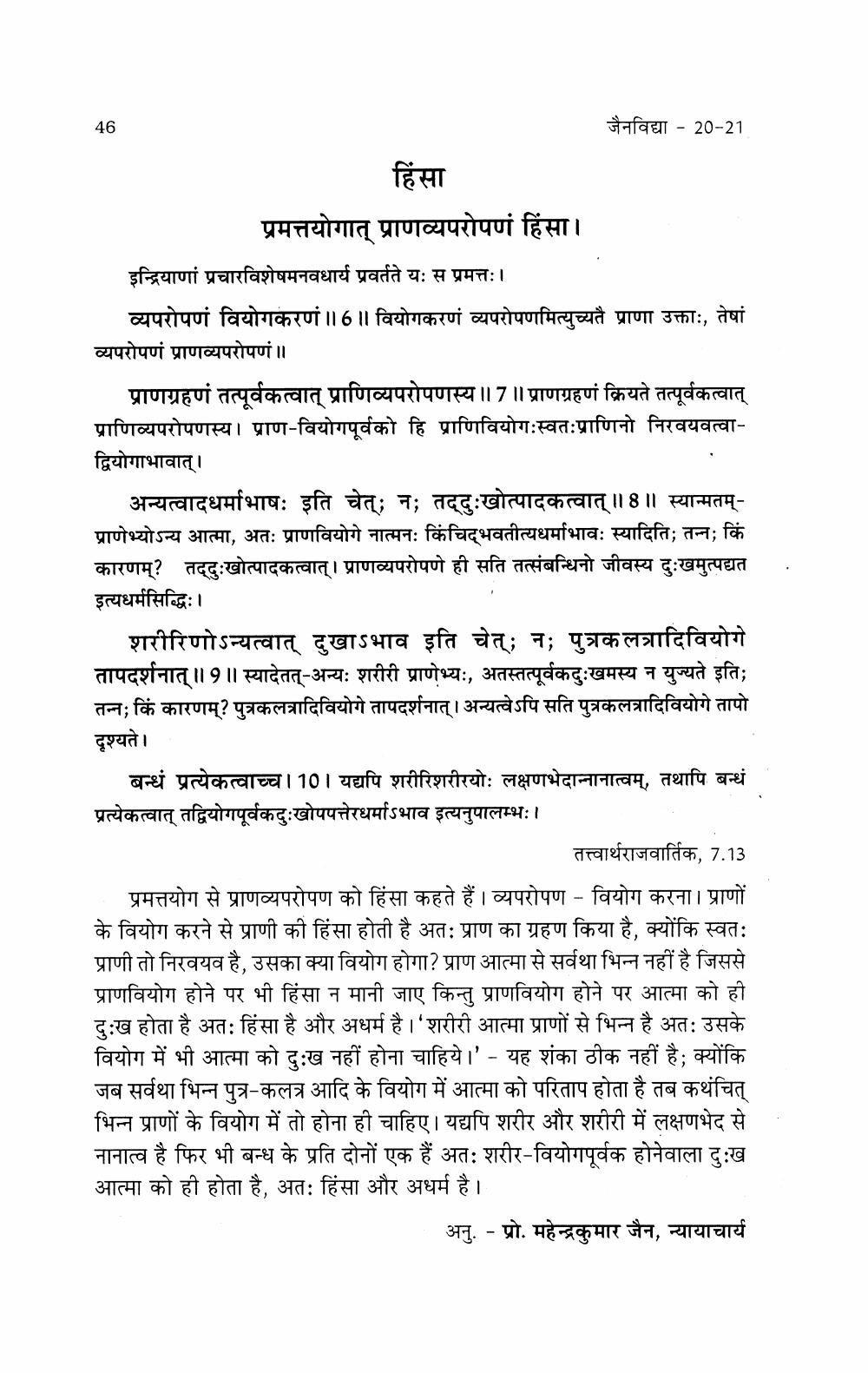________________
46
जैनविद्या - 20-21
हिंसा प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा। इन्द्रियाणां प्रचारविशेषमनवधार्य प्रवर्तते यः स प्रमत्तः।
व्यपरोपणं वियोगकरणं॥6॥ वियोगकरणं व्यपरोपणमित्युच्यतै प्राणा उक्ताः, तेषां व्यपरोपणं प्राणव्यपरोपणं॥
प्राणग्रहणं तत्पूर्वकत्वात् प्राणिव्यपरोपणस्य॥7॥प्राणग्रहणं क्रियते तत्पूर्वकत्वात् प्राणिव्यपरोपणस्य। प्राण-वियोगपूर्वको हि प्राणिवियोग:स्वतःप्राणिनो निरवयवत्वाद्वियोगाभावात्।
अन्यत्वादधर्माभाषः इति चेत्, न; तदुःखोत्पादकत्वात्॥8॥ स्यान्मतम्प्राणेभ्योऽन्य आत्मा, अतः प्राणवियोगे नात्मनः किंचिद्भवतीत्यधर्माभावः स्यादिति; तन्न; किं कारणम्? तदुःखोत्पादकत्वात्। प्राणव्यपरोपणे ही सति तत्संबन्धिनो जीवस्य दुःखमुत्पद्यत इत्यधर्मसिद्धिः।
शरीरिणोऽन्यत्वात् दुखाऽभाव इति चेत्, न; पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात्॥9॥ स्यादेतत्-अन्यः शरीरी प्राणेभ्यः, अतस्तत्पूर्वकदुःखमस्य न युज्यते इति; तन्न; किं कारणम्? पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात् । अन्यत्वेऽपि सति पुत्रकलत्रादिवियोगे तापो दृश्यते।
बन्धं प्रत्येकत्वाच्च। 10। यद्यपि शरीरिशरीरयोः लक्षणभेदान्नानात्वम्, तथापि बन्धं प्रत्येकत्वात् तद्वियोगपूर्वकदुःखोपपत्तेरधर्माऽभाव इत्यनुपालम्भः।
तत्त्वार्थराजवार्तिक, 7.13 प्रमत्तयोग से प्राणव्यपरोपण को हिंसा कहते हैं । व्यपरोपण - वियोग करना। प्राणों के वियोग करने से प्राणी की हिंसा होती है अत: प्राण का ग्रहण किया है, क्योंकि स्वतः प्राणी तो निरवयव है, उसका क्या वियोग होगा? प्राण आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं है जिससे प्राणवियोग होने पर भी हिंसा न मानी जाए किन्तु प्राणवियोग होने पर आत्मा को ही दुःख होता है अत: हिंसा है और अधर्म है। 'शरीरी आत्मा प्राणों से भिन्न है अत: उसके वियोग में भी आत्मा को दुःख नहीं होना चाहिये।' - यह शंका ठीक नहीं है; क्योंकि जब सर्वथा भिन्न पुत्र-कलत्र आदि के वियोग में आत्मा को परिताप होता है तब कथंचित् भिन्न प्राणों के वियोग में तो होना ही चाहिए। यद्यपि शरीर और शरीरी में लक्षणभेद से नानात्व है फिर भी बन्ध के प्रति दोनों एक हैं अतः शरीर-वियोगपूर्वक होनेवाला दु:ख आत्मा को ही होता है, अतः हिंसा और अधर्म है।
अनु. - प्रो. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य