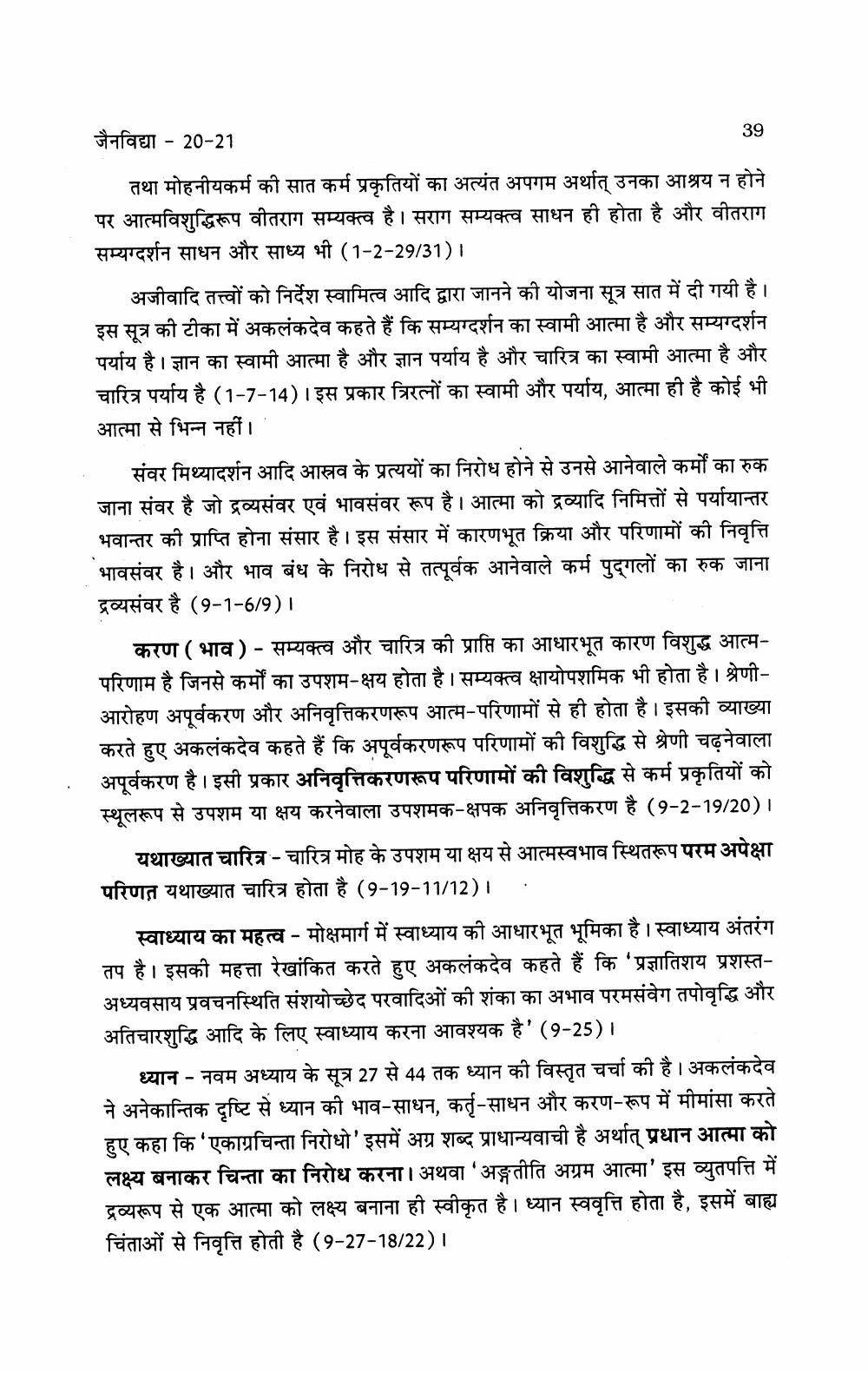________________
जैनविद्या - 20-21
39 ___ तथा मोहनीयकर्म की सात कर्म प्रकृतियों का अत्यंत अपगम अर्थात् उनका आश्रय न होने पर आत्मविशुद्धिरूप वीतराग सम्यक्त्व है। सराग सम्यक्त्व साधन ही होता है और वीतराग सम्यग्दर्शन साधन और साध्य भी (1-2-29/31)।
अजीवादि तत्त्वों को निर्देश स्वामित्व आदि द्वारा जानने की योजना सूत्र सात में दी गयी है। इस सूत्र की टीका में अकलंकदेव कहते हैं कि सम्यग्दर्शन का स्वामी आत्मा है और सम्यग्दर्शन पर्याय है। ज्ञान का स्वामी आत्मा है और ज्ञान पर्याय है और चारित्र का स्वामी आत्मा है और चारित्र पर्याय है (1-7-14)। इस प्रकार त्रिरत्नों का स्वामी और पर्याय, आत्मा ही है कोई भी आत्मा से भिन्न नहीं।
संवर मिथ्यादर्शन आदि आस्रव के प्रत्ययों का निरोध होने से उनसे आनेवाले कर्मों का रुक जाना संवर है जो द्रव्यसंवर एवं भावसंवर रूप है। आत्मा को द्रव्यादि निमित्तों से पर्यायान्तर भवान्तर की प्राप्ति होना संसार है। इस संसार में कारणभूत क्रिया और परिणामों की निवृत्ति भावसंवर है। और भाव बंध के निरोध से तत्पूर्वक आनेवाले कर्म पुद्गलों का रुक जाना द्रव्यसंवर है (9-1-6/9)।
करण (भाव) - सम्यक्त्व और चारित्र की प्राप्ति का आधारभूत कारण विशुद्ध आत्मपरिणाम है जिनसे कर्मों का उपशम-क्षय होता है। सम्यक्त्व क्षायोपशमिक भी होता है। श्रेणीआरोहण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणरूप आत्म-परिणामों से ही होता है। इसकी व्याख्या करते हुए अकलंकदेव कहते हैं कि अपूर्वकरणरूप परिणामों की विशुद्धि से श्रेणी चढ़नेवाला अपूर्वकरण है। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणरूप परिणामों की विशुद्धि से कर्म प्रकृतियों को स्थूलरूप से उपशम या क्षय करनेवाला उपशमक-क्षपक अनिवृत्तिकरण है (9-2-19/20)।
यथाख्यात चारित्र- चारित्र मोह के उपशम या क्षय से आत्मस्वभाव स्थितरूप परम अपेक्षा परिणत यथाख्यात चारित्र होता है (9-19-11/12)। .
स्वाध्याय का महत्व - मोक्षमार्ग में स्वाध्याय की आधारभूत भूमिका है। स्वाध्याय अंतरंग तप है। इसकी महत्ता रेखांकित करते हुए अकलंकदेव कहते हैं कि 'प्रज्ञातिशय प्रशस्तअध्यवसाय प्रवचनस्थिति संशयोच्छेद परवादिओं की शंका का अभाव परमसंवेग तपोवृद्धि और अतिचारशुद्धि आदि के लिए स्वाध्याय करना आवश्यक है' (9-25)।
ध्यान - नवम अध्याय के सूत्र 27 से 44 तक ध्यान की विस्तृत चर्चा की है। अकलंकदेव ने अनेकान्तिक दृष्टि से ध्यान की भाव-साधन, कर्तृ-साधन और करण-रूप में मीमांसा करते हुए कहा कि 'एकाग्रचिन्ता निरोधो' इसमें अग्र शब्द प्राधान्यवाची है अर्थात् प्रधान आत्मा को लक्ष्य बनाकर चिन्ता का निरोध करना। अथवा 'अङ्गतीति अग्रम आत्मा' इस व्युतपत्ति में द्रव्यरूप से एक आत्मा को लक्ष्य बनाना ही स्वीकृत है। ध्यान स्ववृत्ति होता है, इसमें बाह्य चिंताओं से निवृत्ति होती है (9-27-18/22)।