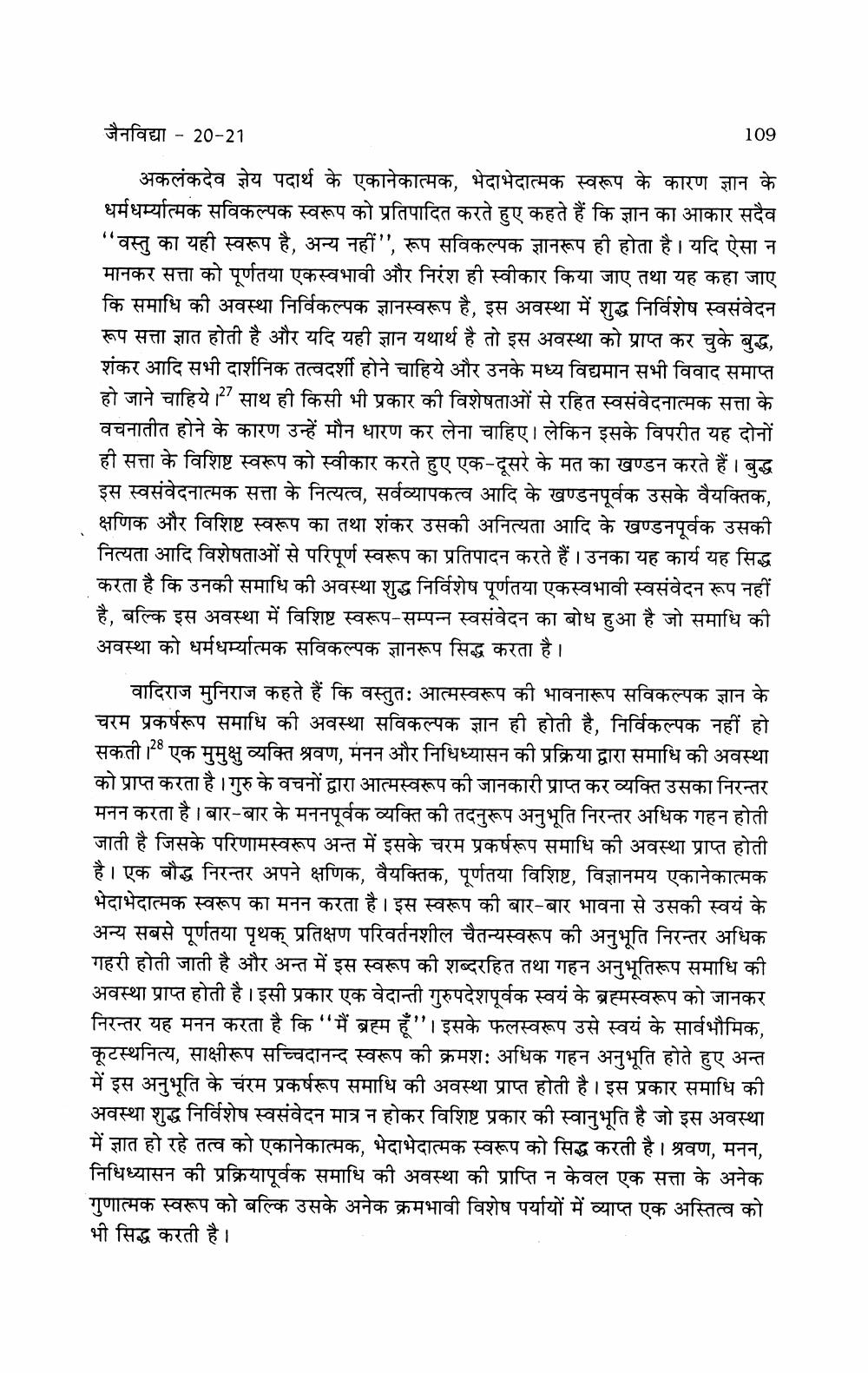________________
जैनविद्या - 20-21
109 अकलंकदेव ज्ञेय पदार्थ के एकानेकात्मक, भेदाभेदात्मक स्वरूप के कारण ज्ञान के धर्मधात्मक सविकल्पक स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान का आकार सदैव "वस्तु का यही स्वरूप है, अन्य नहीं", रूप सविकल्पक ज्ञानरूप ही होता है। यदि ऐसा न मानकर सत्ता को पूर्णतया एकस्वभावी और निरंश ही स्वीकार किया जाए तथा यह कहा जाए कि समाधि की अवस्था निर्विकल्पक ज्ञानस्वरूप है, इस अवस्था में शुद्ध निर्विशेष स्वसंवेदन रूप सत्ता ज्ञात होती है और यदि यही ज्ञान यथार्थ है तो इस अवस्था को प्राप्त कर चुके बुद्ध, शंकर आदि सभी दार्शनिक तत्वदर्शी होने चाहिये और उनके मध्य विद्यमान सभी विवाद समाप्त हो जाने चाहिये। साथ ही किसी भी प्रकार की विशेषताओं से रहित स्वसंवेदनात्मक सत्ता के वचनातीत होने के कारण उन्हें मौन धारण कर लेना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत यह दोनों ही सत्ता के विशिष्ट स्वरूप को स्वीकार करते हुए एक-दूसरे के मत का खण्डन करते हैं । बुद्ध इस स्वसंवेदनात्मक सत्ता के नित्यत्व, सर्वव्यापकत्व आदि के खण्डनपूर्वक उसके वैयक्तिक, क्षणिक और विशिष्ट स्वरूप का तथा शंकर उसकी अनित्यता आदि के खण्डनपूर्वक उसकी नित्यता आदि विशेषताओं से परिपूर्ण स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं । उनका यह कार्य यह सिद्ध करता है कि उनकी समाधि की अवस्था शुद्ध निर्विशेष पूर्णतया एकस्वभावी स्वसंवेदन रूप नहीं है, बल्कि इस अवस्था में विशिष्ट स्वरूप-सम्पन्न स्वसंवेदन का बोध हुआ है जो समाधि की अवस्था को धर्मधात्मक सविकल्पक ज्ञानरूप सिद्ध करता है।
वादिराज मुनिराज कहते हैं कि वस्तुतः आत्मस्वरूप की भावनारूप सविकल्पक ज्ञान के चरम प्रकर्षरूप समाधि की अवस्था सविकल्पक ज्ञान ही होती है, निर्विकल्पक नहीं हो सकती। एक मुमुक्षु व्यक्ति श्रवण, मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया द्वारा समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। गुरु के वचनों द्वारा आत्मस्वरूप की जानकारी प्राप्त कर व्यक्ति उसका निरन्तर मनन करता है। बार-बार के मननपूर्वक व्यक्ति की तदनुरूप अनुभूति निरन्तर अधिक गहन होती जाती है जिसके परिणामस्वरूप अन्त में इसके चरम प्रकर्षरूप समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। एक बौद्ध निरन्तर अपने क्षणिक, वैयक्तिक, पूर्णतया विशिष्ट, विज्ञानमय एकानेकात्मक भेदाभेदात्मक स्वरूप का मनन करता है। इस स्वरूप की बार-बार भावना से उसकी स्वयं के अन्य सबसे पूर्णतया पृथक् प्रतिक्षण परिवर्तनशील चैतन्यस्वरूप की अनुभूति निरन्तर अधिक गहरी होती जाती है और अन्त में इस स्वरूप की शब्दरहित तथा गहन अनुभूतिरूप समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक वेदान्ती गुरुपदेशपूर्वक स्वयं के ब्रह्मस्वरूप को जानकर निरन्तर यह मनन करता है कि "मैं ब्रह्म हूँ"। इसके फलस्वरूप उसे स्वयं के सार्वभौमिक, कूटस्थनित्य, साक्षीरूप सच्चिदानन्द स्वरूप की क्रमशः अधिक गहन अनुभूति होते हुए अन्त में इस अनुभूति के चरम प्रकर्षरूप समाधि की अवस्था प्राप्त होती है । इस प्रकार समाधि की अवस्था शुद्ध निर्विशेष स्वसंवेदन मात्र न होकर विशिष्ट प्रकार की स्वानुभूति है जो इस अवस्था में ज्ञात हो रहे तत्व को एकानेकात्मक, भेदाभेदात्मक स्वरूप को सिद्ध करती है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन की प्रक्रियापूर्वक समाधि की अवस्था की प्राप्ति न केवल एक सत्ता के अनेक गुणात्मक स्वरूप को बल्कि उसके अनेक क्रमभावी विशेष पर्यायों में व्याप्त एक अस्तित्व को भी सिद्ध करती है।