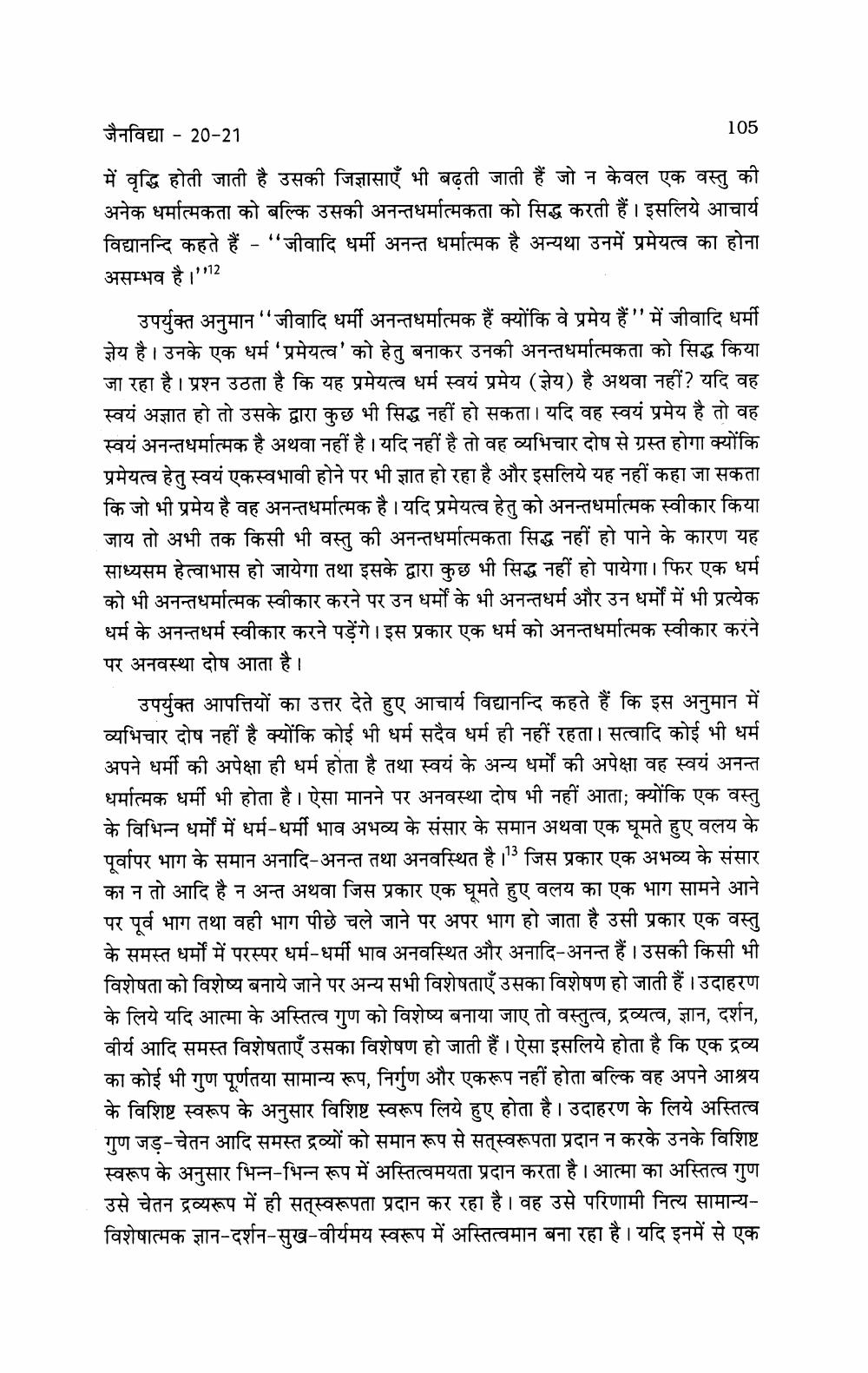________________
जैनविद्या - 20-21
105 में वृद्धि होती जाती है उसकी जिज्ञासाएँ भी बढ़ती जाती हैं जो न केवल एक वस्तु की
अनेक धर्मात्मकता को बल्कि उसकी अनन्तधर्मात्मकता को सिद्ध करती हैं। इसलिये आचार्य विद्यानन्दि कहते हैं - "जीवादि धर्मी अनन्त धर्मात्मक है अन्यथा उनमें प्रमेयत्व का होना असम्भव है। 12
उपर्युक्त अनुमान "जीवादि धर्मी अनन्तधर्मात्मक हैं क्योंकि वे प्रमेय हैं" में जीवादि धर्मी ज्ञेय है। उनके एक धर्म ‘प्रमेयत्व' को हेतु बनाकर उनकी अनन्तधर्मात्मकता को सिद्ध किया जा रहा है। प्रश्न उठता है कि यह प्रमेयत्व धर्म स्वयं प्रमेय (ज्ञेय) है अथवा नहीं? यदि वह स्वयं अज्ञात हो तो उसके द्वारा कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। यदि वह स्वयं प्रमेय है तो वह स्वयं अनन्तधर्मात्मक है अथवा नहीं है। यदि नहीं है तो वह व्यभिचार दोष से ग्रस्त होगा क्योंकि प्रमेयत्व हेतु स्वयं एकस्वभावी होने पर भी ज्ञात हो रहा है और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जो भी प्रमेय है वह अनन्तधर्मात्मक है। यदि प्रमेयत्व हेतु को अनन्तधर्मात्मक स्वीकार किया जाय तो अभी तक किसी भी वस्तु की अनन्तधर्मात्मकता सिद्ध नहीं हो पाने के कारण यह साध्यसम हेत्वाभास हो जायेगा तथा इसके द्वारा कुछ भी सिद्ध नहीं हो पायेगा। फिर एक धर्म को भी अनन्तधर्मात्मक स्वीकार करने पर उन धर्मों के भी अनन्तधर्म और उन धर्मों में भी प्रत्येक धर्म के अनन्तधर्म स्वीकार करने पड़ेंगे। इस प्रकार एक धर्म को अनन्तधर्मात्मक स्वीकार करने पर अनवस्था दोष आता है।
उपर्युक्त आपत्तियों का उत्तर देते हुए आचार्य विद्यानन्दि कहते हैं कि इस अनुमान में व्यभिचार दोष नहीं है क्योंकि कोई भी धर्म सदैव धर्म ही नहीं रहता। सत्वादि कोई भी धर्म अपने धर्मी की अपेक्षा ही धर्म होता है तथा स्वयं के अन्य धर्मों की अपेक्षा वह स्वयं अनन्त धर्मात्मक धर्मी भी होता है। ऐसा मानने पर अनवस्था दोष भी नहीं आता; क्योंकि एक वस्तु के विभिन्न धर्मों में धर्म-धर्मी भाव अभव्य के संसार के समान अथवा एक घूमते हुए वलय के पूर्वापर भाग के समान अनादि-अनन्त तथा अनवस्थित है। जिस प्रकार एक अभव्य के संसार का न तो आदि है न अन्त अथवा जिस प्रकार एक घूमते हुए वलय का एक भाग सामने आने पर पूर्व भाग तथा वही भाग पीछे चले जाने पर अपर भाग हो जाता है उसी प्रकार एक वस्तु के समस्त धर्मों में परस्पर धर्म-धर्मी भाव अनवस्थित और अनादि-अनन्त हैं । उसकी किसी भी विशेषता को विशेष्य बनाये जाने पर अन्य सभी विशेषताएँ उसका विशेषण हो जाती हैं। उदाहरण के लिये यदि आत्मा के अस्तित्व गुण को विशेष्य बनाया जाए तो वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि समस्त विशेषताएँ उसका विशेषण हो जाती हैं । ऐसा इसलिये होता है कि एक द्रव्य का कोई भी गण पूर्णतया सामान्य रूप, निर्गण और एकरूप नहीं होता बल्कि वह अपने आश्रय के विशिष्ट स्वरूप के अनुसार विशिष्ट स्वरूप लिये हुए होता है। उदाहरण के लिये अस्तित्व गुण जड़-चेतन आदि समस्त द्रव्यों को समान रूप से सत्स्वरूपता प्रदान न करके उनके विशिष्ट स्वरूप के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में अस्तित्वमयता प्रदान करता है । आत्मा का अस्तित्व गुण उसे चेतन द्रव्यरूप में ही सत्स्वरूपता प्रदान कर रहा है। वह उसे परिणामी नित्य सामान्यविशेषात्मक ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यमय स्वरूप में अस्तित्वमान बना रहा है। यदि इनमें से एक