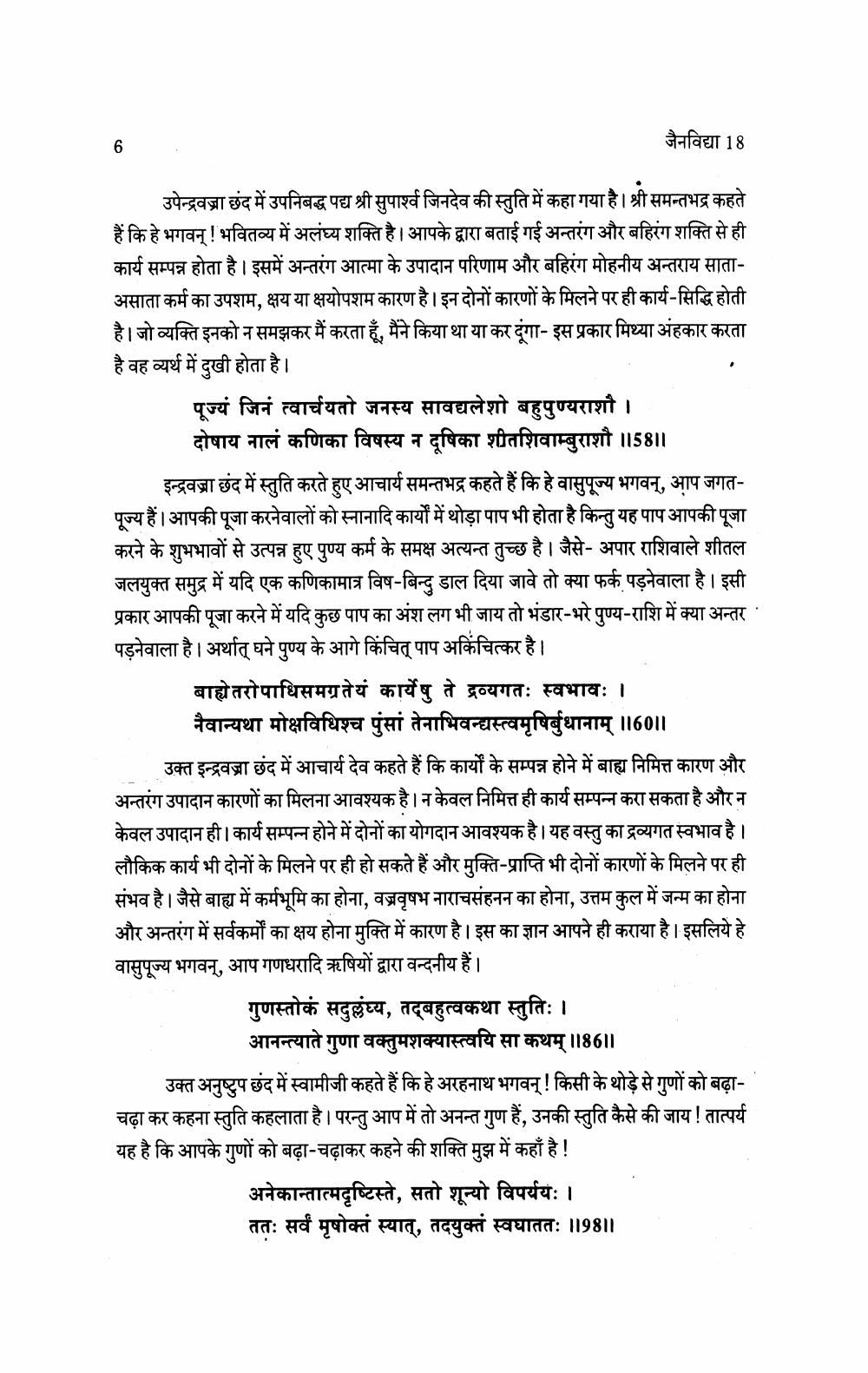________________
जैनविद्या 18
उपेन्द्रवज्रा छंद में उपनिबद्ध पद्य श्री सुपार्श्व जिनदेव की स्तुति में कहा गया है। श्री समन्तभद्र कहते हैं कि हे भगवन् ! भवितव्य में अलंघ्य शक्ति है। आपके द्वारा बताई गई अन्तरंग और बहिरंग शक्ति से ही कार्य सम्पन्न होता है। इसमें अन्तरंग आत्मा के उपादान परिणाम और बहिरंग मोहनीय अन्तराय साताअसाता कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम कारण है। इन दोनों कारणों के मिलने पर ही कार्य-सिद्धि होती है। जो व्यक्ति इनको न समझकर मैं करता हूँ, मैंने किया था या कर दूंगा- इस प्रकार मिथ्या अंहकार करता है वह व्यर्थ में दुखी होता है।
पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ ।
दोषाय नालं कणिका विषस्य न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ ॥58॥ इन्द्रवज्रा छंद में स्तुति करते हुए आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि हे वासुपूज्य भगवन्, आप जगतपूज्य हैं। आपकी पूजा करनेवालों को स्नानादि कार्यों में थोड़ा पाप भी होता है किन्तु यह पाप आपकी पूजा करने के शुभभावों से उत्पन्न हुए पुण्य कर्म के समक्ष अत्यन्त तुच्छ है। जैसे- अपार राशिवाले शीतल जलयुक्त समुद्र में यदि एक कणिकामात्र विष-बिन्दु डाल दिया जावे तो क्या फर्क पड़नेवाला है। इसी प्रकार आपकी पूजा करने में यदि कुछ पाप का अंश लग भी जाय तो भंडार-भरे पुण्य-राशि में क्या अन्तर । पड़नेवाला है। अर्थात् घने पुण्य के आगे किंचित् पाप अकिंचित्कर है।
बाह्ये तरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः ।
नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसां तेनाभिवन्धस्त्वमृषिर्बुधानाम् ॥6॥ उक्त इन्द्रवज्रा छंद में आचार्य देव कहते हैं कि कार्यों के सम्पन्न होने में बाह्य निमित्त कारण और अन्तरंग उपादान कारणों का मिलना आवश्यक है। न केवल निमित्त ही कार्य सम्पन्न करा सकता है और न केवल उपादान ही। कार्य सम्पन्न होने में दोनों का योगदान आवश्यक है। यह वस्तु का द्रव्यगत स्वभाव है। लौकिक कार्य भी दोनों के मिलने पर ही हो सकते हैं और मुक्ति-प्राप्ति भी दोनों कारणों के मिलने पर ही संभव है। जैसे बाह्य में कर्मभूमि का होना, वज्रवृषभ नाराचसंहनन का होना, उत्तम कुल में जन्म का होना
और अन्तरंग में सर्वकर्मों का क्षय होना मुक्ति में कारण है। इस का ज्ञान आपने ही कराया है। इसलिये हे वासुपूज्य भगवन्, आप गणधरादि ऋषियों द्वारा वन्दनीय हैं।
गुणस्तोकं सदुल्लंघ्य, तद्बहुत्वकथा स्तुतिः ।
आनन्त्याते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम् ॥86॥ उक्त अनुष्टुप छंद में स्वामीजी कहते हैं कि हे अरहनाथ भगवन् ! किसी के थोड़े से गुणों को बढ़ाचढ़ा कर कहना स्तुति कहलाता है। परन्तु आप में तो अनन्त गुण हैं, उनकी स्तुति कैसे की जाय ! तात्पर्य यह है कि आपके गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर कहने की शक्ति मुझ में कहाँ है !
अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते, सतो शून्यो विपर्ययः । ततः सर्वं मृषोक्तं स्यात्, तदयुक्तं स्वघाततः ॥98॥