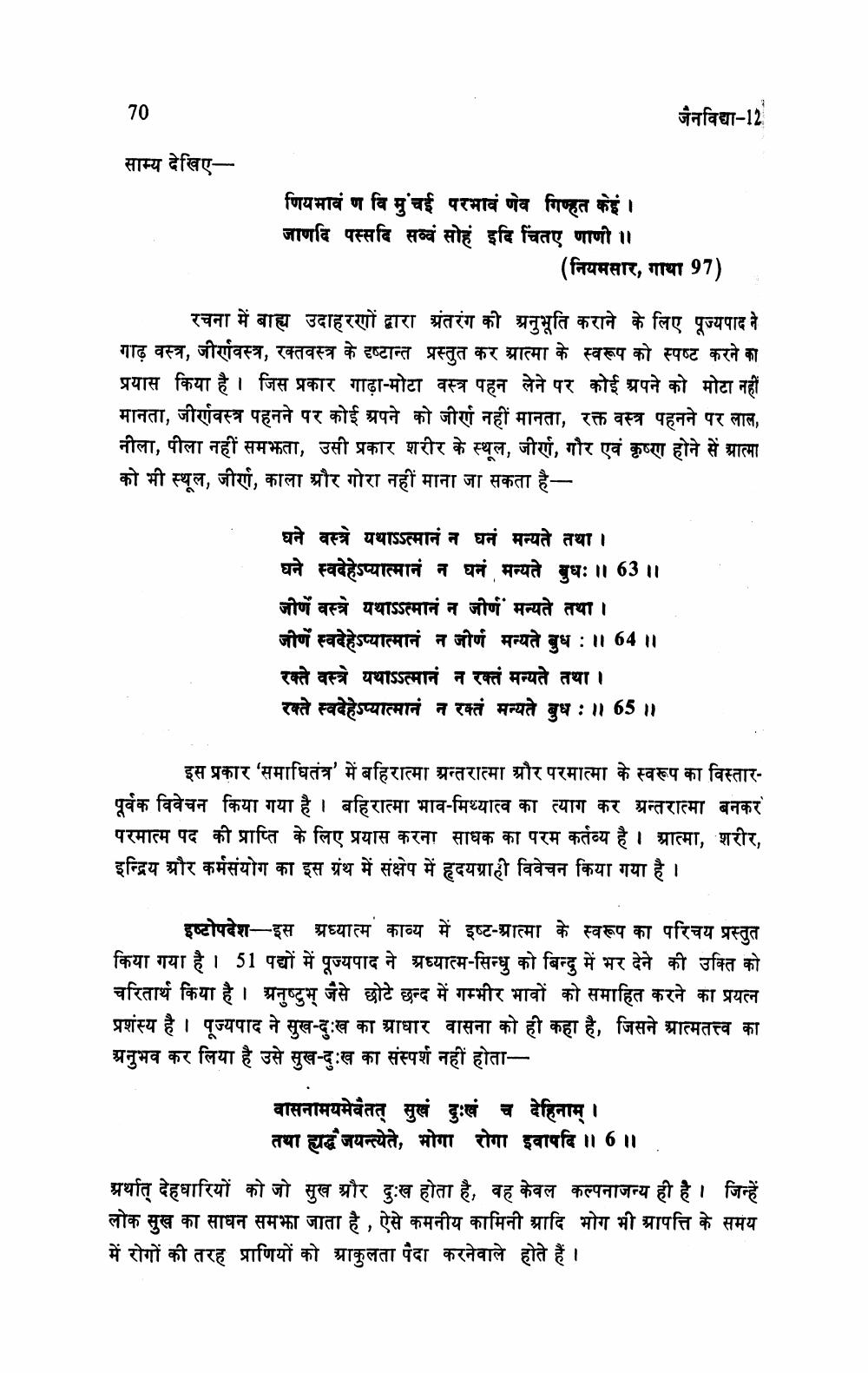________________
70
जनविद्या-12
साम्य देखिए
णियमावं ण वि मुंचई परभावं व गिण्हत कई । जाणदि पस्सदि सव्वं सोहं इदि चितए णाणी ॥
(नियमसार, गाया 97)
रचना में बाह्य उदाहरणों द्वारा अंतरंग की अनुभूति कराने के लिए पूज्यपाद ने गाढ़ वस्त्र, जीर्णवस्त्र, रक्तवस्त्र के दृष्टान्त प्रस्तुत कर आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार गाढ़ा-मोटा वस्त्र पहन लेने पर कोई अपने को मोटा नहीं मानता, जीर्णवस्त्र पहनने पर कोई अपने को जीर्ण नहीं मानता, रक्त वस्त्र पहनने पर लाल, नीला, पीला नहीं समझता, उसी प्रकार शरीर के स्थूल, जीर्ण, गौर एवं कृष्ण होने से आत्मा को भी स्थल, जीर्ण, काला और गोरा नहीं माना जा सकता है
घने वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न घनं मन्यते तथा। घने स्वदेहेऽप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधः। 63 ॥ जीणे वस्त्रे यथाऽत्मानं न जीर्ण मन्यते तथा। जोणे स्वदेहेऽप्यात्मानं न जीर्ण मन्यते बुध : ॥ 64॥ रक्ते वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न रक्तं मन्यते तथा । रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुध :॥ 65॥
इस प्रकार 'समाधितंत्र' में बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है । बहिरात्मा भाव-मिथ्यात्व का त्याग कर अन्तरात्मा बनकर परमात्म पद की प्राप्ति के लिए प्रयास करना साधक का परम कर्तव्य है। आत्मा, शरीर, इन्द्रिय और कर्मसंयोग का इस ग्रंथ में संक्षेप में हृदयग्राही विवेचन किया गया है ।
इष्टोपदेश-इस अध्यात्म काव्य में इष्ट-प्रात्मा के स्वरूप का परिचय प्रस्तुत किया गया है। 51 पद्यों में पूज्यपाद ने अध्यात्म-सिन्धु को बिन्दु में भर देने की उक्ति को चरितार्थ किया है। अनुष्टुम् जैसे छोटे छन्द में गम्भीर भावों को समाहित करने का प्रयत्न प्रशंस्य है । पूज्यपाद ने सुख-दुःख का आधार वासना को ही कहा है, जिसने आत्मतत्त्व का अनुभव कर लिया है उसे सुख-दुःख का संस्पर्श नहीं होता
वासनामयमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनाम् ।
तथा ह्यद्ध जयन्त्येते, भोगा रोगा इवापदि ॥6॥ अर्थात् देहधारियों को जो सुख और दुःख होता है, वह केवल कल्पनाजन्य ही है। जिन्हें लोक सुख का साधन समझा जाता है , ऐसे कमनीय कामिनी आदि भोग भी आपत्ति के समय में रोगों की तरह प्राणियों को प्राकुलता पैदा करनेवाले होते हैं ।