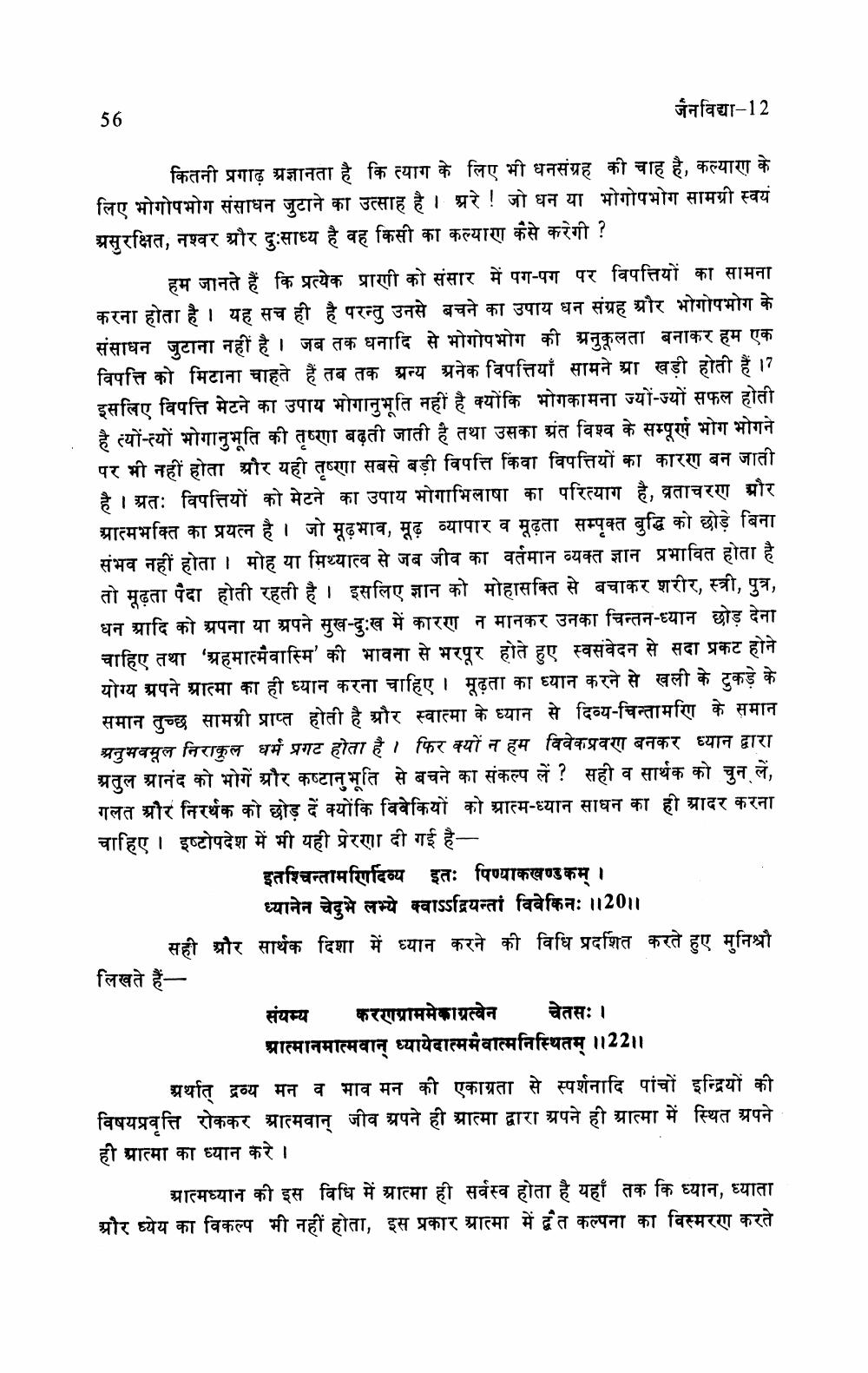________________
56
जनविद्या-12
कितनी प्रगाढ़ अज्ञानता है कि त्याग के लिए भी धनसंग्रह की चाह है, कल्याण के लिए भोगोपभोग संसाधन जुटाने का उत्साह है। अरे ! जो धन या भोगोपभोग सामग्री स्वयं असुरक्षित, नश्वर और दुःसाध्य है वह किसी का कल्याण कैसे करेगी ?
हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी को संसार में पग-पग पर विपत्तियों का सामना करना होता है । यह सच ही है परन्तु उनसे बचने का उपाय धन संग्रह और भोगोपभोग के संसाधन जुटाना नहीं है। जब तक धनादि से भोगोपभोग की अनुकूलता बनाकर हम एक विपत्ति को मिटाना चाहते हैं तब तक अन्य अनेक विपत्तियाँ सामने आ खड़ी होती हैं ।। इसलिए विपत्ति मेटने का उपाय भोगानुभूति नहीं है क्योंकि भोगकामना ज्यों-ज्यों सफल होती है त्यों-त्यों भोगानुभूति की तृष्णा बढ़ती जाती है तथा उसका अंत विश्व के सम्पूर्ण भोग भोगने पर भी नहीं होता और यही तृष्णा सबसे बड़ी विपत्ति किंवा विपत्तियों का कारण बन जाती है । अतः विपत्तियों को मेटने का उपाय भोगाभिलाषा का परित्याग है, व्रताचरण और आत्मभक्ति का प्रयत्न है। जो मूढ़भाव, मूढ़ व्यापार व मूढ़ता सम्पृक्त बुद्धि को छोड़े बिना संभव नहीं होता। मोह या मिथ्यात्व से जब जीव का वर्तमान व्यक्त ज्ञान प्रभावित होता है तो मूढ़ता पैदा होती रहती है। इसलिए ज्ञान को मोहासक्ति से बचाकर शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि को अपना या अपने सुख-दुःख में कारण न मानकर उनका चिन्तन-ध्यान छोड़ देना चाहिए तथा 'अहमात्मैवास्मि' की भावना से भरपूर होते हुए स्वसंवेदन से सदा प्रकट होने योग्य अपने प्रात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। मूढ़ता का ध्यान करने से खली के टुकड़े के समान तुच्छ सामग्री प्राप्त होती है और स्वात्मा के ध्यान से दिव्य-चिन्तामणि के समान अनुभवमूल निराकुल धर्म प्रगट होता है। फिर क्यों न हम विवेकप्रवरण बनकर ध्यान द्वारा अतुल आनंद को भोगें और कष्टानुभूति से बचने का संकल्प लें ? सही व सार्थक को चुन लें, गलत और निरर्थक को छोड़ दें क्योंकि विवेकियों को प्रात्म-ध्यान साधन का ही आदर करना चाहिए। इष्टोपदेश में भी यही प्रेरणा दी गई है
इतश्चिन्तामणिदिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ।
ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाऽऽद्रियन्तां विवेकिनः ॥20॥ सही और सार्थक दिशा में ध्यान करने की विधि प्रदर्शित करते हुए मुनिश्री लिखते हैं
संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः ।
प्रात्मानमात्मवान् ध्यायेदात्ममैवात्मनिस्थितम् ॥22॥ अर्थात् द्रव्य मन व भाव मन की एकाग्रता से स्पर्शनादि पांचों इन्द्रियों की विषयप्रवृत्ति रोककर आत्मवान् जीव अपने ही आत्मा द्वारा अपने ही आत्मा में स्थित अपने ही प्रात्मा का ध्यान करे।
आत्मध्यान की इस विधि में आत्मा ही सर्वस्व होता है यहाँ तक कि ध्यान, ध्याता और ध्येय का विकल्प भी नहीं होता, इस प्रकार आत्मा में द्वैत कल्पना का विस्मरण करते