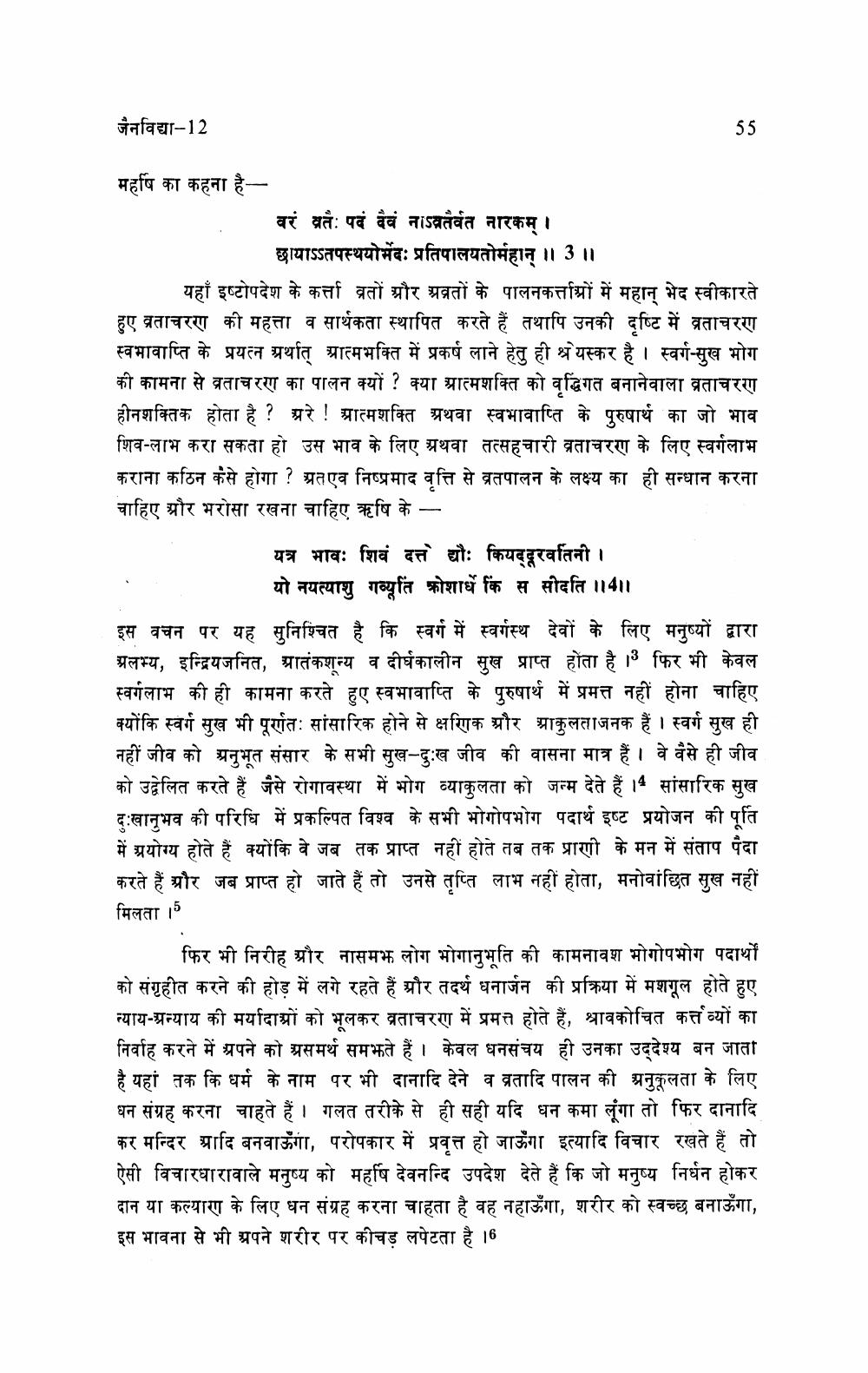________________
जैनविद्या-12
55
महर्षि का कहना है
वरं व्रतैः पदं दैवं नाऽवतैर्वत नारकम् ।
छायाऽऽतपस्थयोर्मेदः प्रतिपालयतोमहान् ॥ 3 ॥ यहाँ इष्टोपदेश के कर्ता व्रतों और अव्रतों के पालनकर्तालों में महान् भेद स्वीकारते हुए व्रताचरण की महत्ता व सार्थकता स्थापित करते हैं तथापि उनकी दृष्टि में व्रताचरण स्वभावाप्ति के प्रयत्न अर्थात् प्रात्मभक्ति में प्रकर्ष लाने हेतु ही श्रेयस्कर है । स्वर्ग-सुख भोग की कामना से व्रताचरण का पालन क्यों ? क्या आत्मशक्ति को वृद्धिंगत बनानेवाला व्रताचरण हीनशक्तिक होता है ? अरे ! आत्मशक्ति अथवा स्वभावाप्ति के पुरुषार्थ का जो भाव शिव-लाभ करा सकता हो उस भाव के लिए अथवा तत्सहचारी व्रताचरण के लिए स्वर्गलाभ कराना कठिन कैसे होगा ? अतएव निष्प्रमाद वृत्ति से व्रतपालन के लक्ष्य का ही सन्धान करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए ऋषि के -
यत्र भावः शिवं दत्त द्यौः कियदूरवतिनी ।
यो नयत्याशु गव्यूति क्रोशार्धे किं स सीदति ॥4॥ इस वचन पर यह सुनिश्चित है कि स्वर्ग में स्वर्गस्थ देवों के लिए मनुष्यों द्वारा अलभ्य, इन्द्रियजनित, आतंकशून्य व दीर्घकालीन सुख प्राप्त होता है । फिर भी केवल स्वर्गलाभ की ही कामना करते हुए स्वभावाप्ति के पुरुषार्थ में प्रमत्त नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वर्ग सुख भी पूर्णतः सांसारिक होने से क्षणिक और प्राकुलताजनक हैं । स्वर्ग सुख ही नहीं जीव को अनुभूत संसार के सभी सुख-दुःख जीव की वासना मात्र हैं। वे वैसे ही जीव को उद्वेलित करते हैं जैसे रोगावस्था में भोग व्याकुलता को जन्म देते हैं । सांसारिक सुख दुःखानुभव की परिधि में प्रकल्पित विश्व के सभी भोगोपभोग पदार्थ इष्ट प्रयोजन की पूर्ति में अयोग्य होते हैं क्योंकि वे जब तक प्राप्त नहीं होते तब तक प्राणी के मन में संताप पैदा करते हैं और जब प्राप्त हो जाते हैं तो उनसे तृप्ति लाभ नहीं होता, मनोवांछित सुख नहीं मिलता।
फिर भी निरीह और नासमझ लोग भोगानुभूति की कामनावश भोगोपभोग पदार्थों को संगृहीत करने की होड़ में लगे रहते हैं और तदर्थ धनार्जन की प्रक्रिया में मशगूल होते हुए न्याय-अन्याय की मर्यादाओं को भूलकर व्रताचरण में प्रमत्त होते हैं, श्रावकोचित कर्तव्यों का निर्वाह करने में अपने को असमर्थ समझते हैं। केवल धनसंचय ही उनका उद्देश्य बन जाता है यहां तक कि धर्म के नाम पर भी दानादि देने व व्रतादि पालन की अनुकूलता के लिए धन संग्रह करना चाहते हैं । गलत तरीके से ही सही यदि धन कमा लूंगा तो फिर दानादि कर मन्दिर आदि बनवाऊँगा, परोपकार में प्रवृत्त हो जाऊँगा इत्यादि विचार रखते हैं तो ऐसी विचारधारावाले मनुष्य को महर्षि देवनन्दि उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य निर्धन होकर दान या कल्याण के लिए धन संग्रह करना चाहता है वह नहाऊँगा, शरीर को स्वच्छ बनाऊँगा, इस भावना से भी अपने शरीर पर कीचड़ लपेटता है ।।