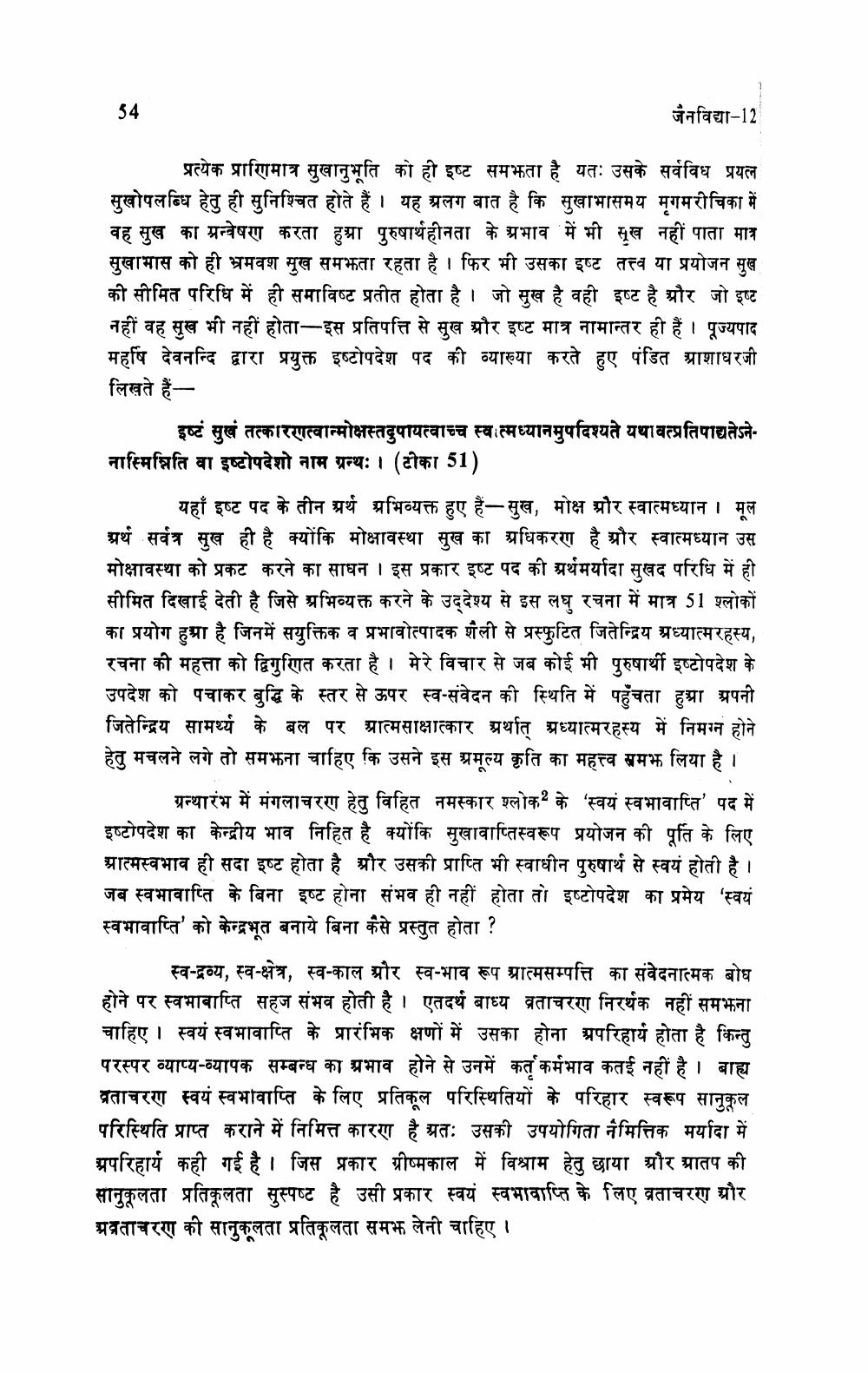________________
जनविद्या-12
प्रत्येक प्राणिमात्र सुखानुभूति को ही इष्ट समझता है यतः उसके सर्वविध प्रयत्न सुखोपलब्धि हेतु ही सुनिश्चित होते हैं । यह अलग बात है कि सुखाभासमय मृगमरीचिका में वह सुख का अन्वेषण करता हुआ पुरुषार्थहीनता के अभाव में भी सुख नहीं पाता मात्र सुखाभास को ही भ्रमवश मुख समझता रहता है । फिर भी उसका इष्ट तत्त्व या प्रयोजन सुख की सीमित परिधि में ही समाविष्ट प्रतीत होता है। जो सुख है वही इष्ट है और जो इष्ट नहीं वह सुख भी नहीं होता-इस प्रतिपत्ति से सुख और इष्ट मात्र नामान्तर ही हैं । पूज्यपाद महर्षि देवनन्दि द्वारा प्रयुक्त इष्टोपदेश पद की व्याख्या करते हुए पंडित अाशाधरजी लिखते हैं
इष्टं सुखं तत्कारणत्वान्मोक्षस्तदुपायत्वाच्च स्वात्मध्यानमुपदिश्यते यथावत्प्रतिपाद्यतेऽनेनास्मिन्निति वा इष्टोपदेशो नाम ग्रन्थः । (टीका 51)
___ यहाँ इष्ट पद के तीन अर्थ अभिव्यक्त हुए हैं-सुख, मोक्ष और स्वात्मध्यान । मूल अर्थ सर्वत्र सुख ही है क्योंकि मोक्षावस्था सुख का अधिकरण है और स्वात्मध्यान उस मोक्षावस्था को प्रकट करने का साधन । इस प्रकार इष्ट पद की अर्थमर्यादा सुखद परिधि में ही सीमित दिखाई देती है जिसे अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से इस लघु रचना में मात्र 51 श्लोकों का प्रयोग हुअा है जिनमें सयुक्तिक व प्रभावोत्पादक शैली से प्रस्फुटित जितेन्द्रिय अध्यात्मरहस्य, रचना की महत्ता को द्विगुणित करता है। मेरे विचार से जब कोई भी पुरुषार्थी इष्टोपदेश के उपदेश को पचाकर बुद्धि के स्तर से ऊपर स्व-संवेदन की स्थिति में पहुँचता हुआ अपनी जितेन्द्रिय सामर्थ्य के बल पर आत्मसाक्षात्कार अर्थात् अध्यात्मरहस्य में निमग्न होने हेतु मचलने लगे तो समझना चाहिए कि उसने इस अमूल्य कृति का महत्त्व समझ लिया है ।
ग्रन्थारंभ में मंगलाचरण हेतु विहित नमस्कार श्लोक के 'स्वयं स्वभावाप्ति' पद में इष्टोपदेश का केन्द्रीय भाव निहित है क्योंकि सुखावाप्तिस्वरूप प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रात्मस्वभाव ही सदा इष्ट होता है और उसकी प्राप्ति भी स्वाधीन पुरुषार्थ से स्वयं होती है । जब स्वभावाप्ति के बिना इष्ट होना संभव ही नहीं होता तो इष्टोपदेश का प्रमेय 'स्वयं स्वभावाप्ति' को केन्द्रभूत बनाये बिना कैसे प्रस्तुत होता ?
स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और स्व-भाव रूप आत्मसम्पत्ति का संवेदनात्मक बोध होने पर स्वभावाप्ति सहज संभव होती है । एतदर्थ बाध्य व्रताचरण निरर्थक नहीं समझना चाहिए। स्वयं स्वभावाप्ति के प्रारंभिक क्षणों में उसका होना अपरिहार्य होता है किन्तु परस्पर व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध का अभाव होने से उनमें कर्तृ कर्मभाव कतई नहीं है । बाह्य व्रताचरण स्वयं स्वभावाप्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के परिहार स्वरूप सानुकूल परिस्थिति प्राप्त कराने में निमित्त कारण है अतः उसकी उपयोगिता नैमित्तिक मर्यादा में अपरिहार्य कही गई है। जिस प्रकार ग्रीष्मकाल में विश्राम हेतु छाया और आतप की सानुकूलता प्रतिकूलता सुस्पष्ट है उसी प्रकार स्वयं स्वभावाप्ति के लिए व्रताचरण और अव्रताचरण की सानुकूलता प्रतिकूलता समझ लेनी चाहिए ।