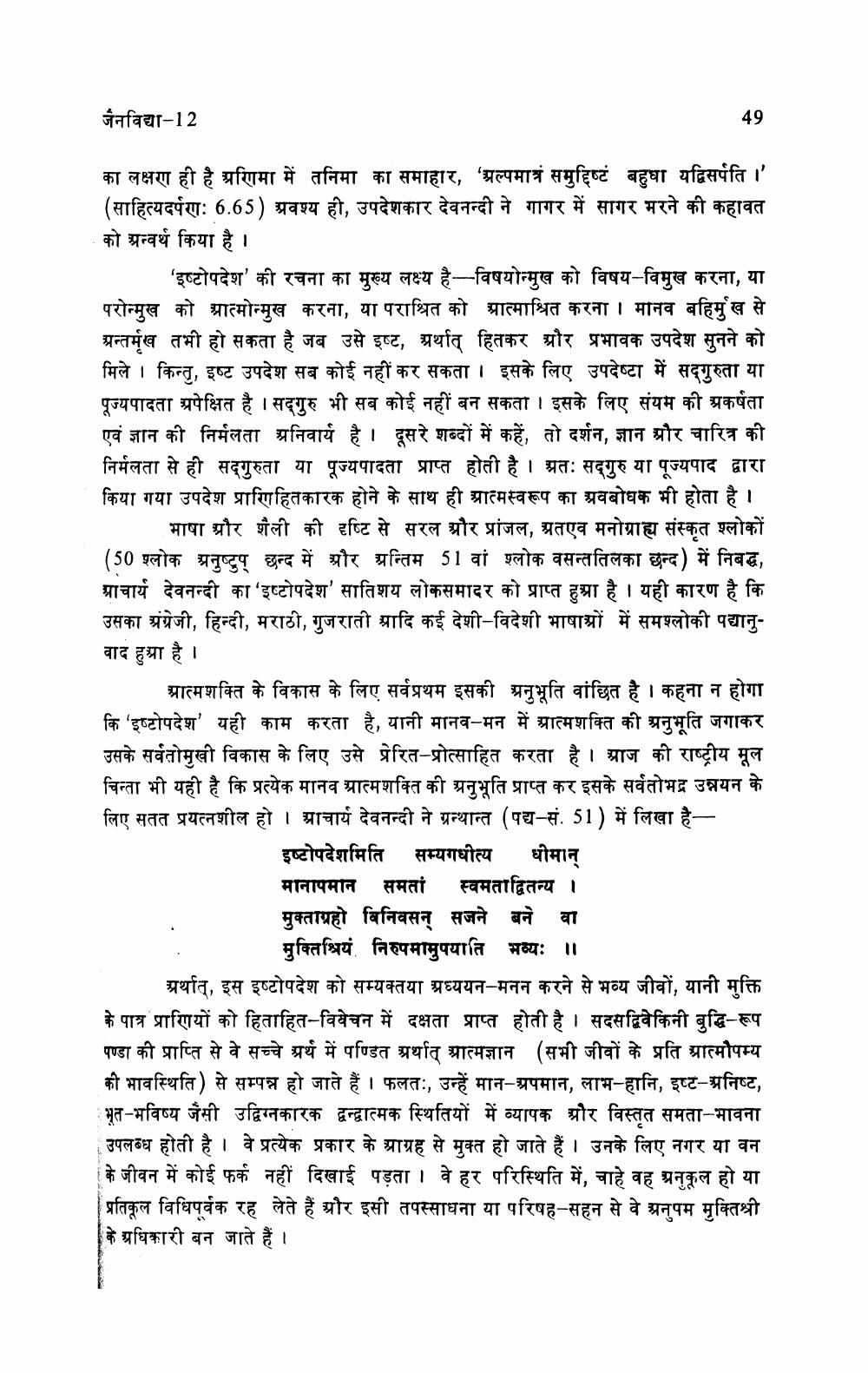________________
जनविद्या-12
49
का लक्षण ही है अणिमा में तनिमा का समाहार, 'अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसर्पति ।' (साहित्यदर्पणः 6.65) अवश्य ही, उपदेशकार देवनन्दी ने गागर में सागर भरने की कहावत को अन्वर्थ किया है।
'इष्टोपदेश' की रचना का मुख्य लक्ष्य है-विषयोन्मुख को विषय-विमुख करना, या परोन्मुख को आत्मोन्मुख करना, या पराश्रित को प्रात्माश्रित करना । मानव बहिर्मुख से अन्तर्मुख तभी हो सकता है जब उसे इष्ट, अर्थात् हितकर और प्रभावक उपदेश सुनने को मिले । किन्तु, इष्ट उपदेश सब कोई नहीं कर सकता। इसके लिए उपदेष्टा में सद्गुरुता या पूज्यपादता अपेक्षित है । सद्गुरु भी सब कोई नहीं बन सकता । इसके लिए संयम की अकर्षता एवं ज्ञान की निर्मलता अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कहें, तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र की निर्मलता से ही सद्गुरुता या पूज्यपादता प्राप्त होती है । अतः सद्गुरु या पूज्यपाद द्वारा किया गया उपदेश प्राणिहितकारक होने के साथ ही प्रात्मस्वरूप का अवबोधक भी होता है ।
भाषा और शैली की दृष्टि से सरल और प्रांजल, अतएव मनोग्राह्य संस्कृत श्लोकों (50 श्लोक अनुष्टुप् छन्द में और अन्तिम 51 वां श्लोक वसन्ततिलका छन्द) में निबद्ध, प्राचार्य देवनन्दी का 'इष्टोपदेश' सातिशय लोकसमादर को प्राप्त हुआ है । यही कारण है कि उसका अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि कई देशी-विदेशी भाषाओं में समश्लोकी पद्यानुवाद हुआ है।
आत्मशक्ति के विकास के लिए सर्वप्रथम इसकी अनुभूति वांछित है । कहना न होगा कि 'इष्टोपदेश' यही काम करता है, यानी मानव-मन में प्रात्मशक्ति की अनुभूति जगाकर उसके सर्वतोमुखी विकास के लिए उसे प्रेरित-प्रोत्साहित करता है। आज की राष्ट्रीय मूल चिन्ता भी यही है कि प्रत्येक मानव प्रात्मशक्ति की अनुभूति प्राप्त कर इसके सर्वतोभद्र उन्नयन के लिए सतत प्रयत्नशील हो । आचार्य देवनन्दी ने ग्रन्थान्त (पद्य-सं. 51 ) में लिखा है
इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य । मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने बने वा
मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः ॥ अर्थात्, इस इष्टोपदेश को सम्यक्तया अध्ययन-मनन करने से भव्य जीवों, यानी मुक्ति के पात्र प्राणियों को हिताहित-विवेचन में दक्षता प्राप्त होती है । सदसद्विवेकिनी बुद्धि-रूप पण्डा की प्राप्ति से वे सच्चे अर्थ में पण्डित अर्थात् आत्मज्ञान (सभी जीवों के प्रति आत्मौपम्य की भावस्थिति) से सम्पन्न हो जाते हैं । फलतः, उन्हें मान-अपमान, लाभ-हानि, इष्ट-अनिष्ट, भूत-भविष्य जैसी उद्विग्नकारक द्वन्द्वात्मक स्थितियों में व्यापक और विस्तृत समता-भावना उपलब्ध होती है। वे प्रत्येक प्रकार के प्राग्रह से मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए नगर या वन के जीवन में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। वे हर परिस्थिति में, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल विधिपूर्वक रह लेते हैं और इसी तपस्साधना या परिषह-सहन से वे अनुपम मुक्तिश्री के अधिकारी बन जाते हैं।