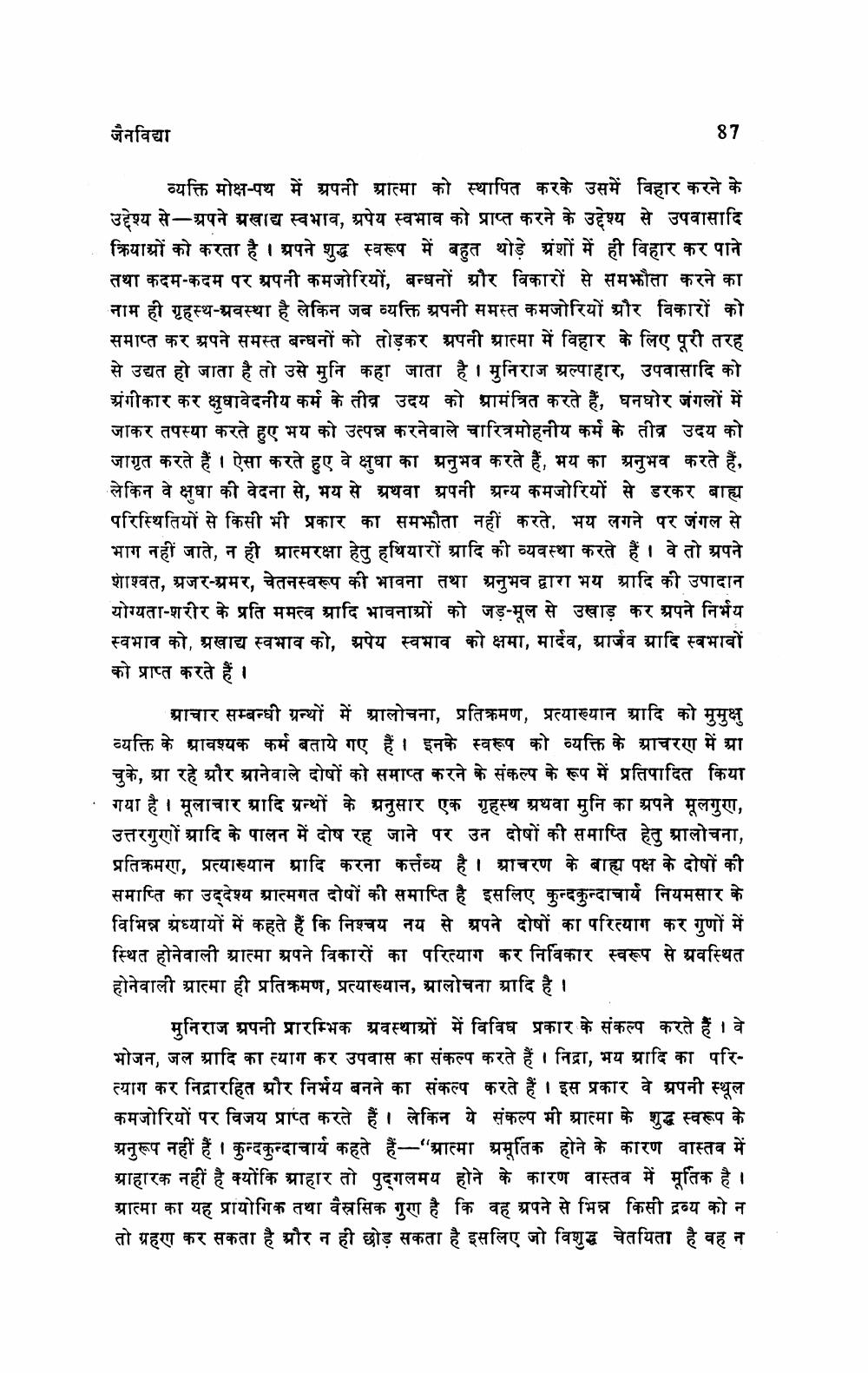________________
जैनविद्या
87
व्यक्ति मोक्ष-पथ में अपनी आत्मा को स्थापित करके उसमें विहार करने के उद्देश्य से - अपने अखाद्य स्वभाव, अपेय स्वभाव को प्राप्त करने के उद्देश्य उपवासादि क्रियाओं को करता है । अपने शुद्ध स्वरूप में बहुत थोड़े अंशों में ही विहार कर पाने तथा कदम-कदम पर अपनी कमजोरियों, बन्धनों और विकारों से समझौता करने का नाम ही गृहस्थ अवस्था है लेकिन जब व्यक्ति अपनी समस्त कमजोरियों और विकारों को समाप्त कर अपने समस्त बन्धनों को तोड़कर अपनी प्रात्मा में विहार के लिए पूरी तरह से उद्यत हो जाता है तो उसे मुनि कहा जाता है । मुनिराज अल्पाहार उपवासादि को अंगीकार कर क्षुधावेदनीय कर्म के तीव्र उदय को श्रामंत्रित करते हैं, घनघोर जंगलों में जाकर तपस्या करते हुए भय को उत्पन्न करनेवाले चारित्रमोहनीय कर्म के तीव्र उदय को जागृत करते हैं । ऐसा करते हुए वे क्षुधा का अनुभव करते हैं, भय का अनुभव करते हैं, लेकिन वे क्षुधा की वेदना से, भय से अथवा अपनी अन्य कमजोरियों से डरकर बाह्य परिस्थितियों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते, भय लगने पर जंगल से भाग नहीं जाते, न ही प्रात्मरक्षा हेतु हथियारों आदि की व्यवस्था करते हैं । वे तो अपने शाश्वत, अजर-अमर, चेतनस्वरूप की भावना तथा अनुभव द्वारा भय आदि की उपादान योग्यता - शरीर के प्रति ममत्व आदि भावनाओं को जड़ मूल से उखाड़ कर अपने निर्भय स्वभाव को खाद्य स्वभाव को अपेय स्वभाव को क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि स्वभावों को प्राप्त करते हैं ।
प्राचार सम्बन्धी ग्रन्थों में प्रालोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि को मुमुक्षु व्यक्ति के श्रावश्यक कर्म बताये गए हैं । इनके स्वरूप को व्यक्ति के आचरण में आ चुके, आ रहे और आनेवाले दोषों को समाप्त करने के संकल्प के रूप में प्रतिपादित किया गया है । मूलाचार आदि ग्रन्थों के अनुसार एक गृहस्थ अथवा मुनि का अपने मूलगुण, उत्तरगुणों आदि के पालन में दोष रह जाने पर उन दोषों की समाप्ति हेतु श्रालोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान श्रादि करना कर्त्तव्य है । आचरण के बाह्य पक्ष के दोषों की समाप्ति का उद्देश्य ग्रात्मगत दोषों की समाप्ति है इसलिए कुन्दकुन्दाचार्य नियमसार के विभिन्न अध्यायों में कहते हैं कि निश्चय नय से अपने दोषों का परित्याग कर गुणों में स्थित होनेवाली आत्मा अपने विकारों का परित्याग कर निर्विकार स्वरूप से प्रवस्थित होनेवाली आत्मा ही प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि है ।
मुनिराज अपनी प्रारम्भिक अवस्थाओं में विविध प्रकार के संकल्प करते हैं । वे भोजन, जल आदि का त्याग कर उपवास का संकल्प करते हैं । निद्रा, भय आदि का परित्याग कर निद्रारहित और निर्भय बनने का संकल्प करते हैं । इस प्रकार वे अपनी स्थूल कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं । लेकिन ये संकल्प भी आत्मा के शुद्ध स्वरूप के अनुरूप नहीं हैं । कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं- "आत्मा प्रमूर्तिक होने के कारण वास्तव में आहारक नहीं है क्योंकि आहार तो पुद्गलमय होने के कारण वास्तव में मूर्तिक है । आत्मा का यह प्रायोगिक तथा वैस्रसिक गुण है कि वह अपने से भिन्न तो ग्रहण कर सकता है और न ही छोड़ सकता है इसलिए जो विशुद्ध
किसी द्रव्य को न चेतयिता है वह न