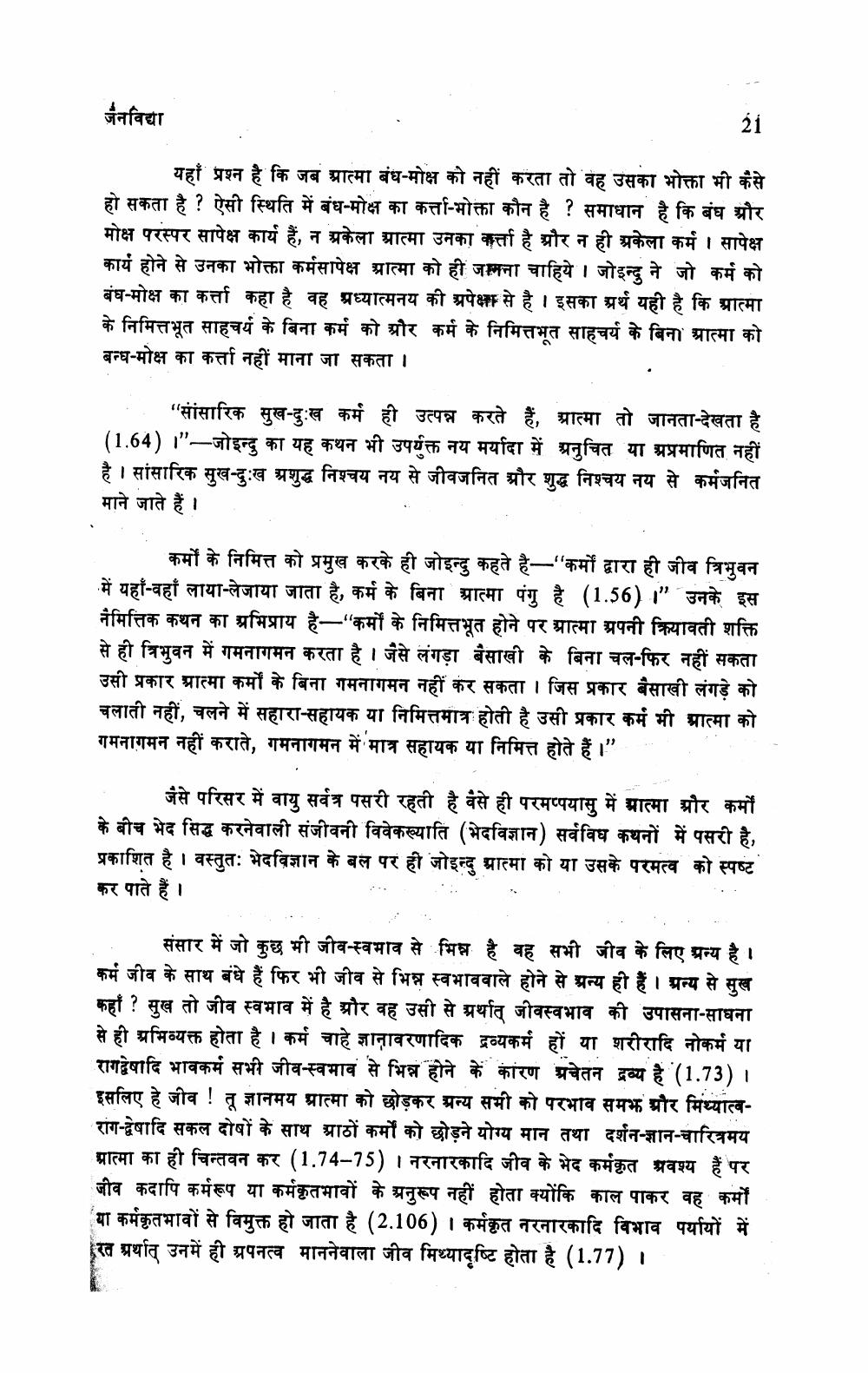________________
जनविद्या
यहाँ प्रश्न है कि जब आत्मा बंध-मोक्ष को नहीं करता तो वह उसका भोक्ता भी कैसे हो सकता है ? ऐसी स्थिति में बंध-मोक्ष का कर्ता-भोक्ता कौन है ? समाधान है कि बंध और मोक्ष परस्पर सापेक्ष कार्य हैं, न अकेला आत्मा उनका कर्ता है और न ही अकेला कर्म । सापेक्ष कार्य होने से उनका भोक्ता कर्मसापेक्ष आत्मा को ही जामना चाहिये । जोइन्दु ने जो कर्म को बंध-मोक्ष का कर्ता कहा है वह अध्यात्मनय की अपेक्षा से है । इसका अर्थ यही है कि प्रात्मा के निमित्तभूत साहचर्य के बिना कर्म को और कर्म के निमित्तभूत साहचर्य के बिना आत्मा को बन्ध-मोक्ष का कर्ता नहीं माना जा सकता।
___ "सांसारिक सुख-दुःख कर्म ही उत्पन्न करते हैं, आत्मा तो जानता-देखता है (1.64)।"-जोइन्दु का यह कथन भी उपर्युक्त नय मर्यादा में अनुचित या अप्रमाणित नहीं है । सांसारिक सुख-दुःख अशुद्ध निश्चय नय से जीवजनित और शुद्ध निश्चय नय से कर्मजनित माने जाते हैं।
कर्मों के निमित्त को प्रमुख करके ही जोइन्दु कहते है-“कर्मों द्वारा ही जीव त्रिभुवन में यहाँ-वहाँ लाया-लेजाया जाता है, कर्म के बिना आत्मा पंगु है (1.56)।" उनके इस नैमित्तिक कथन का अभिप्राय है-“कर्मों के निमित्तभूत होने पर प्रात्मा अपनी क्रियावती शक्ति से ही त्रिभुवन में गमनागमन करता है । जैसे लंगड़ा बैसाखी के बिना चल-फिर नहीं सकता उसी प्रकार प्रात्मा कर्मों के बिना गमनागमन नहीं कर सकता । जिस प्रकार बैसाखी लंगड़े को चलाती नहीं, चलने में सहारा-सहायक या निमित्तमात्र होती है उसी प्रकार कर्म भी प्रात्मा को गमनागमन नहीं कराते, गमनागमन में मात्र सहायक या निमित्त होते हैं।"
जैसे परिसर में वायु सर्वत्र पसरी रहती है वैसे ही परमप्पयासु में आत्मा और कर्मों के बीच भेद सिद्ध करनेवाली संजीवनी विवेकख्याति (भेदविज्ञान) सर्वविध कथनों में पसरी है, प्रकाशित है । वस्तुतः भेदविज्ञान के बल पर ही जोइन्दु प्रात्मा को या उसके परमत्व को स्पष्ट कर पाते हैं।
__संसार में जो कुछ भी जीव-स्वभाव से भिन्न है वह सभी जीव के लिए अन्य है। कर्म जीव के साथ बंधे हैं फिर भी जीव से भिन्न स्वभाववाले होने से अन्य ही हैं । अन्य से सुख कहाँ ? सुख तो जीव स्वभाव में है और वह उसी से अर्थात् जीवस्वभाव की उपासना-साधना से ही अभिव्यक्त होता है । कर्म चाहे ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्म हों या शरीरादि नोकर्म या रागद्वेषादि भावकर्म सभी जीव-स्वभाव से भिन्न होने के कारण अचेतन द्रव्य है (1.73) । इसलिए हे जीव ! तू ज्ञानमय प्रात्मा को छोड़कर अन्य सभी को परभाव समझ और मिथ्यात्वराग-द्वेषादि सकल दोषों के साथ आठों कर्मों को छोड़ने योग्य मान तथा दर्शन-ज्ञान-चारित्रमय मात्मा का ही चिन्तवन कर (1.74-75) । नरनारकादि जीव के भेद कर्मकृत अवश्य हैं पर जीव कदापि कर्मरूप या कर्मकृतभावों के अनुरूप नहीं होता क्योंकि काल पाकर वह कर्मों या कर्मकृतभावों से विमुक्त हो जाता है (2.106) । कर्मकृत नरनारकादि विभाव पर्यायों में रत अर्थात् उनमें ही अपनत्व माननेवाला जीव मिथ्यादृष्टि होता है (1.77) ।