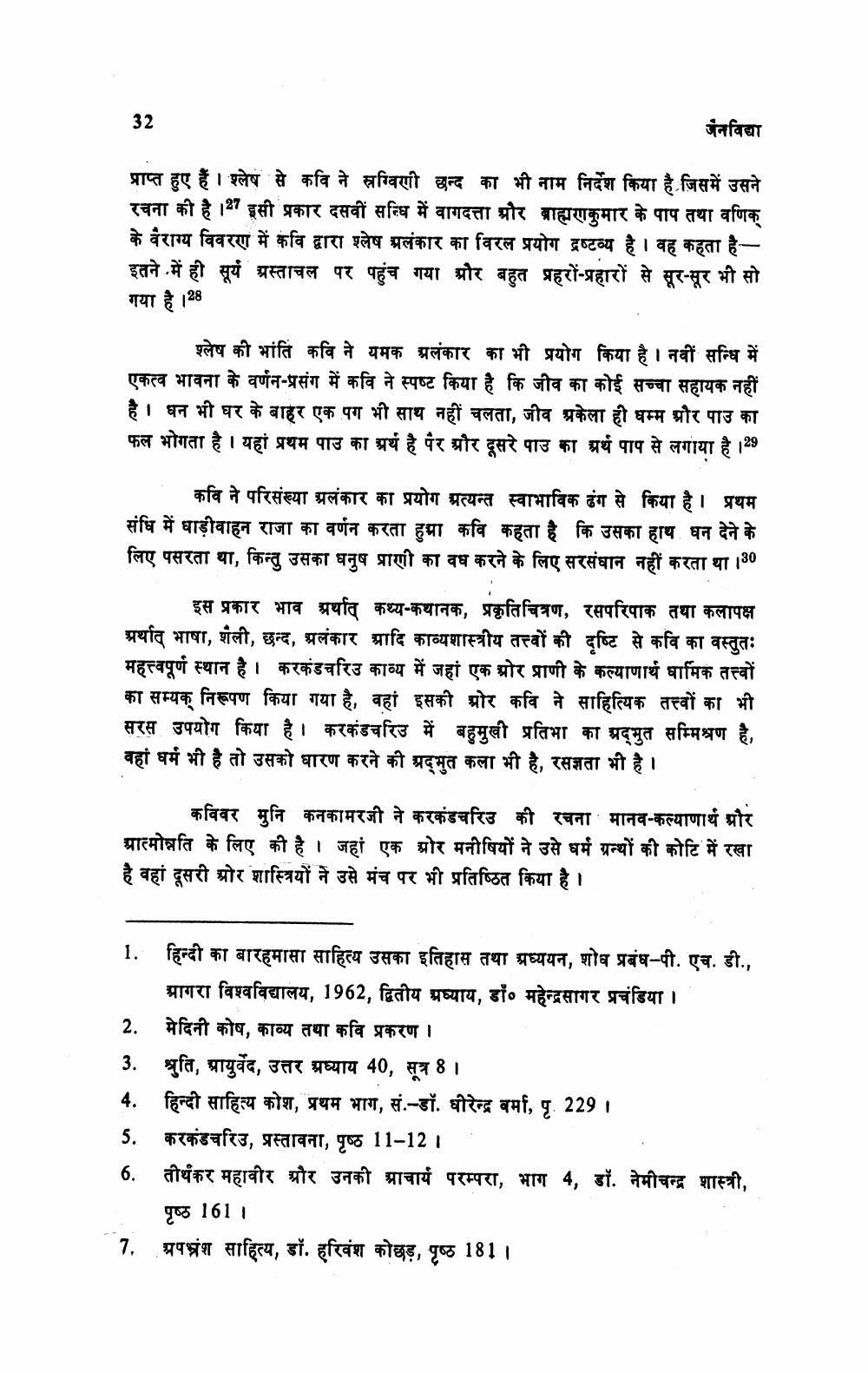________________
32
जनविद्या
प्राप्त हुए हैं । श्लेष से कवि ने स्रग्विणी छन्द का भी नाम निर्देश किया है जिसमें उसने रचना की है। इसी प्रकार दसवीं सन्धि में वागदत्ता और ब्राह्मणकुमार के पाप तथा वणिक् के वैराग्य विवरण में कवि द्वारा श्लेष अलंकार का विरल प्रयोग द्रष्टव्य है । वह कहता हैइतने में ही सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गया और बहुत प्रहरों-प्रहारों से सूर-सूर भी सो गया है ।28
श्लेष की भांति कवि ने यमक अलंकार का भी प्रयोग किया है । नवीं सन्धि में एकत्व भावना के वर्णन-प्रसंग में कवि ने स्पष्ट किया है कि जीव का कोई सच्चा सहायक नहीं है। धन भी घर के बाहर एक पग भी साथ नहीं चलता, जीव अकेला ही धम्म और पाउ का फल भोगता है । यहां प्रथम पाउ का अर्थ है पर और दूसरे पाउ का अर्थ पाप से लगाया है ।29
कवि ने परिसंख्या अलंकार का प्रयोग अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से किया है। प्रथम संधि में धाड़ीवाहन राजा का वर्णन करता हुमा कवि कहता है कि उसका हाथ धन देने के लिए पसरता था, किन्तु उसका धनुष प्राणी का वध करने के लिए सरसंधान नहीं करता था।30
इस प्रकार भाव अर्थात् कथ्य-कथानक, प्रकृतिचित्रण, रसपरिपाक तथा कलापक्ष अर्थात् भाषा, शैली, छन्द, अलंकार आदि काव्यशास्त्रीय तत्त्वों की दृष्टि से कवि का वस्तुतः महत्त्वपूर्ण स्थान है। करकंडचरिउ काव्य में जहां एक ओर प्राणी के कल्याणार्थ धार्मिक तत्त्वों का सम्यक निरूपण किया गया है, वहां इसकी अोर कवि ने साहित्यिक तत्त्वों का भी सरस उपयोग किया है। करकंडचरिउ में बहुमुखी प्रतिभा का अद्भुत सम्मिश्रण है, वहां धर्म भी है तो उसको धारण करने की अद्भुत कला भी है, रसज्ञता भी है ।
कविवर मुनि कनकामरजी ने करकंडचरिउ की रचना मानव-कल्याणार्थ और आत्मोन्नति के लिए की है । जहां एक ओर मनीषियों ने उसे धर्म ग्रन्थों की कोटि में रखा है वहां दूसरी ओर शास्त्रियों ने उसे मंच पर भी प्रतिष्ठित किया है।
1. हिन्दी का बारहमासा साहित्य उसका इतिहास तथा अध्ययन, शोध प्रबंध-पी. एच. डी.,
आगरा विश्वविद्यालय, 1962, द्वितीय अध्याय, डॉ. महेन्द्रसागर प्रचंडिया। 2. मेदिनी कोष, काव्य तथा कवि प्रकरण । 3. श्रुति, आयुर्वेद, उत्तर अध्याय 40, सूत्र 8 । 4. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, सं.-डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, पृ. 229 । 5. करकंडचरिउ, प्रस्तावना, पृष्ठ 11-12 । 6. तीर्थंकर महावीर और उनकी प्राचार्य परम्परा, भाग 4, डॉ. नेमीचन्द्र शास्त्री,
पृष्ठ 161 । 7, अपभ्रंश साहित्य, डॉ. हरिवंश कोछड़, पृष्ठ 181 ।