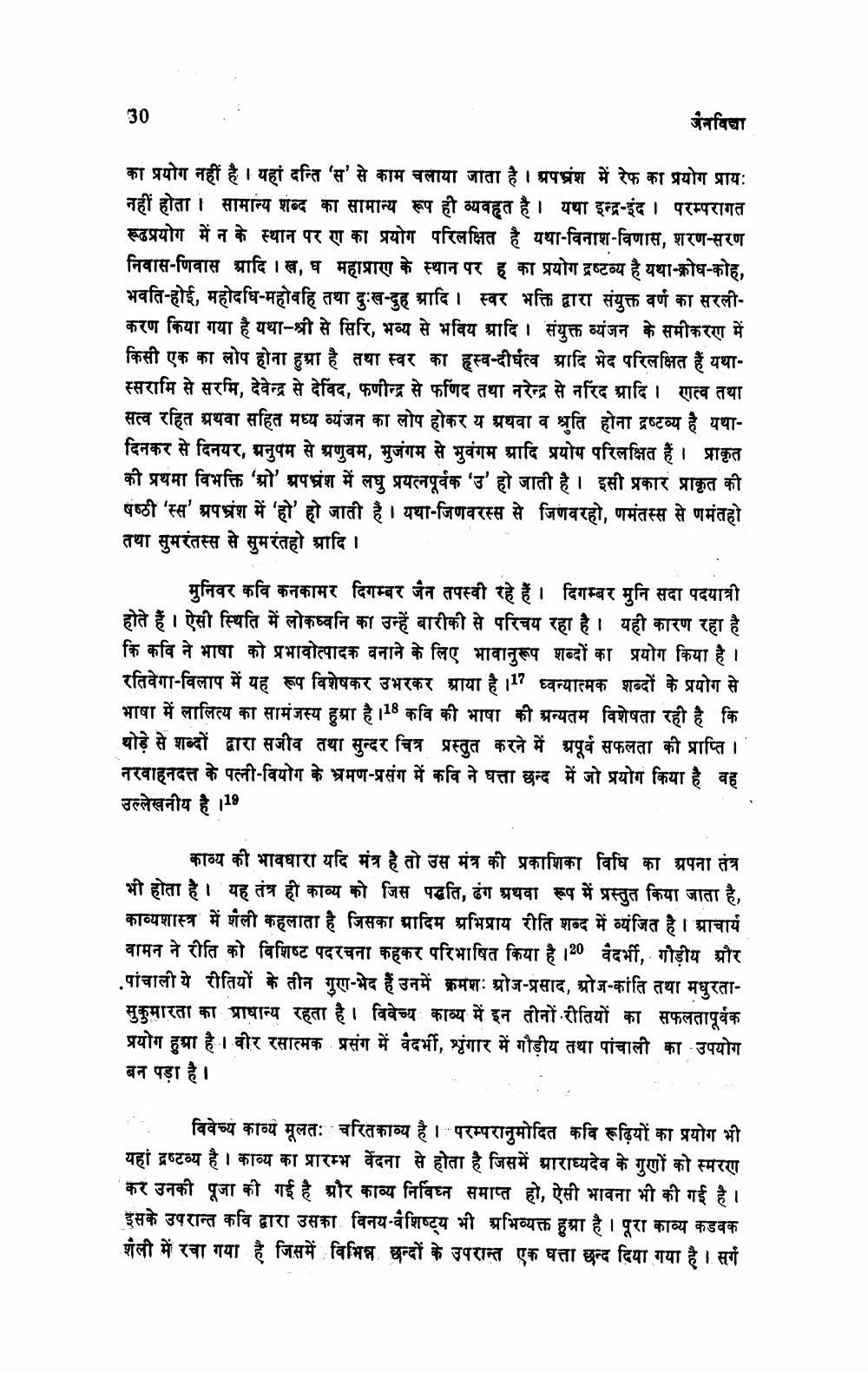________________
30
जनविधा
का प्रयोग नहीं है । यहां दन्ति 'स' से काम चलाया जाता है । अपभ्रंश में रेफ का प्रयोग प्राय: नहीं होता। सामान्य शब्द का सामान्य रूप ही व्यवहृत है। यथा इन्द्र-इंद। परम्परागत रूढप्रयोग में न के स्थान पर ण का प्रयोग परिलक्षित है यथा-विनाश-विणास, शरण-सरण निवास-णिवास आदि । ख, घ महाप्राण के स्थान पर ह का प्रयोग द्रष्टव्य है यथा-क्रोध-कोह, भवति-होई, महोदधि-महोवहि तथा दुःख-दुह आदि। स्वर भक्ति द्वारा संयुक्त वर्ण का सरलीकरण किया गया है यथा-श्री से सिरि, भव्य से भविय आदि । संयुक्त व्यंजन के समीकरण में किसी एक का लोप होना हुआ है तथा स्वर का हस्व-दीर्घत्व आदि भेद परिलक्षित हैं यथास्सरामि से सरमि, देवेन्द्र से देविंद, फणीन्द्र से फणिद तथा नरेन्द्र से नरिंद आदि । णत्व तथा सत्व रहित अथवा सहित मध्य व्यंजन का लोप होकर य अथवा व श्रुति होना द्रष्टव्य है यथादिनकर से दिनयर, अनुपम से अणुवम, भुजंगम से भुवंगम आदि प्रयोग परिलक्षित हैं। प्राकृत की प्रथमा विभक्ति 'ओ' अपभ्रंश में लघु प्रयत्नपूर्वक 'उ' हो जाती है। इसी प्रकार प्राकृत की षष्ठी 'स्स' अपभ्रंश में 'हो' हो जाती है । यथा-जिणवरस्स से जिणवरहो, णमंतस्स से णमंतहो तथा सुमरंतस्स से सुमरंतहो आदि ।
मुनिवर कवि कनकामर दिगम्बर जैन तपस्वी रहे हैं। दिगम्बर मुनि सदा पदयात्री होते हैं । ऐसी स्थिति में लोकध्वनि का उन्हें बारीकी से परिचय रहा है। यही कारण रहा है कि कवि ने भाषा को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए भावानुरूप शब्दों का प्रयोग किया है । रतिवेगा-विलाप में यह रूप विशेषकर उभरकर आया है ।" ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग से भाषा में लालित्य का सामंजस्य हुआ है।18 कवि की भाषा की अन्यतम विशेषता रही है कि थोड़े से शब्दों द्वारा सजीव तथा सुन्दर चित्र प्रस्तुत करने में अपूर्व सफलता की प्राप्ति । नरवाहनदत्त के पत्नी-वियोग के भ्रमण-प्रसंग में कवि ने पत्ता छन्द में जो प्रयोग किया है वह उल्लेखनीय है ।19
___ काव्य की भावधारा यदि मंत्र है तो उस मंत्र को प्रकाशिका विधि का अपना तंत्र भी होता है। यह तंत्र ही काव्य को जिस पद्धति, ढंग अथवा रूप में प्रस्तुत किया जाता है, काव्यशास्त्र में शैली कहलाता है जिसका मादिम अभिप्राय रीति शब्द में व्यंजित है। प्राचार्य वामन ने रीति को विशिष्ट पदरचना कहकर परिभाषित किया है ।20 वैदर्भी, गौड़ीय और .पांचाली ये रीतियों के तीन गुण-भेद हैं उनमें क्रमशः प्रोज-प्रसाद, प्रोज-कांति तथा मधुरतासुकुमारता का प्राधान्य रहता है। विवेच्य काव्य में इन तीनों रीतियों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है । वीर रसात्मक प्रसंग में वैदर्भी, शृंगार में गौड़ीय तथा पांचाली का उपयोग बन पड़ा है।
विवेच्य काव्य मूलतः चरितकाव्य है। परम्परानुमोदित कवि रूढ़ियों का प्रयोग भी यहां द्रष्टव्य है । काव्य का प्रारम्भ वेदना से होता है जिसमें माराध्यदेव के गुणों को स्मरण कर उनकी पूजा की गई है और काव्य निर्विघ्न समाप्त हो, ऐसी भावना भी की गई है। इसके उपरान्त कवि द्वारा उसका विनय वैशिष्ट्य भी अभिव्यक्त हुआ है । पूरा काव्य कडवक शैली में रचा गया है जिसमें विभिन्न छन्दों के उपरान्त एक घत्ता छन्द दिया गया है। सर्ग