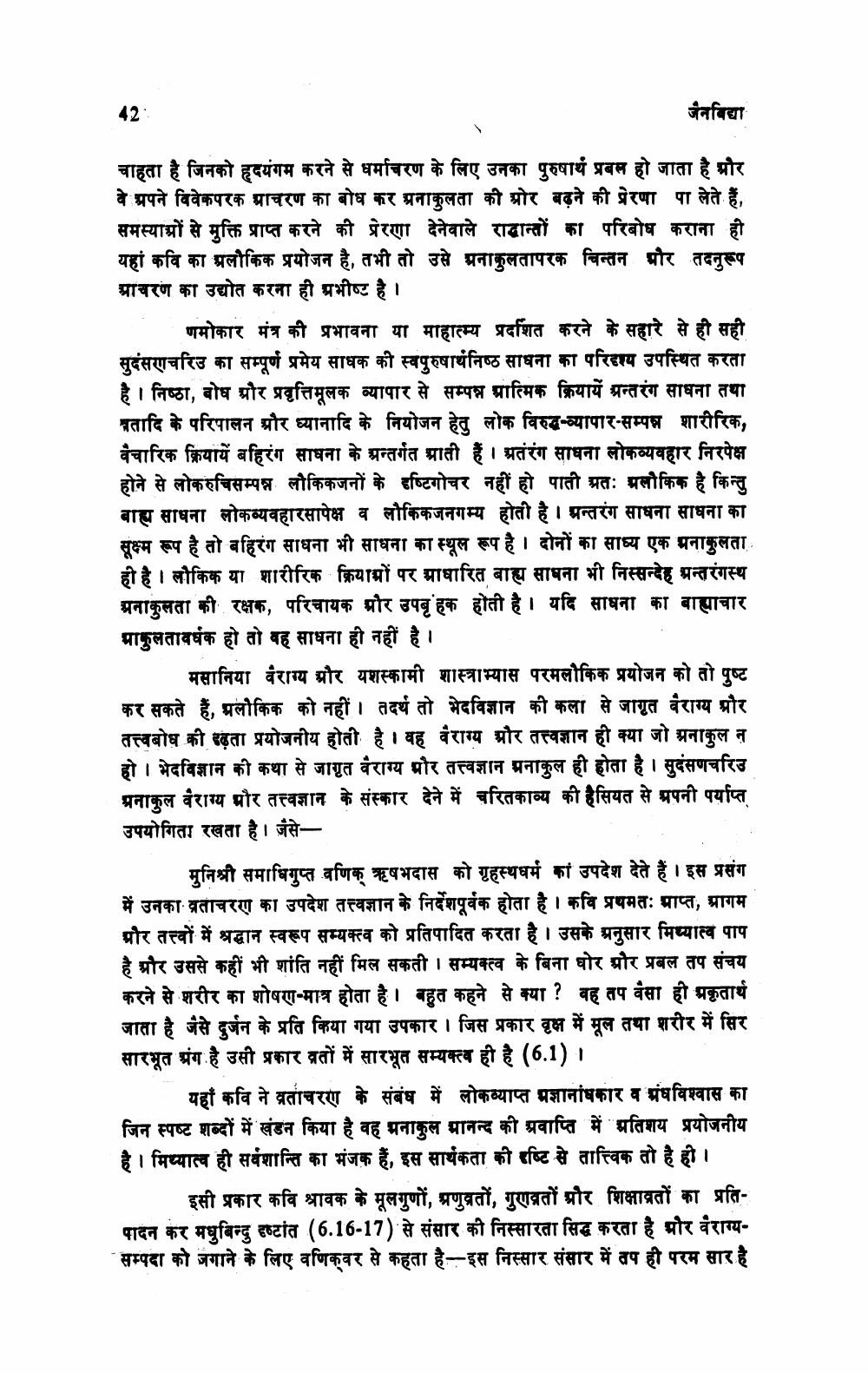________________
जनविद्या
चाहता है जिनको हृदयंगम करने से धर्माचरण के लिए उनका पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है और वे अपने विवेकपरक पाचरण का बोध कर अनाकुलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा पा लेते हैं, समस्यानों से मुक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देनेवाले राधान्तों का परिबोध कराना ही यहां कवि का अलौकिक प्रयोजन है, तभी तो उसे अनाकुलतापरक चिन्तन और तदनुरूप प्राचरण का उद्योत करना ही अभीष्ट है।
णमोकार मंत्र की प्रभावना या माहात्म्य प्रदर्शित करने के सहारे से ही सही सुदंसणचरिउ का सम्पूर्ण प्रमेय साधक की स्वपुरुषार्थनिष्ठ साधना का परिदृश्य उपस्थित करता है । निष्ठा, बोध और प्रवृत्तिमूलक व्यापार से सम्पन्न प्रात्मिक क्रियायें अन्तरंग साधना तथा वतादि के परिपालन और ध्यानादि के नियोजन हेतु लोक विरुद्ध-व्यापार-सम्पन्न शारीरिक, वैचारिक क्रियायें बहिरंग साधना के अन्तर्गत पाती हैं । अतंरंग साधना लोकव्यवहार निरपेक्ष होने से लोकरुचिसम्पन्न लौकिकजनों के दृष्टिगोचर नहीं हो पाती अतः प्रलौकिक है किन्तु बाह्य साधना लोकव्यवहारसापेक्ष व लौकिकजनगम्य होती है । अन्तरंग साधना साधना का सूक्ष्म रूप है तो बहिरंग साधना भी साधना का स्थूल रूप है । दोनों का साध्य एक मनाकुलता ही है । लौकिक या शारीरिक क्रियामों पर आधारित बाह्य साधना भी निस्सन्देह अन्तरंगस्थ अनाकुलता की रक्षक, परिचायक और उपबृहक होती है। यदि साधना का बाह्याचार माकुलतावर्धक हो तो वह साधना ही नहीं है।
मसानिया वैराग्य और यशस्कामी शास्त्राभ्यास परमलौकिक प्रयोजन को तो पुष्ट कर सकते हैं, अलौकिक को नहीं। तदर्थ तो भेदविज्ञान की कला से जागृत वैराग्य और तत्त्वबोध की बढ़ता प्रयोजनीय होती है । वह वैराग्य और तत्त्वज्ञान ही क्या जो अनाकुल न हो । भेदविज्ञान की कथा से जागृत वैराग्य और तत्त्वज्ञान प्रनाकुल ही होता है । सुदंसणचरिउ अनाकुल वैराग्य और तत्त्वज्ञान के संस्कार देने में चरितकाव्य की हैसियत से अपनी पर्याप्त उपयोगिता रखता है। जैसे
मुनिश्री समाधिगुप्त वणिक् ऋषभदास को गृहस्थधर्म का उपदेश देते हैं । इस प्रसंग में उनका व्रताचरण का उपदेश तत्त्वज्ञान के निर्देशपूर्वक होता है । कवि प्रथमतः माप्त, प्रागम पौर तत्त्वों में श्रद्धान स्वरूप सम्यक्त्व को प्रतिपादित करता है। उसके अनुसार मिथ्यात्व पाप है और उससे कहीं भी शांति नहीं मिल सकती । सम्यक्त्व के बिना घोर और प्रबल तप संचय करने से शरीर का शोषण-मात्र होता है। बहुत कहने से क्या? वह तप वैसा ही प्रकृतार्य जाता है जैसे दुर्जन के प्रति किया गया उपकार । जिस प्रकार वृक्ष में मूल तथा शरीर में सिर सारभूत अंग है उसी प्रकार व्रतों में सारभूत सम्यक्त्व ही है (6.1)।
यहाँ कवि ने व्रताचरण के संबंध में लोकव्याप्त प्रज्ञानांधकार व अंधविश्वास का जिन स्पष्ट शब्दों में खंडन किया है वह मनाकुल मानन्द की अवाप्ति में अतिशय प्रयोजनीय है। मिथ्यात्व ही सर्वशान्ति का मंजक हैं, इस सार्थकता की रष्टि से तात्त्विक तो है ही।
इसी प्रकार कवि श्रावक के मूलगुणों, अणुव्रतों, गुणवतों और शिक्षाव्रतों का प्रतिपादन कर मधुबिन्दु दृष्टांत (6.16-17) से संसार की निस्सारता सिद्ध करता है और वैराग्यसम्पदा को जगाने के लिए वणिक्वर से कहता है-इस निस्सार संसार में तप ही परम सार है