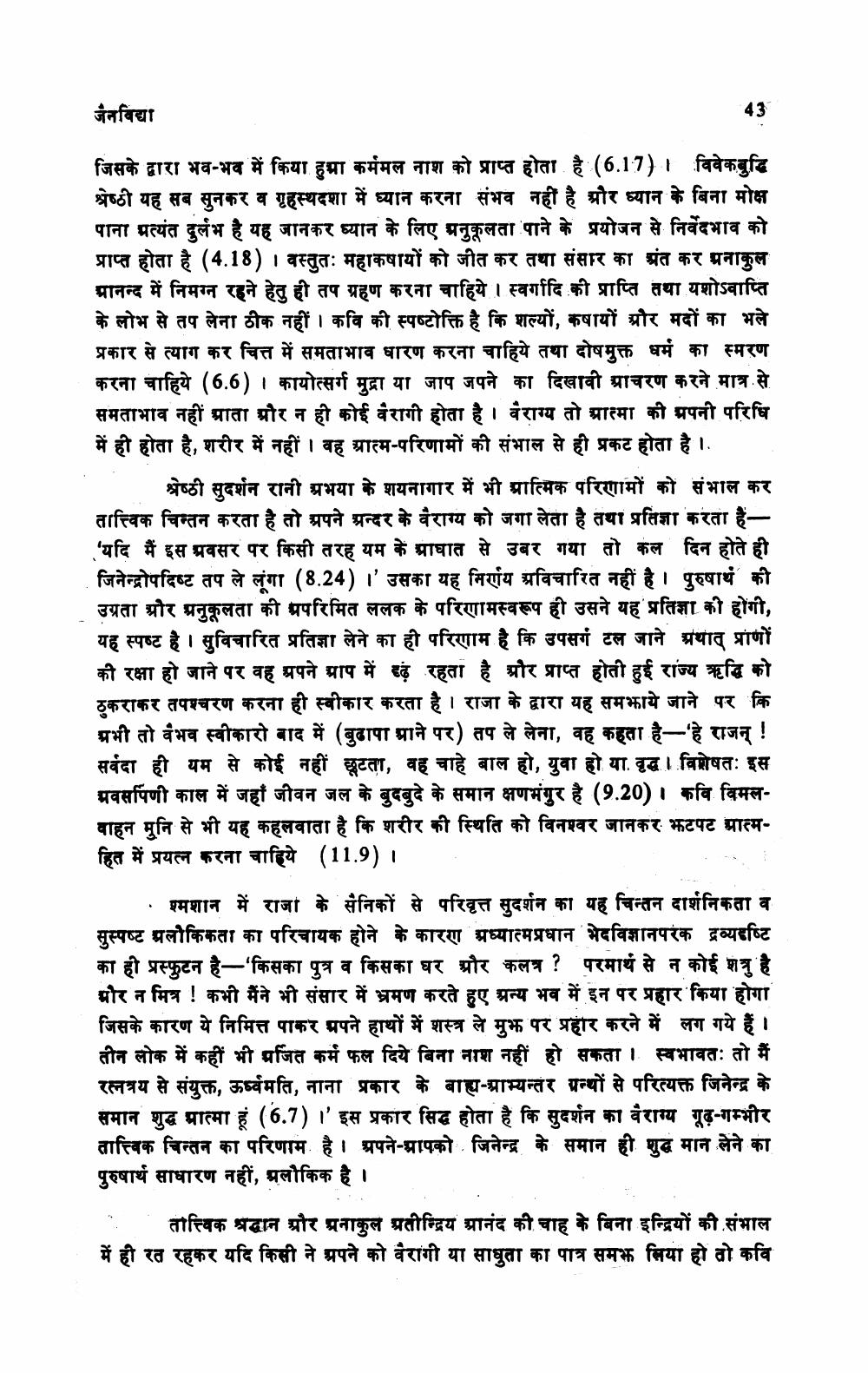________________
जनविद्या
जिसके द्वारा भव-भव में किया हुमा कर्ममल नाश को प्राप्त होता है (6.17)। विवेकबुद्धि श्रेष्ठी यह सब सुनकर व गृहस्थदशा में ध्यान करना संभव नहीं है और ध्यान के बिना मोक्ष पाना प्रत्यंत दुर्लभ है यह जानकर ध्यान के लिए अनुकूलता पाने के प्रयोजन से निर्वेदभाव को प्राप्त होता है (4.18) । वस्तुतः महाकषायों को जीत कर तथा संसार का अंत कर प्रनाकुल मानन्द में निमग्न रहने हेतु ही तप ग्रहण करना चाहिये । स्वर्गादि की प्राप्ति तथा यशोऽवाप्ति के लोभ से तप लेना ठीक नहीं । कवि की स्पष्टोक्ति है कि शल्यों, कषायों और मदों का भले प्रकार से त्याग कर चित्त में समताभाव धारण करना चाहिये तथा दोषमुक्त धर्म का स्मरण करना चाहिये (6.6) । कायोत्सर्ग मुद्रा या जाप जपने का दिखावी आचरण करने मात्र से समताभाव नहीं पाता और न ही कोई वैरागी होता है । वैराग्य तो प्रात्मा की अपनी परिधि में ही होता है, शरीर में नहीं । वह आत्म-परिणामों की संभाल से ही प्रकट होता है।
श्रेष्ठी सुदर्शन रानी अभया के शयनागार में भी पात्मिक परिणामों को संभाल कर तात्त्विक चिन्तन करता है तो अपने अन्दर के वैराग्य को जगा लेता है तथा प्रतिज्ञा करता है'यदि मैं इस अवसर पर किसी तरह यम के प्राघात से उबर गया तो कल दिन होते ही जिनेन्द्रोपदिष्ट तप ले लूंगा (8.24) ।' उसका यह निर्णय अविचारित नहीं है । पुरुषार्थ की उग्रता और अनुकूलता की अपरिमित ललक के परिणामस्वरूप ही उसने यह प्रतिज्ञा की होगी, यह स्पष्ट है । सुविचारित प्रतिज्ञा लेने का ही परिणाम है कि उपसर्ग टल जाने प्रथात् प्राणों की रक्षा हो जाने पर वह अपने पाप में दृढ़ रहता है और प्राप्त होती हुई राज्य ऋद्धि को ठुकराकर तपश्चरण करना ही स्वीकार करता है । राजा के द्वारा यह समझाये जाने पर कि अभी तो वैभव स्वीकारो बाद में (बुढापा पाने पर) तप ले लेना, वह कहता है-'हे राजन् ! सर्वदा ही यम से कोई नहीं छूटता, वह चाहे बाल हो, युवा हो या. वृद्ध । विशेषतः इस अवसर्पिणी काल में जहाँ जीवन जल के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर है (9.20)। कवि विमलवाहन मुनि से भी यह कहलवाता है कि शरीर की स्थिति को विनश्वर जानकर झटपट प्रात्महित में प्रयत्न करना चाहिये (11.9) ।
.. श्मशान में राजा के सैनिकों से परिवृत्त सुदर्शन का यह चिन्तन दार्शनिकता व सुस्पष्ट अलौकिकता का परिचायक होने के कारण अध्यात्मप्रधान भेदविज्ञानपरक द्रव्यदृष्टि का ही प्रस्फुटन है-'किसका पुत्र व किसका घर और कलत्र ? परमार्थ से न कोई शत्रु है मौर न मित्र ! कभी मैंने भी संसार में भ्रमण करते हुए अन्य भव में इन पर प्रहार किया होगा जिसके कारण ये निमित्त पाकर अपने हाथों में शस्त्र ले मुझ पर प्रहार करने में लग गये हैं। तीन लोक में कहीं भी अर्जित कर्म फल दिये बिना नाश नहीं हो सकता। स्वभावतः तो मैं रत्नत्रय से संयुक्त, ऊर्ध्वमति, नाना प्रकार के बाह्य-प्राभ्यन्तर ग्रन्थों से परित्यक्त जिनेन्द्र के समान शुद्ध प्रात्मा हूं (6.7)।' इस प्रकार सिद्ध होता है कि सुदर्शन का वैराग्य गूढ-गम्भीर तात्त्विक चिन्तन का परिणाम है। अपने पापको जिनेन्द्र के समान ही शुद्ध मान लेने का पुरुषार्थ साधारण नहीं, अलौकिक है ।
तात्त्विक श्रद्धान और प्रनाकुल प्रतीन्द्रिय आनंद की चाह के बिना इन्द्रियों की संभाल में ही रत रहकर यदि किसी ने अपने को वैरागी या साधुता का पात्र समझ लिया हो तो कवि