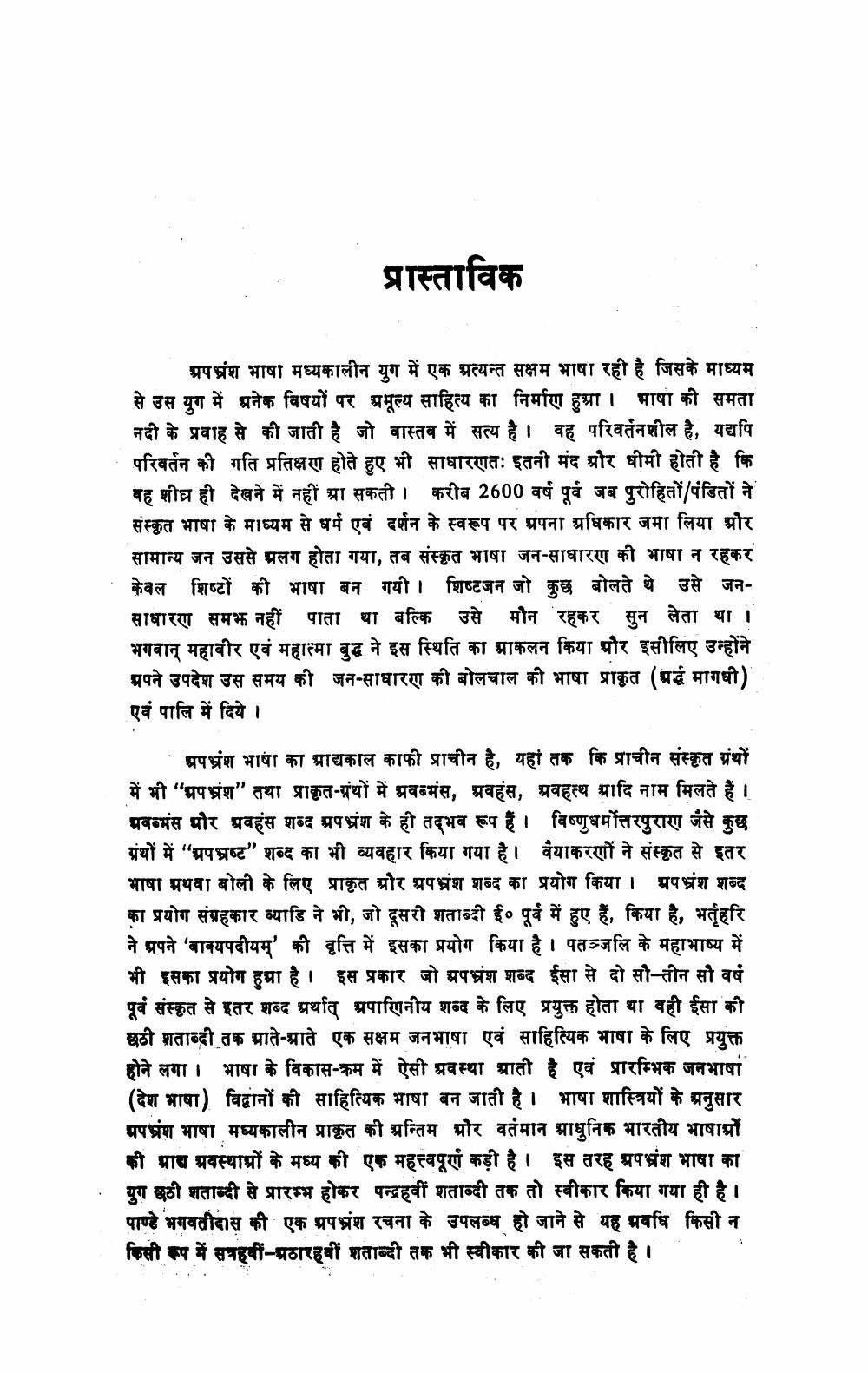________________
प्रास्ताविक
अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन युग में एक अत्यन्त सक्षम भाषा रही है जिसके माध्यम से उस युग में अनेक विषयों पर अमूल्य साहित्य का निर्माण हुआ। भाषा की समता नदी के प्रवाह से की जाती है जो वास्तव में सत्य है। वह परिवर्तनशील है, यद्यपि परिवर्तन की गति प्रतिक्षण होते हुए भी साधारणतः इतनी मंद और धीमी होती है कि वह शीघ्र ही देखने में नहीं आ सकती। करीब 2600 वर्ष पूर्व जब पुरोहितों/पंडितों ने संस्कृत भाषा के माध्यम से धर्म एवं दर्शन के स्वरूप पर अपना अधिकार जमा लिया और सामान्य जन उससे अलग होता गया, तब संस्कृत भाषा जन-साधारण की भाषा न रहकर केवल शिष्टों की भाषा बन गयी। शिष्टजन जो कुछ बोलते थे उसे जनसाधारण समझ नहीं पाता था बल्कि उसे मौन रहकर सुन लेता था । भगवान् महावीर एवं महात्मा बुद्ध ने इस स्थिति का प्राकलन किया और इसीलिए उन्होंने अपने उपदेश उस समय की जन-साधारण की बोलचाल की भाषा प्राकृत (प्रर्द्ध मागधी) एवं पालि में दिये।
अपभ्रंश भाषा का प्राद्यकाल काफी प्राचीन है, यहां तक कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी "अपभ्रंश" तथा प्राकृत-ग्रंथों में प्रवन्मंस, अवहंस, अवहत्थ आदि नाम मिलते हैं । प्रवन्मंस मोर अवहंस शब्द अपभ्रंश के ही तद्भव रूप हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण जैसे कुछ ग्रंथों में "अपभ्रष्ट" शब्द का भी व्यवहार किया गया है। वैयाकरणों ने संस्कृत से इतर भाषा अथवा बोली के लिए प्राकृत और अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग संग्रहकार व्याडि ने भी, जो दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में हुए हैं, किया है, भर्तृहरि ने अपने 'वाक्यपदीयम्' की वृत्ति में इसका प्रयोग किया है । पतञ्जलि के महाभाष्य में भी इसका प्रयोग हुआ है। इस प्रकार जो अपभ्रंश शब्द ईसा से दो सौ-तीन सौ वर्ष पूर्व संस्कृत से इतर शब्द अर्थात् अपाणिनीय शब्द के लिए प्रयुक्त होता था वही ईसा की छठी शताब्दी तक माते-पाते एक सक्षम जन भाषा एवं साहित्यिक भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। भाषा के विकास-क्रम में ऐसी अवस्था पाती है एवं प्रारम्भिक जनभाषा (देश भाषा) विद्वानों की साहित्यिक भाषा बन जाती है। भाषा शास्त्रियों के अनुसार अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन प्राकृत की अन्तिम और वर्तमान प्राधुनिक भारतीय भाषामों की माय भवस्थानों के मध्य की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इस तरह अपभ्रंश भाषा का युग छठी शताब्दी से प्रारम्भ होकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक तो स्वीकार किया गया ही है। पाण्डे भगवतीदास की एक अपभ्रंश रचना के उपलब्ध हो जाने से यह अवधि किसी न किसी रूप में सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी तक भी स्वीकार की जा सकती है ।