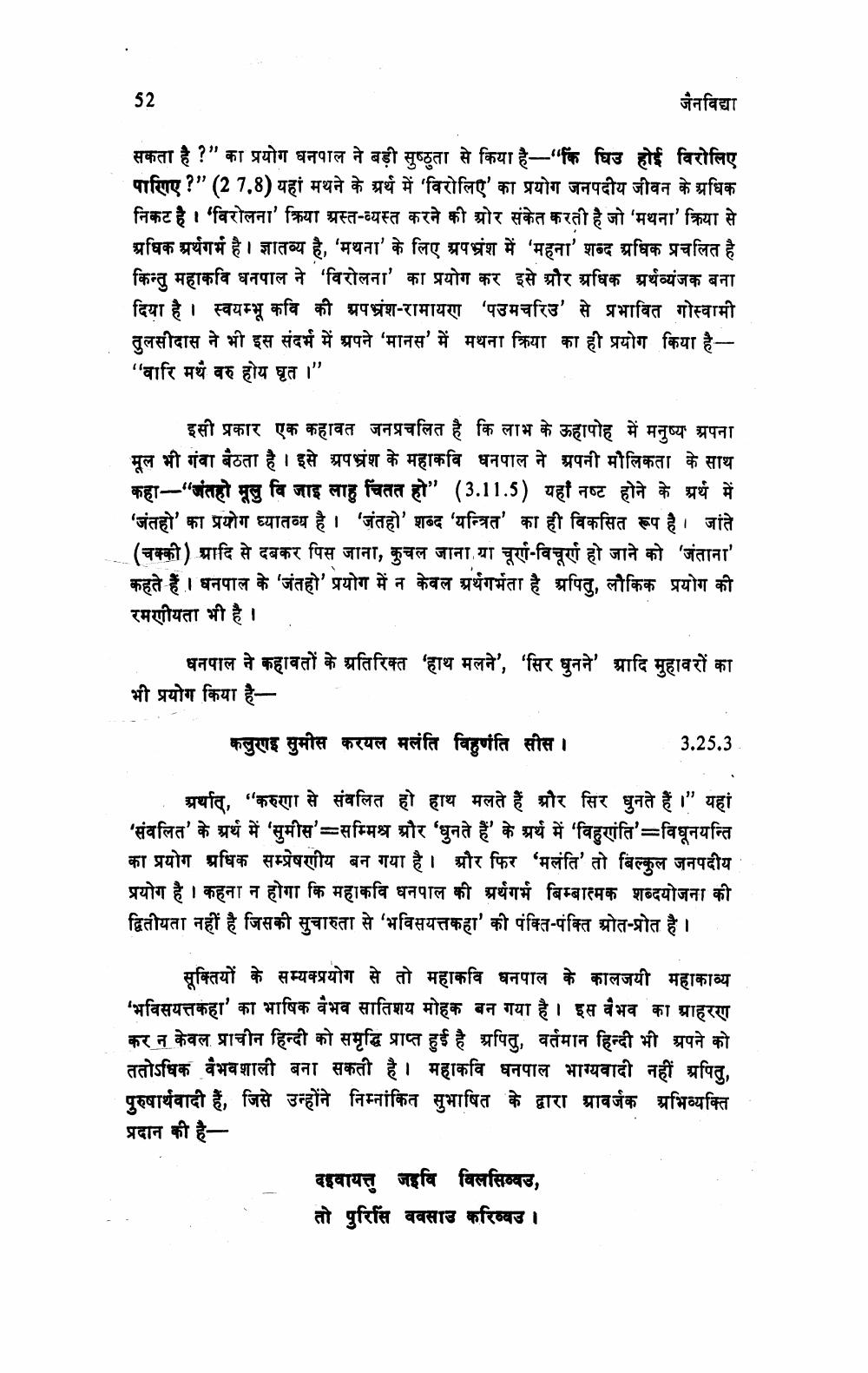________________
जनविद्या
सकता है ?" का प्रयोग धनपाल ने बड़ी सुष्ठुता से किया है-"किं घिउ होई विरोलिए पाणिए ?" (2 7.8) यहां मथने के अर्थ में 'विरोलिए' का प्रयोग जनपदीय जीवन के अधिक निकट है । 'विरोलना' क्रिया अस्त-व्यस्त करने की ओर संकेत करती है जो 'मथना' क्रिया से अधिक अर्थगर्भ है । ज्ञातव्य है, 'मथना' के लिए अपभ्रंश में 'महना' शब्द अधिक प्रचलित है किन्तु महाकवि धनपाल ने 'विरोलना' का प्रयोग कर इसे और अधिक अर्थव्यंजक बना दिया है। स्वयम्भू कवि की अपभ्रंश-रामायण 'पउमचरिउ' से प्रभावित गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस संदर्भ में अपने 'मानस' में मथना क्रिया का ही प्रयोग किया है"वारि मथै वरु होय घृत ।"
इसी प्रकार एक कहावत जनप्रचलित है कि लाभ के ऊहापोह में मनुष्य अपना मूल भी गंवा बैठता है । इसे अपभ्रंश के महाकवि धनपाल ने अपनी मौलिकता के साथ कहा-"जतहो मूलु वि जाइ लाहु चितत हो" (3.11.5) यहां नष्ट होने के अर्थ में 'जंतहो' का प्रयोग ध्यातव्य है । 'जंतहो' शब्द 'यन्त्रित' का ही विकसित रूप है। जाते (चक्की) प्रादि से दबकर पिस जाना, कुचल जाना या चूर्ण-विचूर्ण हो जाने को 'जताना' कहते हैं । धनपाल के 'जतहो' प्रयोग में न केवल अर्थगर्भता है अपितु, लौकिक प्रयोग की रमणीयता भी है।
धनपाल ने कहावतों के अतिरिक्त 'हाथ मलने', 'सिर धुनने' आदि मुहावरों का भी प्रयोग किया है
कलुणइ सुमीस करयल मलंति विहुगंति सीस।
3.25.3.
अर्थात्, “करुणा से संवलित हो हाथ मलते हैं और सिर धुनते हैं ।" यहां 'संवलित' के अर्थ में 'सुमीस' =सम्मिश्र और 'धुनते हैं' के अर्थ में 'विहुणंति'=विधूनयन्ति का प्रयोग अधिक सम्प्रेषणीय बन गया है। और फिर 'मलंति' तो बिल्कुल जनपदीय प्रयोग है । कहना न होगा कि महाकवि धनपाल की अर्थगर्भ बिम्बात्मक शब्दयोजना की द्वितीयता नहीं है जिसकी सुचारुता से 'भविसयत्तकहा' की पंक्ति-पंक्ति प्रोत-प्रोत है।
सक्तियों के सम्यक्प्रयोग से तो महाकवि धनपाल के कालजयी महाकाव्य 'भविसयत्तकहा' का भाषिक वैभव सातिशय मोहक बन गया है। इस वैभव का प्राहरण कर न केवल प्राचीन हिन्दी को समृद्धि प्राप्त हुई है अपितु, वर्तमान हिन्दी भी अपने को ततोऽधिक वैभवशाली बना सकती है। महाकवि धनपाल भाग्यवादी नहीं अपितु, पुरुषार्थवादी हैं, जिसे उन्होंने निम्नांकित सुभाषित के द्वारा आवर्जक अभिव्यक्ति प्रदान की है
दइवायत्तु जइवि विलसिव्वउ, तो पुरिसिं ववसाउ करिव्वउ ।