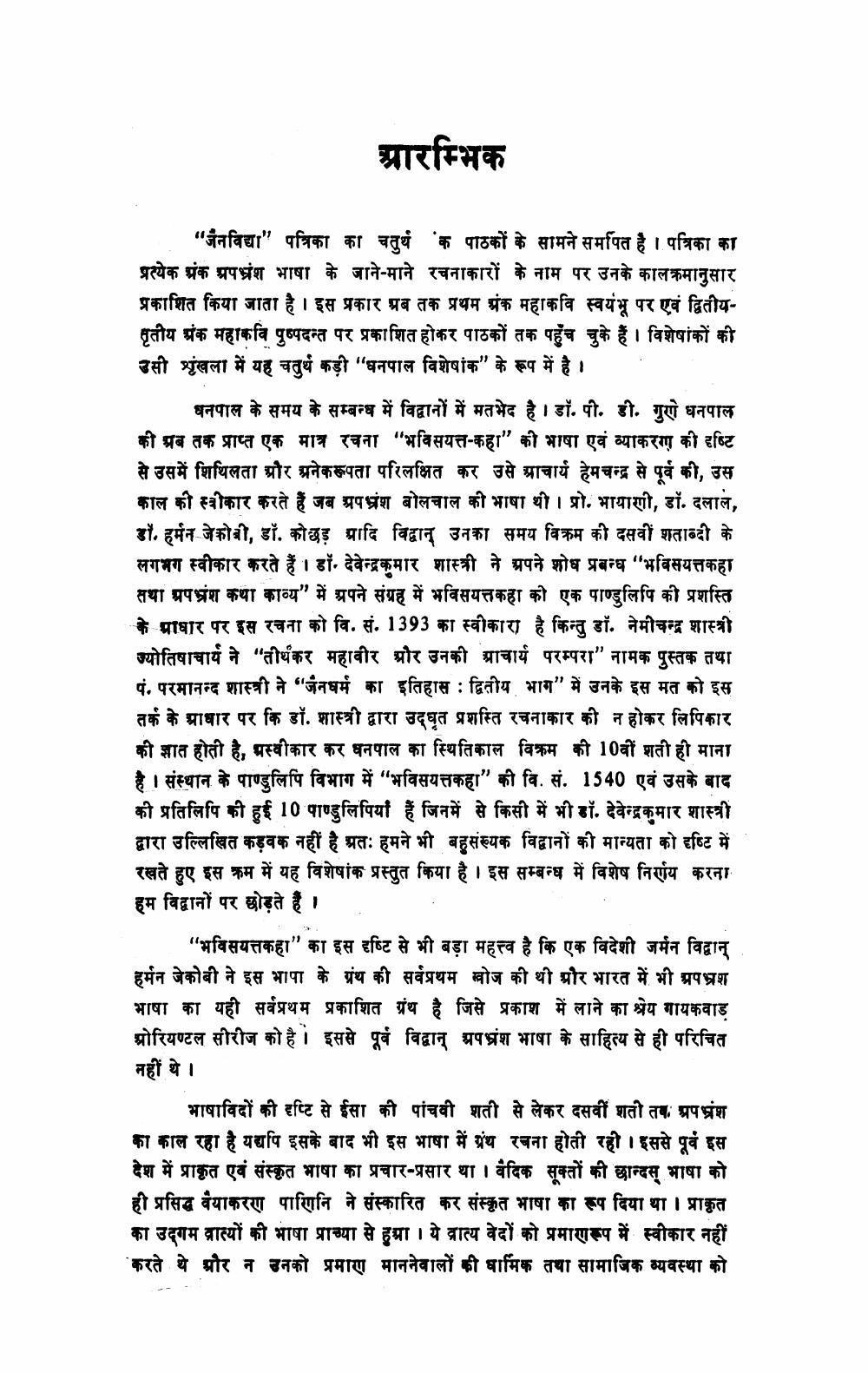________________
प्रारम्भिक
"जनविद्या" पत्रिका का चतुर्थ क पाठकों के सामने समर्पित है । पत्रिका का प्रत्येक अंक अपभ्रंश भाषा के जाने-माने रचनाकारों के नाम पर उनके कालक्रमानुसार प्रकाशित किया जाता है । इस प्रकार अब तक प्रथम अंक महाकवि स्वयंभू पर एवं द्वितीयतृतीय अंक महाकवि पुष्पदन्त पर प्रकाशित होकर पाठकों तक पहुंच चुके हैं । विशेषांकों की उसी शृंखला में यह चतुर्थ कड़ी "धनपाल विशेषांक" के रूप में है।
धनपाल के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। डॉ. पी. डी. गुणे धनपाल की अब तक प्राप्त एक मात्र रचना "भक्सियत्त-कहा" की भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से उसमें शिथिलता और अनेकरूपता परिलक्षित कर उसे प्राचार्य हेमचन्द्र से पूर्व की, उस काल की स्वीकार करते हैं जब अपभ्रंश बोलचाल की भाषा थी। प्रो. भायाणी, डॉ. दलाल, डॉ. हर्मन जेकोबी, डॉ. कोछड़ प्रादि विद्वान् उनका समय विक्रम की दसवीं शताब्दी के लगभग स्वीकार करते हैं । डॉ. देवेन्द्रकुमार शास्त्री ने अपने शोध प्रबन्ध "भविसयत्तकहा सथा अपभ्रंश कथा काव्य" में अपने संग्रह में भविसयत्तकहा को एक पाण्डुलिपि की प्रशस्ति के प्राधार पर इस रचना को वि. सं. 1393 का स्वीकारा है किन्तु डॉ. नेमीचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने "तीर्थंकर महावीर और उनकी प्राचार्य परम्परा" नामक पुस्तक तथा पं. परमानन्द शास्त्री ने "जैनधर्म का इतिहास : द्वितीय भाग" में उनके इस मत को इस तर्क के आधार पर कि डॉ. शास्त्री द्वारा उद्धृत प्रशस्ति रचनाकार की न होकर लिपिकार की ज्ञात होती है, अस्वीकार कर धनपाल का स्थितिकाल विक्रम की 10वीं शती ही माना है । संस्थान के पाण्डुलिपि विभाग में "भविसयत्तकहा" की वि. सं. 1540 एवं उसके बाद की प्रतिलिपि की हुई 10 पाण्डुलिपियां हैं जिनमें से किसी में भी डॉ. देवेन्द्रकुमार शास्त्री द्वारा उल्लिखित कड़वक नहीं है अतः हमने भी बहुसंख्यक विद्वानों की मान्यता को दृष्टि में रखते हुए इस क्रम में यह विशेषांक प्रस्तुत किया है । इस सम्बन्ध में विशेष निर्णय करना हम विद्वानों पर छोड़ते हैं ।
___ "भविसयत्तकहा" का इस दृष्टि से भी बड़ा महत्त्व है कि एक विदेशी जर्मन विद्वान् हर्मन जेकोबी ने इस भापा के ग्रंथ की सर्वप्रथम खोज की थी और भारत में भी अपभ्रश भाषा का यही सर्वप्रथम प्रकाशित ग्रंथ है जिसे प्रकाश में लाने का श्रेय गायकवाड़ प्रोरियण्टल सीरीज को है। इससे पूर्व विद्वान् अपभ्रंश भाषा के साहित्य से ही परिचित नहीं थे।
भाषाविदों की दृष्टि से ईसा की पांचवी शती से लेकर दसवीं शती तक अपभ्रंश का काल रहा है यद्यपि इसके बाद भी इस भाषा में ग्रंथ रचना होती रही। इससे पूर्व इस देश में प्राकृत एवं संस्कृत भाषा का प्रचार-प्रसार था । वैदिक सूक्तों की छान्दस् भाषा को ही प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने संस्कारित कर संस्कृत भाषा का रूप दिया था । प्राकृत का उद्गम व्रात्यों की भाषा प्राच्या से हुआ । ये व्रात्य वेदों को प्रमाणरूप में स्वीकार नहीं करते थे और न उनको प्रमाण माननेवालों की धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था को