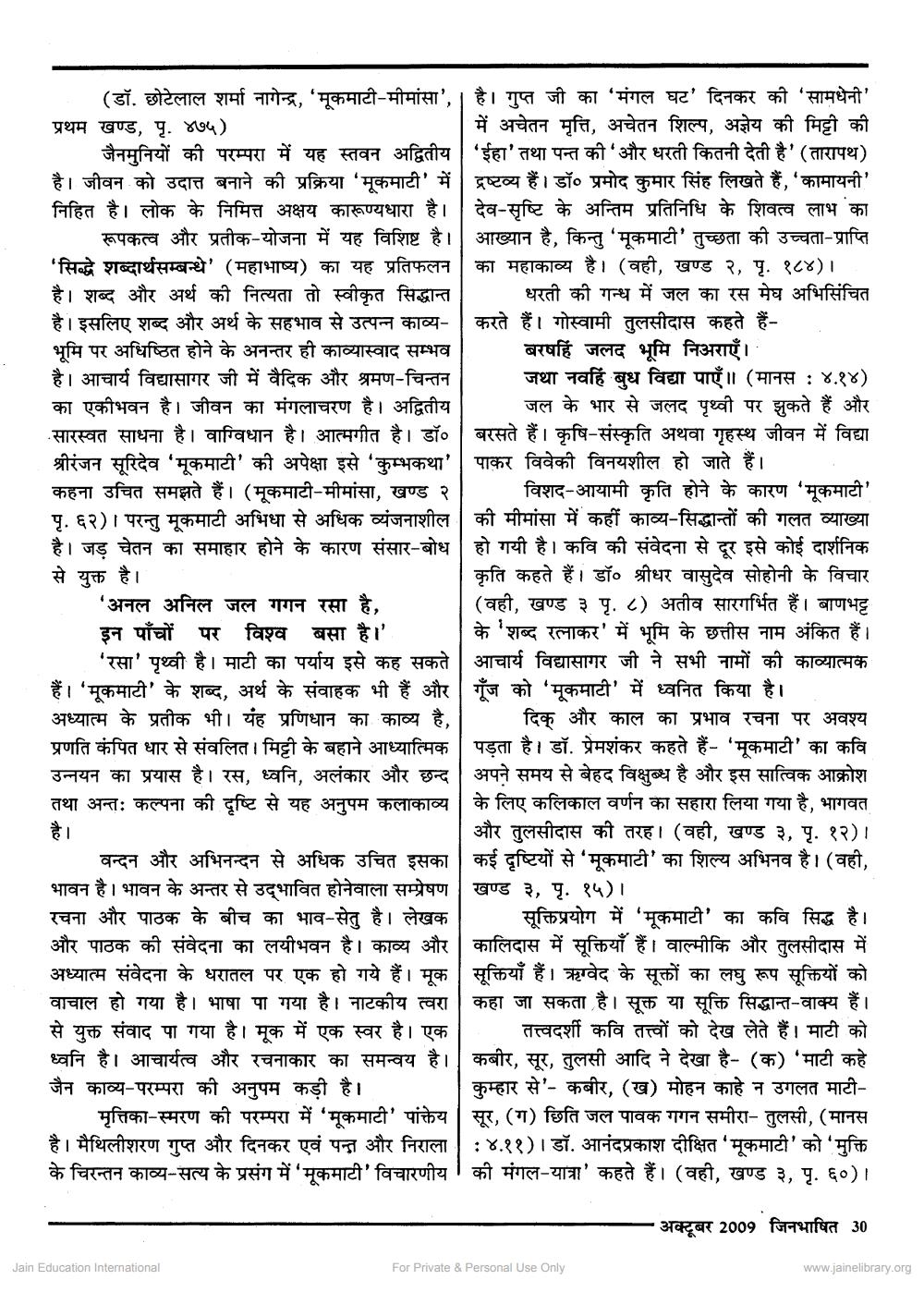________________
।
6
(डॉ. छोटेलाल शर्मा नागेन्द्र, 'मूकमाटी-मीमांसा' है। गुप्त जी का 'मंगल घट' दिनकर की 'सामधेनी' में अचेतन मृत्ति, अचेतन शिल्प, अज्ञेय की मिट्टी की 'ईहा' तथा पन्त की और धरती कितनी देती है' (तारापथ) द्रष्टव्य हैं। डॉ० प्रमोद कुमार सिंह लिखते हैं, 'कामायनी' देव सृष्टि के अन्तिम प्रतिनिधि के शिवत्व लाभ का - आख्यान है, किन्तु 'मूकमाटी' तुच्छता की उच्चता - प्राप्ति का महाकाव्य है। (वही, खण्ड २, पृ. १८४) ।
धरती की गन्ध में जल का रस मेघ अभिसिंचित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं
बरषहिं जलद भूमि निअराएँ।
प्रथम खण्ड, पृ. ४७५)
जैनमुनियों की परम्परा में यह स्तवन अद्वितीय है। जीवन को उदात्त बनाने की प्रक्रिया 'मूकमाटी' में निहित है। लोक के निमित्त अक्षय कारूण्यधारा है।
रूपकत्व और प्रतीक योजना में यह विशिष्ट है। 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' ( महाभाष्य) का यह प्रतिफलन है शब्द और अर्थ की नित्यता तो स्वीकृत सिद्धान्त है। इसलिए शब्द और अर्थ के सहभाव से उत्पन्न काव्यभूमि पर अधिष्ठित होने के अनन्तर ही काव्यास्वाद सम्भव है। आचार्य विद्यासागर जी में वैदिक और श्रमण-चिन्तन का एकीभवन है। जीवन का मंगलाचरण है। अद्वितीय सारस्वत साधना है। वाग्विधान है। आत्मगीत है। डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव मूकमाटी' की अपेक्षा इसे 'कुम्भकथा' कहना उचित समझते हैं (मूकमाटी मीमांसा, खण्ड २ पृ. ६२) । परन्तु मूकमाटी अभिधा से अधिक व्यंजनाशील है जड़ चेतन का समाहार होने के कारण संसार बोध - से युक्त है ।
'अनल अनिल जल गगन रसा है, इन पाँचों पर विश्व बसा है ।' 'रसा' पृथ्वी है। माटी का पर्याय इसे कह सकते हैं। 'मूकमाटी' के शब्द अर्थ के संवाहक भी हैं और अध्यात्म के प्रतीक भी। यह प्रणिधान का काव्य है, प्रणति कंपित धार से संवलित मिट्टी के बहाने आध्यात्मिक उन्नयन का प्रयास है रस, ध्वनि, अलंकार और छन्द तथा अन्तः कल्पना की दृष्टि से यह अनुपम कलाकाव्य है।
वन्दन और अभिनन्दन से अधिक उचित इसका भाव है। भावन के अन्तर से उद्भावित होनेवाला सम्प्रेषण रचना और पाठक के बीच का भाव- सेतु है । लेखक और पाठक की संवेदना का लयीभवन है। काव्य और अध्यात्म संवेदना के धरातल पर एक हो गये हैं। मूक वाचाल हो गया है। भाषा पा गया है नाटकीय त्वरा से युक्त संवाद पा गया है। मूक में एक स्वर है। एक ध्वनि है। आचार्यत्व और रचनाकार का समन्वय है । जैन काव्य- परम्परा की अनुपम कड़ी है।
मृत्तिका - स्मरण की परम्परा में 'मूकमाटी' पांक्तेय है। मैथिलीशरण गुप्त और दिनकर एवं पन्त और निराला के चिरन्तन काव्य-सत्य के प्रसंग में 'मूकमाटी' विचारणीय
Jain Education International
जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ । ( मानस : ४.१४) जल के भार से जलद पृथ्वी पर झुकते हैं और बरसते हैं। कृषि संस्कृति अथवा गृहस्थ जीवन में विद्या पाकर विवेकी विनयशील हो जाते हैं।
।
-
विशद-आयामी कृति होने के कारण 'मूकमाटी' की मीमांसा में कहीं काव्य सिद्धान्तों की गलत व्याख्या हो गयी है। कवि की संवेदना से दूर इसे कोई दार्शनिक कृति कहते हैं। डॉ० श्रीधर वासुदेव सोहोनी के विचार (वही, खण्ड ३ पृ. ८) अतीव सारगर्भित हैं । बाणभट्ट के 'शब्द रत्नाकर' में भूमि के छत्तीस नाम अंकित हैं। आचार्य विद्यासागर जी ने सभी नामों की काव्यात्मक गूँज को 'मूकमाटी' में ध्वनित किया है।
दिक् और काल का प्रभाव रचना पर अवश्य पड़ता है। डॉ. प्रेमशंकर कहते हैं- 'मूकमाटी' का कवि अपने समय से बेहद विक्षुब्ध है और इस सात्विक आक्रोश के लिए कलिकाल वर्णन का सहारा लिया गया है, भागवत और तुलसीदास की तरह (वही, खण्ड ३, पृ. १२) । कई दृष्टियों से 'मूकमाटी' का शिल्य अभिनव है। (वही, खण्ड ३, पृ. १५) ।
।
सूक्तिप्रयोग में 'मूकमाटी' का कवि सिद्ध है। कालिदास में सूक्तियाँ हैं। वाल्मीकि और तुलसीदास में सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद के सूक्तों का लघु रूप सूक्तियों को कहा जा सकता है। सूक्त या सूक्ति सिद्धान्त वाक्य हैं।
तत्त्वदर्शी कवि तत्त्वों को देख लेते हैं। माटी को कबीर, सूर, तुलसी आदि ने देखा है- (क) 'माटी कहे कुम्हार से' कबीर, (ख) मोहन काहे न उगलत माटीसूर, (ग) छिति जल पावक गगन समीरा - तुलसी, (मानस : ४.११) । डॉ. आनंदप्रकाश दीक्षित 'मूकमाटी' को 'मुक्ति की मंगल यात्रा' कहते हैं (वही, खण्ड ३, पृ. ६० ) ।
अक्टूबर 2009 जिनभाषित 30
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org