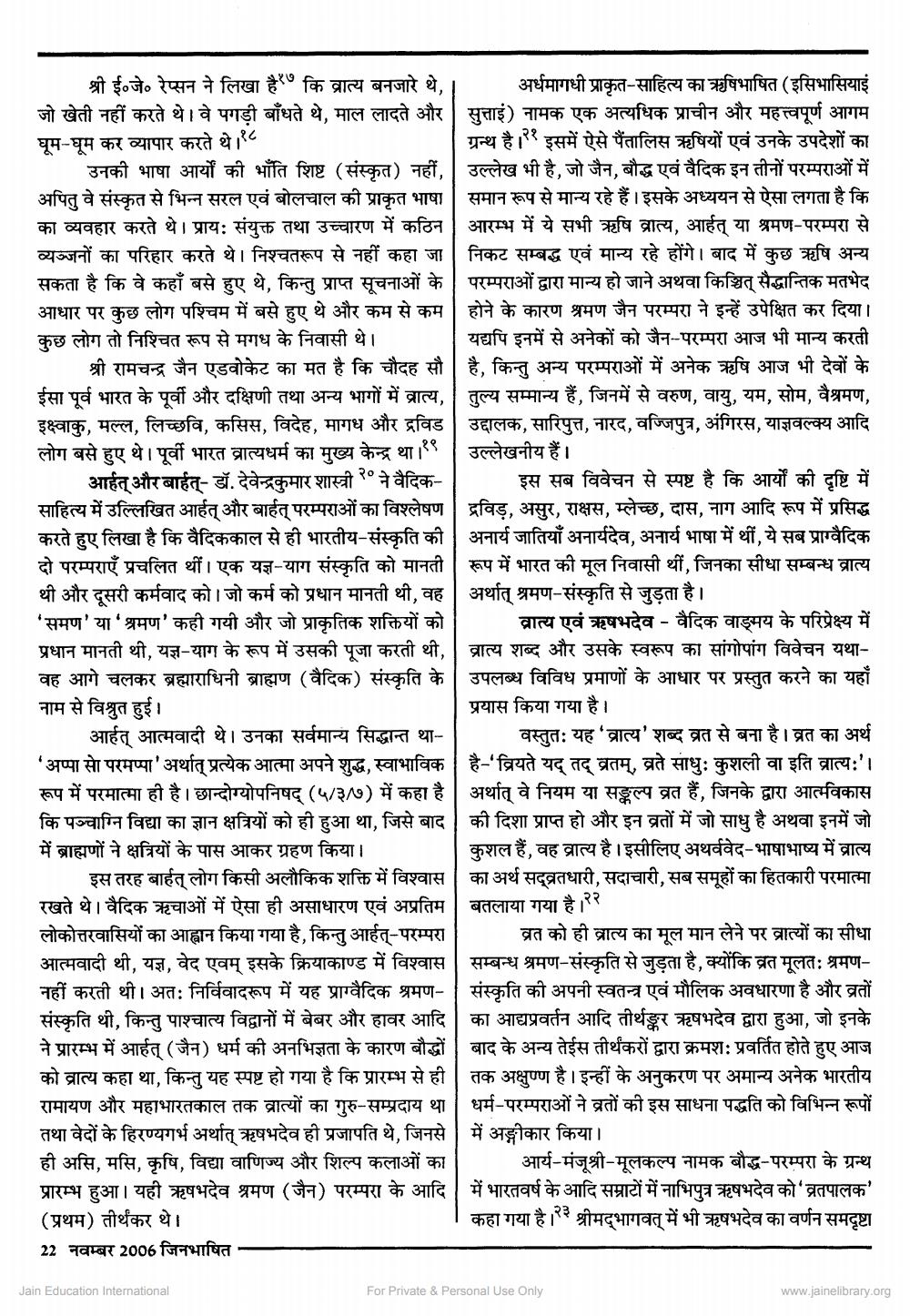________________
श्री ई० जे० रेप्सन ने लिखा है कि व्रात्य बनजारे थे, जो खेती नहीं करते थे। वे पगड़ी बाँधते थे, माल लादते और घूम-घूम कर व्यापार करते थे । १८
उनकी भाषा आर्यों की भाँति शिष्ट (संस्कृत) नहीं, अपितु वे संस्कृत से भिन्न सरल एवं बोलचाल की प्राकृत भाषा का व्यवहार करते थे । प्रायः संयुक्त तथा उच्चारण में कठिन व्यञ्जनों का परिहार करते थे। निश्चतरूप से नहीं कहा जा सकता है कि वे कहाँ बसे हुए थे, किन्तु प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ लोग पश्चिम में बसे हुए थे और कम से कम कुछ लोग तो निश्चित रूप से मगध के निवासी थे ।
श्री रामचन्द्र जैन एडवोकेट का मत है कि चौदह सौ ईसा पूर्व भारत के पूर्वी और दक्षिणी तथा अन्य भागों में व्रात्य, इक्ष्वाकु, मल्ल, लिच्छवि, कसिस, विदेह, मागध और द्रविड लोग बसे हुए थे पूर्वी भारत व्रात्यधर्म का मुख्य केन्द्र था । १९
आर्हत् और बार्हत्- डॉ. देवेन्द्रकुमार शास्त्री २० ने वैदिकसाहित्य में उल्लिखित आर्हत् और बार्हत् परम्पराओं का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि वैदिककाल से ही भारतीय-संस्कृति की दो परम्पराएँ प्रचलित थीं। एक यज्ञ-याग संस्कृति को मानती थी और दूसरी कर्मवाद को। जो कर्म को प्रधान मानती थी, वह 'समण' या 'श्रमण' कही गयी और जो प्राकृतिक शक्तियों को प्रधान मानती थी, यज्ञ-याग के रूप में उसकी पूजा करती थी, वह आगे चलकर ब्रह्माराधिनी ब्राह्मण (वैदिक) संस्कृति के नाम से विश्रुत हुई ।
आर्हत् आत्मवादी थे । उनका सर्वमान्य सिद्धान्त था'अप्पा सा परमप्पा' अर्थात् प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध, स्वाभाविक रूप में परमात्मा ही है। छान्दोग्योपनिषद् (५/३/७ ) में कहा है कि पञ्चाग्नि विद्या का ज्ञान क्षत्रियों को ही हुआ था, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के पास आकर ग्रहण किया।
इस तरह बार्हत् लोग किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते थे। वैदिक ऋचाओं में ऐसा ही असाधारण एवं अप्रतिम लोकोत्तरवासियों का आह्वान किया गया है, किन्तु आर्हत्-परम्परा आत्मवादी थी, यज्ञ, वेद एवम् इसके क्रियाकाण्ड में विश्वास नहीं करती थी । अतः निर्विवादरूप में यह प्राग्वैदिक श्रमणसंस्कृति थी, किन्तु पाश्चात्य विद्वानों में बेबर और हावर आदि ने प्रारम्भ में आर्हत् (जैन) धर्म की अनभिज्ञता के कारण बौद्धों को व्रात्य कहा था, किन्तु यह स्पष्ट हो गया है कि प्रारम्भ से ही रामायण और महाभारतकाल तक व्रात्यों का गुरु- सम्प्रदाय था तथा वेदों के हिरण्यगर्भ अर्थात् ऋषभदेव ही प्रजापति थे, जिनसे ही असि, मसि, कृषि, विद्या वाणिज्य और शिल्प कलाओं का प्रारम्भ हुआ । यही ऋषभदेव श्रमण (जैन) परम्परा के आदि (प्रथम) तीर्थंकर थे ।
22 नवम्बर 2006 जिनभाषित
Jain Education International
अर्धमागधी प्राकृत-साहित्य का ऋषिभाषित (इसिभासियाई सुत्ताइं ) नामक एक अत्यधिक प्राचीन और महत्त्वपूर्ण आगम ग्रन्थ है । २१ इसमें ऐसे पैंतालिस ऋषियों एवं उनके उपदेशों का उल्लेख भी है, जो जैन, बौद्ध एवं वैदिक इन तीनों परम्पराओं में समान रूप से मान्य रहे हैं। इसके अध्ययन से ऐसा लगता है कि आरम्भ में ये सभी ऋषि व्रात्य, आर्हत् या श्रमण परम्परा से निकट सम्बद्ध एवं मान्य रहे होंगे। बाद में कुछ ऋषि अन्य परम्पराओं द्वारा मान्य हो जाने अथवा किञ्चित् सैद्धान्तिक मतभेद होने के कारण श्रमण जैन परम्परा ने इन्हें उपेक्षित कर दिया । यद्यपि इनमें से अनेकों को जैन-परम्परा आज भी मान्य करती है, किन्तु अन्य परम्पराओं में अनेक ऋषि आज भी देवों के तुल्य सम्मान्य हैं, जिनमें से वरुण, वायु, यम, सोम, वैश्रमण, उद्दालक, सारिपुत्त, नारद, वज्जिपुत्र, अंगिरस, याज्ञवल्क्य आदि उल्लेखनीय हैं।
इस सब विवेचन से स्पष्ट है कि आर्यों की दृष्टि में द्रविड़, असुर, राक्षस, म्लेच्छ, दास, नाग आदि रूप में प्रसिद्ध अनार्य जातियाँ अनार्यदेव, अनार्य भाषा में थीं, ये सब प्राग्वैदिक रूप में भारत की मूल निवासी थीं, जिनका सीधा सम्बन्ध व्रात्य अर्थात् श्रमण-संस्कृति से जुड़ता है।
व्रात्य एवं ऋषभदेव - वैदिक वाड्मय के परिप्रेक्ष्य में व्रात्य शब्द और उसके स्वरूप का सांगोपांग विवेचन यथाउपलब्ध विविध प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करने का यहाँ प्रयास किया गया है।
वस्तुत: यह 'व्रात्य' शब्द व्रत से बना है। व्रत का अर्थ है- 'व्रियते यद् तद् व्रतम्, व्रते साधुः कुशली वा इति व्रात्यः' । अर्थात् वे नियम या सङ्कल्प व्रत हैं, जिनके द्वारा आत्मविकास की दिशा प्राप्त हो और इन व्रतों में जो साधु है अथवा इनमें जो कुशल हैं, वह व्रात्य है। इसीलिए अथर्ववेद - भाषाभाष्य में व्रात्य का अर्थ सद्व्रतधारी, सदाचारी, सब समूहों का हितकारी परमात्मा बतलाया गया है। २२
व्रत को ही व्रात्य का मूल मान लेने पर व्रात्यों का सीधा सम्बन्ध श्रमण-संस्कृति से जुड़ता है, क्योंकि व्रत मूलतः श्रमणसंस्कृति की अपनी स्वतन्त्र एवं मौलिक अवधारणा है और व्रतों का आद्यप्रवर्तन आदि तीर्थङ्कर ऋषभदेव द्वारा हुआ, जो इनके बाद के अन्य तेईस तीर्थंकरों द्वारा क्रमशः प्रवर्तित होते हुए आज तक अक्षुण्ण है। इन्हीं के अनुकरण पर अमान्य अनेक भारतीय धर्म-परम्पराओं ने व्रतों की इस साधना पद्धति को विभिन्न रूपों में अङ्गीकार किया ।
आर्य-मंजूश्री - मूलकल्प नामक बौद्ध परम्परा के ग्रन्थ में भारतवर्ष के आदि सम्राटों में नाभिपुत्र ऋषभदेव को 'व्रतपालक' कहा गया है । २३ श्रीमद्भागवत् में भी ऋषभदेव का वर्णन समदृष्टा
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org