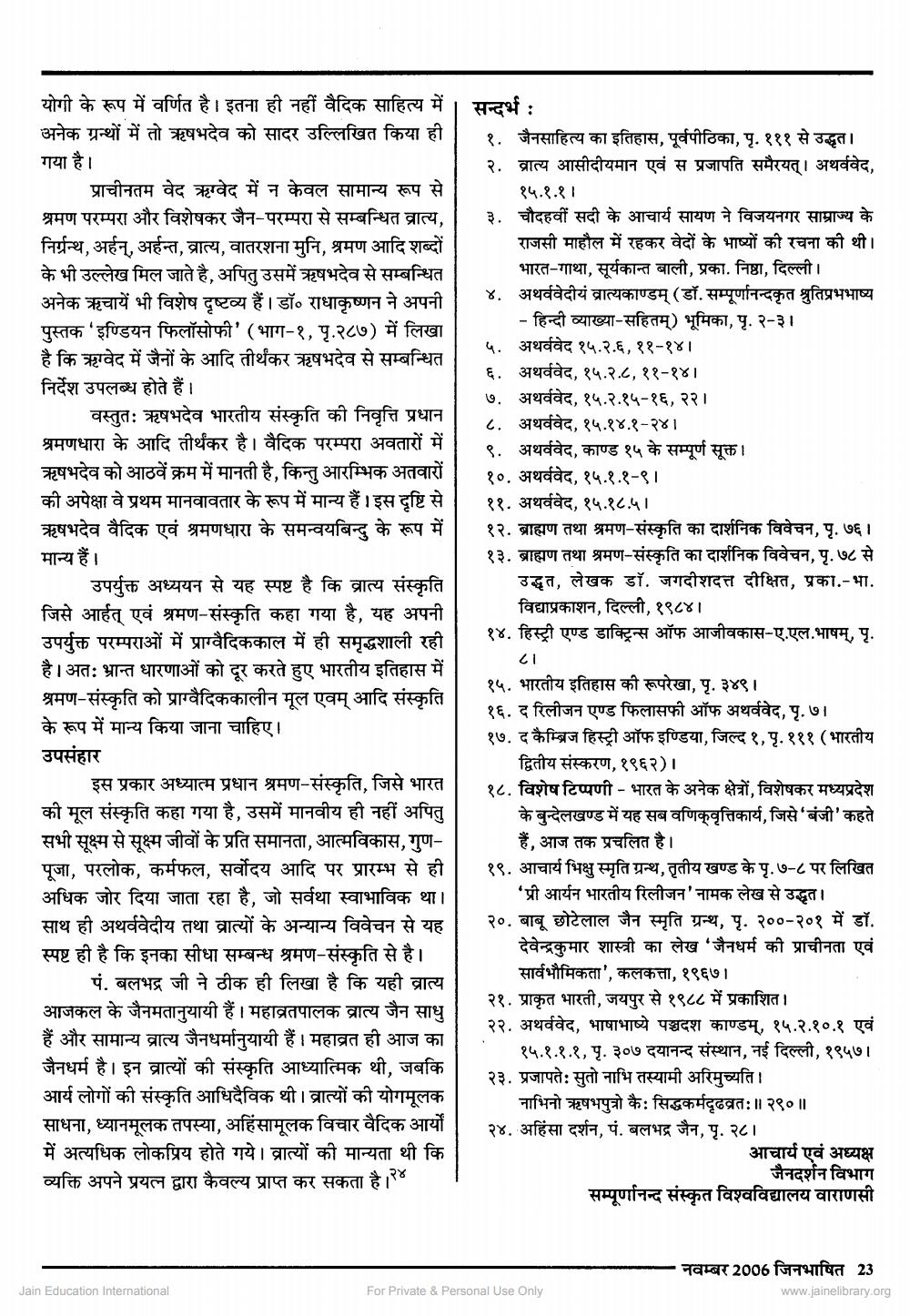________________
योगी के रूप में वर्णित है। इतना ही नहीं वैदिक साहित्य में । अनेक ग्रन्थों में तो ऋषभदेव को सादर उल्लिखित किया ही गया है।
प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में न केवल सामान्य रूप से श्रमण परम्परा और विशेषकर जैन-परम्परा से सम्बन्धित व्रात्य, निर्ग्रन्थ, अर्हन्, अर्हन्त, व्रात्य, वातरशना मुनि, श्रमण आदि शब्दों के भी उल्लेख मिल जाते है, अपितु उसमें ऋषभदेव से सम्बन्धित अनेक ऋचायें भी विशेष दृष्टव्य हैं। डॉ. राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक 'इण्डियन फिलॉसोफी' (भाग-१, पृ.२८७) में लिखा है कि ऋग्वेद में जैनों के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से सम्बन्धित निर्देश उपलब्ध होते हैं।
वस्तुतः ऋषभदेव भारतीय संस्कृति की निवृत्ति प्रधान श्रमणधारा के आदि तीर्थंकर है। वैदिक परम्परा अवतारों में ऋषभदेव को आठवें क्रम में मानती है, किन्तु आरम्भिक अतवारों की अपेक्षा वे प्रथम मानवावतार के रूप में मान्य हैं। इस दृष्टि से ऋषभदेव वैदिक एवं श्रमणधारा के समन्वयबिन्दु के रूप में मान्य हैं।
उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि व्रात्य संस्कृति जिसे आर्हत् एवं श्रमण-संस्कृति कहा गया है, यह अपनी उपर्युक्त परम्पराओं में प्राग्वैदिककाल में ही समृद्धशाली रही | है। अतः भ्रान्त धारणाओं को दूर करते हुए भारतीय इतिहास में श्रमण-संस्कृति को प्राग्वैदिककालीन मूल एवम् आदि संस्कृति के रूप में मान्य किया जाना चाहिए। उपसंहार
इस प्रकार अध्यात्म प्रधान श्रमण-संस्कृति, जिसे भारत की मूल संस्कृति कहा गया है, उसमें मानवीय ही नहीं अपितु सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों के प्रति समानता, आत्मविकास, गुणपूजा, परलोक, कर्मफल, सर्वोदय आदि पर प्रारम्भ से ही अधिक जोर दिया जाता रहा है, जो सर्वथा स्वाभाविक था। साथ ही अथर्ववेदीय तथा व्रात्यों के अन्यान्य विवेचन से यह स्पष्ट ही है कि इनका सीधा सम्बन्ध श्रमण-संस्कृति से है।
पं. बलभद्र जी ने ठीक ही लिखा है कि यही व्रात्य आजकल के जैनमतानुयायी हैं। महाव्रतपालक व्रात्य जैन साधु हैं और सामान्य व्रात्य जैनधर्मानुयायी हैं। महाव्रत ही आज का जैनधर्म है। इन व्रात्यों की संस्कृति आध्यात्मिक थी, जबकि आर्य लोगों की संस्कृति आधिदैविक थी। व्रात्यों की योगमूलक साधना, ध्यानमूलक तपस्या, अहिंसामूलक विचार वैदिक आर्यों में अत्यधिक लोकप्रिय होते गये। व्रात्यों की मान्यता थी कि व्यक्ति अपने प्रयत्न द्वारा कैवल्य प्राप्त कर सकता है।२४
१. जैनसाहित्य का इतिहास, पूर्वपीठिका, पृ. १११ से उद्धृत। २. व्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापति समैरयत्। अथर्ववेद,
१५.१.१। ३. चौदहवीं सदी के आचार्य सायण ने विजयनगर साम्राज्य के
राजसी माहौल में रहकर वेदों के भाष्यों की रचना की थी।
भारत-गाथा, सूर्यकान्त बाली, प्रका. निष्ठा, दिल्ली। ४. अथर्ववेदीयं व्रात्यकाण्डम् (डॉ.सम्पूर्णानन्दकृत श्रुतिप्रभभाष्य
- हिन्दी व्याख्या-सहितम्) भूमिका, पृ. २-३। ५. अथर्ववेद १५.२.६, ११-१४ । ६. अथर्ववेद, १५.२.८, ११-१४। ७. अथर्ववेद, १५.२.१५-१६, २२। ८. अथर्ववेद, १५.१४.१-२४। ९. अथर्ववेद, काण्ड १५ के सम्पूर्ण सूक्त। १०. अथर्ववेद, १५.१.१-९। ११. अथर्ववेद, १५.१८.५। १२. ब्राह्मण तथा श्रमण-संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ.७६ । १३. ब्राह्मण तथा श्रमण-संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ.७८ से
उद्धत, लेखक डॉ. जगदीशदत्त दीक्षित, प्रका.-भा.
विद्याप्रकाशन, दिल्ली, १९८४ । १४. हिस्ट्री एण्ड डाक्ट्रिन्स ऑफ आजीवकास-ए.एल.भाषम्, पृ.
८.
१५. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृ. ३४९। १६. द रिलीजन एण्ड फिलासफी ऑफ अथर्ववेद, पृ.७। १७. द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द १, पृ.१११ (भारतीय
द्वितीय संस्करण, १९६२)। १८. विशेष टिप्पणी- भारत के अनेक क्षेत्रों, विशेषकर मध्यप्रदेश
के बुन्देलखण्ड में यह सब वणिक्वृत्तिकार्य, जिसे 'बंजी' कहते
हैं, आज तक प्रचलित है। १९. आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रन्थ, तृतीय खण्ड के पृ.७-८ पर लिखित
'प्री आर्यन भारतीय रिलीजन' नामक लेख से उद्धत। २०. बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ, पृ. २००-२०१ में डॉ.
देवेन्द्रकुमार शास्त्री का लेख 'जैनधर्म की प्राचीनता एवं
सार्वभौमिकता', कलकत्ता, १९६७। २१. प्राकृत भारती, जयपुर से १९८८ में प्रकाशित। २२. अथर्ववेद, भाषाभाष्ये पञ्चदश काण्डम्, १५.२.१०.१ एवं
१५.१.१.१, पृ. ३०७ दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली, १९५७ । २३. प्रजापतेः सुतो नाभि तस्यामी अरिमुच्यति।
नाभिनो ऋषभपुत्रो कैः सिद्धकर्मदृढव्रतः॥ २९० ॥ २४. अहिंसा दर्शन, पं. बलभद्र जैन, पृ. २८ ।
आचार्य एवं अध्यक्ष
जैनदर्शन विभाग सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी
नवम्बर 2006 जिनभाषित 23
www.jainelibrary.org
Jain Education International
For Private & Personal Use Only