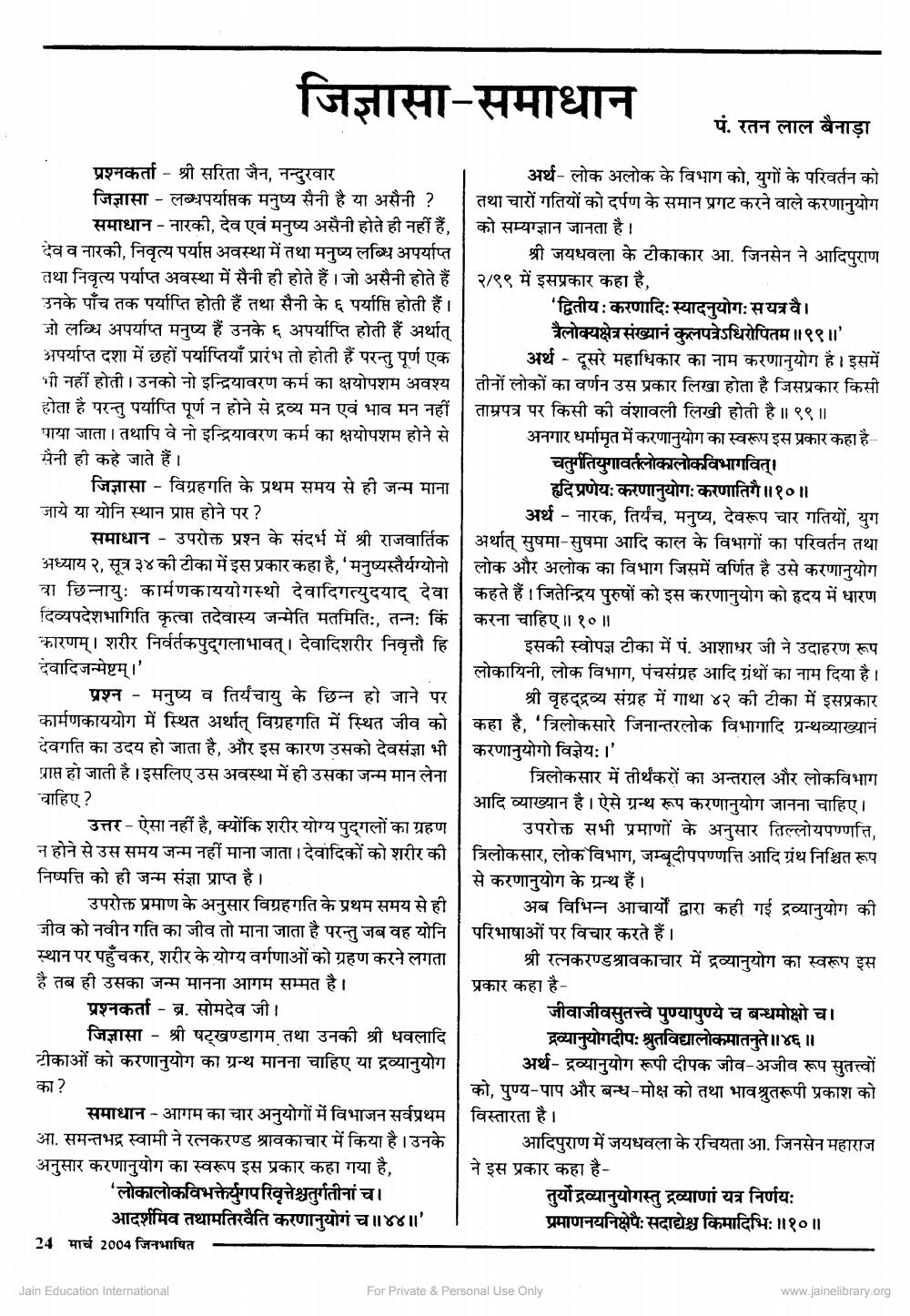________________
पा-समाधान
पं. रतन लाल बैनाड़ा
प्रश्नकर्ता - श्री सरिता जैन, नन्दुरवार
अर्थ- लोक अलोक के विभाग को, युगों के परिवर्तन को जिज्ञासा - लब्धपर्याप्तक मनुष्य सैनी है या असैनी? तथा चारों गतियों को दर्पण के समान प्रगट करने वाले करणानुयोग
समाधान - नारकी, देव एवं मनुष्य असैनी होते ही नहीं हैं, को सम्यग्ज्ञान जानता है। देव व नारकी, निवृत्य पर्याप्त अवस्था में तथा मनुष्य लब्धि अपर्याप्त | श्री जयधवला के टीकाकार आ. जिनसेन ने आदिपुराण तथा निवृत्य पर्याप्त अवस्था में सैनी ही होते हैं । जो असैनी होते हैं । २/९९ में इसप्रकार कहा है, उनके पाँच तक पर्याप्ति होती हैं तथा सैनी के ६ पर्याप्ति होती हैं।
'द्वितीयःकरणादिः स्यादनयोगःसयत्र वै। जो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य हैं उनके ६ अपर्याप्ति होती हैं अर्थात्
त्रैलोक्यक्षेत्रसंख्यानं कुलपत्रेऽधिरोपितम ।।९९॥' अपर्याप्त दशा में छहों पर्याप्तियाँ प्रारंभ तो होती हैं परन्तु पूर्ण एक अर्थ - दूसरे महाधिकार का नाम करणानुयोग है। इसमें भी नहीं होती। उनको नो इन्द्रियावरण कर्म का क्षयोपशम अवश्य | तीनों लोकों का वर्णन उस प्रकार लिखा होता है जिसप्रकार किसी होता है परन्तु पर्याप्ति पूर्ण न होने से द्रव्य मन एवं भाव मन नहीं | ताम्रपत्र पर किसी की वंशावली लिखी होती है ॥ ९९ ॥ पाया जाता। तथापि वे नो इन्द्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होने से अनगार धर्मामृत में करणानुयोग का स्वरूप इस प्रकार कहा है सैनी ही कहे जाते हैं।
चतुर्गतियुगावर्तलोकालोकविभागवित्। जिज्ञासा - विग्रहगति के प्रथम समय से ही जन्म माना
हृदिप्रणेयः करणानुयोग: करणातिगै॥१०॥ जाये या योनि स्थान प्राप्त होने पर?
अर्थ - नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देवरूप चार गतियों, युग समाधान - उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में श्री राजवार्तिक | अर्थात् सुषमा-सुषमा आदि काल के विभागों का परिवर्तन तथा अध्याय २, सूत्र ३४ की टीका में इस प्रकार कहा है, 'मनुष्यस्तैर्यग्योनो लोक और अलोक का विभाग जिसमें वर्णित है उसे करणानुयोग वा छिन्नायुः कार्मणकाययोगस्थो देवादिगत्युदयाद् देवा | कहते हैं। जितेन्द्रिय पुरुषों को इस करणानुयोग को हृदय में धारण दिव्यपदेशभागिति कृत्वा तदेवास्य जन्मेति मतमितिः, तन्नः किं करना चाहिए॥१०॥ कारणम्। शरीर निर्वर्तकपुद्गलाभावत्। देवादिशरीर निवृत्तौ हि इसकी स्वोपज्ञ टीका में पं. आशाधर जी ने उदाहरण रूप देवादिजन्मेष्टम्।'
लोकायिनी, लोक विभाग, पंचसंग्रह आदि ग्रंथों का नाम दिया है। प्रश्न - मनुष्य व तिर्यंचायु के छिन्न हो जाने पर श्री वृहद्रव्य संग्रह में गाथा ४२ की टीका में इसप्रकार कार्मणकाययोग में स्थित अर्थात् विग्रहगति में स्थित जीव को कहा है, 'त्रिलोकसारे जिनान्तरलोक विभागादि ग्रन्थव्याख्यानं देवगति का उदय हो जाता है, और इस कारण उसको देवसंज्ञा भी | करणानुयोगो विज्ञेयः।' प्राप्त हो जाती है। इसलिए उस अवस्था में ही उसका जन्म मान लेना त्रिलोकसार में तीर्थंकरों का अन्तराल और लोकविभाग चाहिए?
आदि व्याख्यान है। ऐसे ग्रन्थ रूप करणानुयोग जानना चाहिए। उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर योग्य पुदगलों का ग्रहण । उपरोक्त सभी प्रमाणों के अनुसार तिल्लोयपण्णत्ति, न होने से उस समय जन्म नहीं माना जाता । देवादिकों को शरीर की | त्रिलोकसार, लोक विभाग, जम्बूदीपपण्णत्ति आदि ग्रंथ निश्चित रूप निष्पत्ति को ही जन्म संज्ञा प्राप्त है।
से करणानुयोग के ग्रन्थ हैं। उपरोक्त प्रमाण के अनुसार विग्रहगति के प्रथम समय से ही अब विभिन्न आचार्यों द्वारा कही गई द्रव्यानुयोग की जीव को नवीन गति का जीव तो माना जाता है परन्तु जब वह योनि | परिभाषाओं पर विचार करते हैं। स्थान पर पहुँचकर, शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करने लगता श्री रत्नकरण्डश्रावकाचार में द्रव्यानुयोग का स्वरूप इस है तब ही उसका जन्म मानना आगम सम्मत है।
प्रकार कहा हैप्रश्नकर्ता - ब्र. सोमदेव जी।
जीवाजीवसुतत्त्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षो च। जिज्ञासा - श्री षटखण्डागम तथा उनकी श्री धवलादि
द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते॥४६॥ टीकाओं को करणानुयोग का ग्रन्थ मानना चाहिए या द्रव्यानुयोग अर्थ- द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जीव-अजीव रूप सुतत्त्वों का?
को, पुण्य-पाप और बन्ध-मोक्ष को तथा भाव श्रुतरूपी प्रकाश को समाधान- आगम का चार अनुयोगों में विभाजन सर्वप्रथम | विस्तारता है। आ. समन्तभद्र स्वामी ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में किया है। उनके । आदिपुराण में जयधवला के रचियता आ. जिनसेन महाराज अनुसार करणानुयोग का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है, ने इस प्रकार कहा है'लोकालोकविभक्तेर्युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनांच।
तुर्योद्रव्यानुयोगस्तु द्रव्याणां यत्र निर्णयः आदर्शमिव तथामतिरवैति करणानुयोगं च॥४४॥'
प्रमाणनयनिक्षेपैः सदाद्येश्च किमादिभिः॥१०॥ 24 मार्च 2004 जिनभाषित
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org