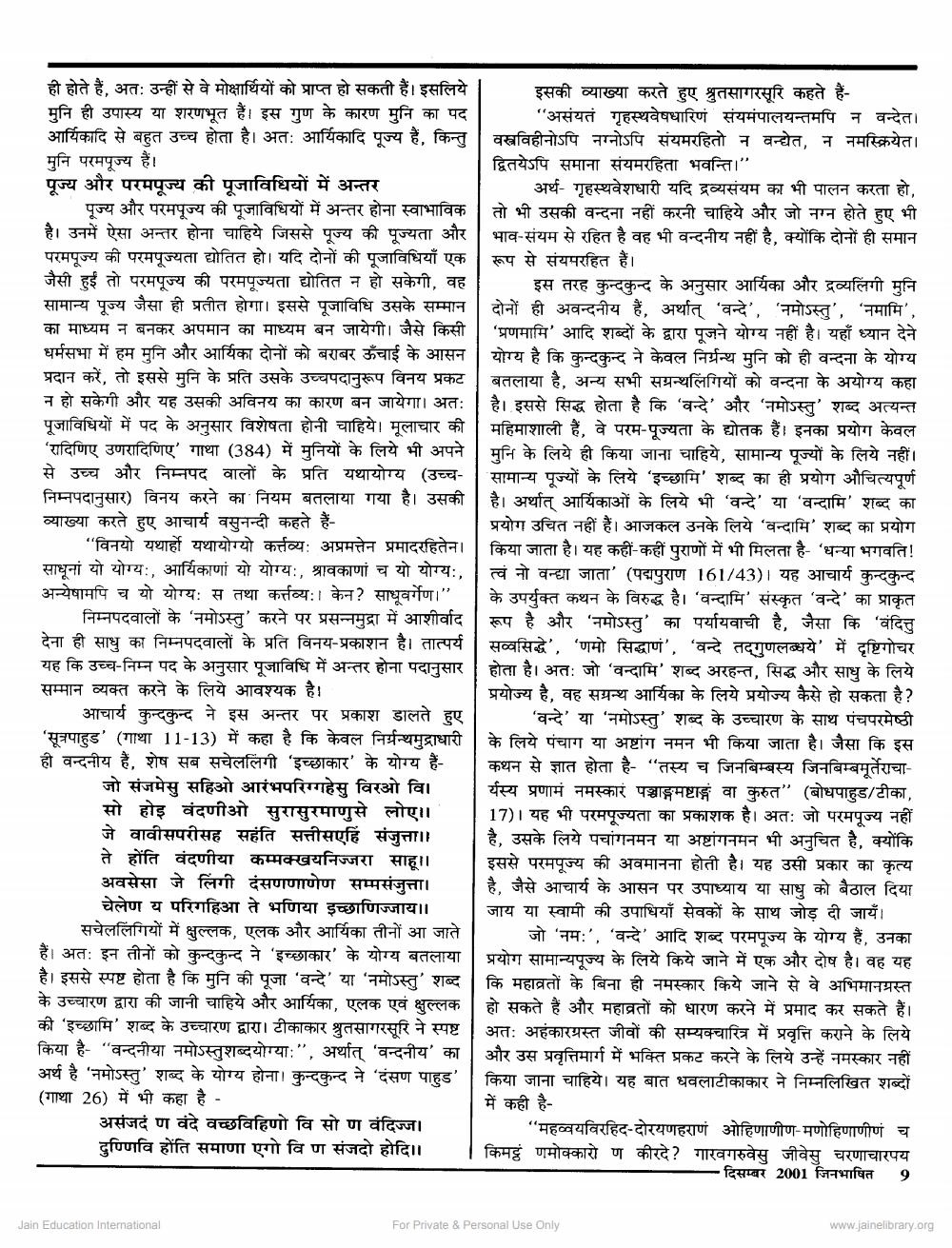________________
ही होते हैं, अत: उन्हीं से वे मोक्षार्थियों को प्राप्त हो सकती हैं। इसलिये | इसकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरि कहते हैंमुनि ही उपास्य या शरणभूत हैं। इस गुण के कारण मुनि का पद "असंयतं गृहस्थवेषधारिणं संयमपालयन्तमपि न वन्देत। आर्यिकादि से बहुत उच्च होता है। अतः आर्यिकादि पूज्य हैं, किन्तु | वस्त्रविहीनोऽपि नग्नोऽपि संयमरहितो न वन्द्येत, न नमस्क्रियेत। मुनि परमपूज्य हैं।
द्वितयेऽपि समाना संयमरहिता भवन्ति।" पूज्य और परमपूज्य की पूजाविधियों में अन्तर
अर्थ- गृहस्थवेशधारी यदि द्रव्यसंयम का भी पालन करता हो, पूज्य और परमपूज्य की पूजाविधियों में अन्तर होना स्वाभाविक | तो भी उसकी वन्दना नहीं करनी चाहिये और जो नग्न होते हुए भी है। उनमें ऐसा अन्तर होना चाहिये जिससे पूज्य की पूज्यता और भाव-संयम से रहित है वह भी वन्दनीय नहीं है, क्योंकि दोनों ही समान परमपूज्य की परमपूज्यता द्योतित हो। यदि दोनों की पूजाविधियाँ एक रूप से संयमरहित हैं। जैसी हुई तो परमपूज्य की परमपूज्यता द्योतित न हो सकेगी, वह इस तरह कुन्दकुन्द के अनुसार आर्यिका और द्रव्यलिंगी मुनि सामान्य पूज्य जैसा ही प्रतीत होगा। इससे पूजाविधि उसके सम्मान दोनों ही अवन्दनीय हैं, अर्थात् 'वन्दे', 'नमोऽस्तु', 'नमामि', का माध्यम न बनकर अपमान का माध्यम बन जायेगी। जैसे किसी 'प्रणमामि' आदि शब्दों के द्वारा पूजने योग्य नहीं है। यहाँ ध्यान देने धर्मसभा में हम मुनि और आर्यिका दोनों को बराबर ऊँचाई के आसन योग्य है कि कुन्दकुन्द ने केवल निर्ग्रन्थ मुनि को ही वन्दना के योग्य प्रदान करें, तो इससे मुनि के प्रति उसके उच्चपदानुरूप विनय प्रकट बतलाया है, अन्य सभी सग्रन्थलिंगियों को वन्दना के अयोग्य कहा न हो सकेगी और यह उसकी अविनय का कारण बन जायेगा। अत: है। इससे सिद्ध होता है कि 'वन्दे' और 'नमोऽस्तु' शब्द अत्यन्त पूजाविधियों में पद के अनुसार विशेषता होनी चाहिये। मूलाचार की महिमाशाली हैं, वे परम-पूज्यता के द्योतक हैं। इनका प्रयोग केवल 'रादिणिए उणरादिणिए' गाथा (384) में मुनियों के लिये भी अपने मुनि के लिये ही किया जाना चाहिये, सामान्य पूज्यों के लिये नहीं। से उच्च और निम्नपद वालों के प्रति यथायोग्य (उच्च- सामान्य पूज्यों के लिये 'इच्छामि' शब्द का ही प्रयोग औचित्यपूर्ण निम्नपदानुसार) विनय करने का नियम बतलाया गया है। उसकी है। अर्थात् आर्यिकाओं के लिये भी 'वन्दे' या 'वन्दामि' शब्द का व्याख्या करते हुए आचार्य वसुनन्दी कहते हैं
प्रयोग उचित नहीं हैं। आजकल उनके लिये 'वन्दामि' शब्द का प्रयोग "विनयो यथार्हो यथायोग्यो कर्त्तव्यः अप्रमत्तेन प्रमादरहितेन। किया जाता है। यह कहीं-कहीं पुराणों में भी मिलता है- 'धन्या भगवति! साधूनां यो योग्यः, आर्यिकाणां यो योग्यः, श्रावकाणां च यो योग्यः, | त्वं नो वन्द्या जाता' (पद्मपुराण 161/43)। यह आचार्य कुन्दकुन्द अन्येषामपि च यो योग्यः स तथा कर्तव्यः। केन? साधूवर्गेण।" के उपर्युक्त कथन के विरुद्ध है। 'वन्दामि' संस्कृत 'वन्दे' का प्राकृत
निम्नपदवालों के 'नमोऽस्तु' करने पर प्रसन्नमुद्रा में आशीर्वाद | रूप है और 'नमोऽस्तु' का पर्यायवाची है, जैसा कि 'वंदित्तु देना ही साधु का निम्नपदवालों के प्रति विनय-प्रकाशन है। तात्पर्य | सव्वसिद्धे', 'णमो सिद्धाणं', 'वन्दे तद्गुणलब्धये' में दृष्टिगोचर यह कि उच्च-निम्न पद के अनुसार पूजाविधि में अन्तर होना पदानुसार होता है। अतः जो 'वन्दामि' शब्द अरहन्त, सिद्ध और साधु के लिये सम्मान व्यक्त करने के लिये आवश्यक है।
प्रयोज्य है, वह सग्रन्थ आर्यिका के लिये प्रयोज्य कैसे हो सकता है? आचार्य कुन्दकुन्द ने इस अन्तर पर प्रकाश डालते हुए 'वन्दे' या 'नमोऽस्तु' शब्द के उच्चारण के साथ पंचपरमेष्ठी 'सूत्रपाहुड' (गाथा 11-13) में कहा है कि केवल निर्ग्रन्थमुद्राधारी | के लिये पंचाग या अष्टांग नमन भी किया जाता है। जैसा कि इस ही वन्दनीय हैं, शेष सब सचेललिंगी 'इच्छाकार' के योग्य हैं- कथन से ज्ञात होता है- "तस्य च जिनबिम्बस्य जिनबिम्बमूर्तेराचा
जो संजमेसु सहिओ आरंभपरिग्गहेसु विरओ वि। र्यस्य प्रणामं नमस्कारं पञ्चाङ्गमष्टाङ्ग वा कुरुत" (बोधपाहुड/टीका, सो होइ वंदणीओ सुरासुरमाणुसे लोए।
17)। यह भी परमपूज्यता का प्रकाशक है। अत: जो परमपूज्य नहीं जे वावीसपरीसह सहति सत्तीसएहिं संजुत्ता।। है, उसके लिये पचांगनमन या अष्टांगनमन भी अनुचित है, क्योंकि ते होंति वंदणीया कम्मक्खयनिज्जरा साहू।। इससे परमपूज्य की अवमानना होती है। यह उसी प्रकार का कृत्य अवसेसा जे लिंगी दंसणणाणेण सम्मसंजुत्ता। है, जैसे आचार्य के आसन पर उपाध्याय या साधु को बैठाल दिया
चेलेण य परिगहिआ ते भणिया इच्छाणिज्जाय।। जाय या स्वामी की उपाधियाँ सेवकों के साथ जोड़ दी जायें।
सचेललिंगियों में क्षुल्लक, एलक और आर्यिका तीनों आ जाते | जो 'नमः', 'वन्दे' आदि शब्द परमपूज्य के योग्य हैं, उनका हैं। अत: इन तीनों को कुन्दकुन्द ने 'इच्छाकार' के योग्य बतलाया प्रयोग सामान्यपूज्य के लिये किये जाने में एक और दोष है। वह यह है। इससे स्पष्ट होता है कि मुनि की पूजा 'वन्दे' या 'नमोऽस्तु' शब्द कि महाव्रतों के बिना ही नमस्कार किये जाने से वे अभिमानग्रस्त के उच्चारण द्वारा की जानी चाहिये और आर्यिका, एलक एवं क्षुल्लक हो सकते हैं और महाव्रतों को धारण करने में प्रमाद कर सकते हैं। की 'इच्छामि' शब्द के उच्चारण द्वारा। टीकाकार श्रुतसागरसूरि ने स्पष्ट अतः अहंकारग्रस्त जीवों की सम्यक्चारित्र में प्रवृत्ति कराने के लिये किया है- "वन्दनीया नमोऽस्तुशब्दयोग्याः", अर्थात् 'वन्दनीय' का और उस प्रवृत्तिमार्ग में भक्ति प्रकट करने के लिये उन्हें नमस्कार नहीं अर्थ है 'नमोऽस्तु' शब्द के योग्य होना। कुन्दकुन्द ने 'दंसण पाहुड' | किया जाना चाहिये। यह बात धवलाटीकाकार ने निम्नलिखित शब्दों (गाथा 26) में भी कहा है -
में कही हैअसंजदं ण वंदे वच्छविहिणो वि सो ण वंदिज्ज।
"महव्वयविरहिद-दोरयणहराणं ओहिणाणीण-मणोहिणाणीणं च दुण्णिवि होंति समाणा एगो वि ण संजदो होदि॥ । किमटुं णमोक्कारो ण कीरदे? गारवगरुवेसु जीवेसु चरणाचारपय
- दिसम्बर 2001 जिनभाषित 9
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org